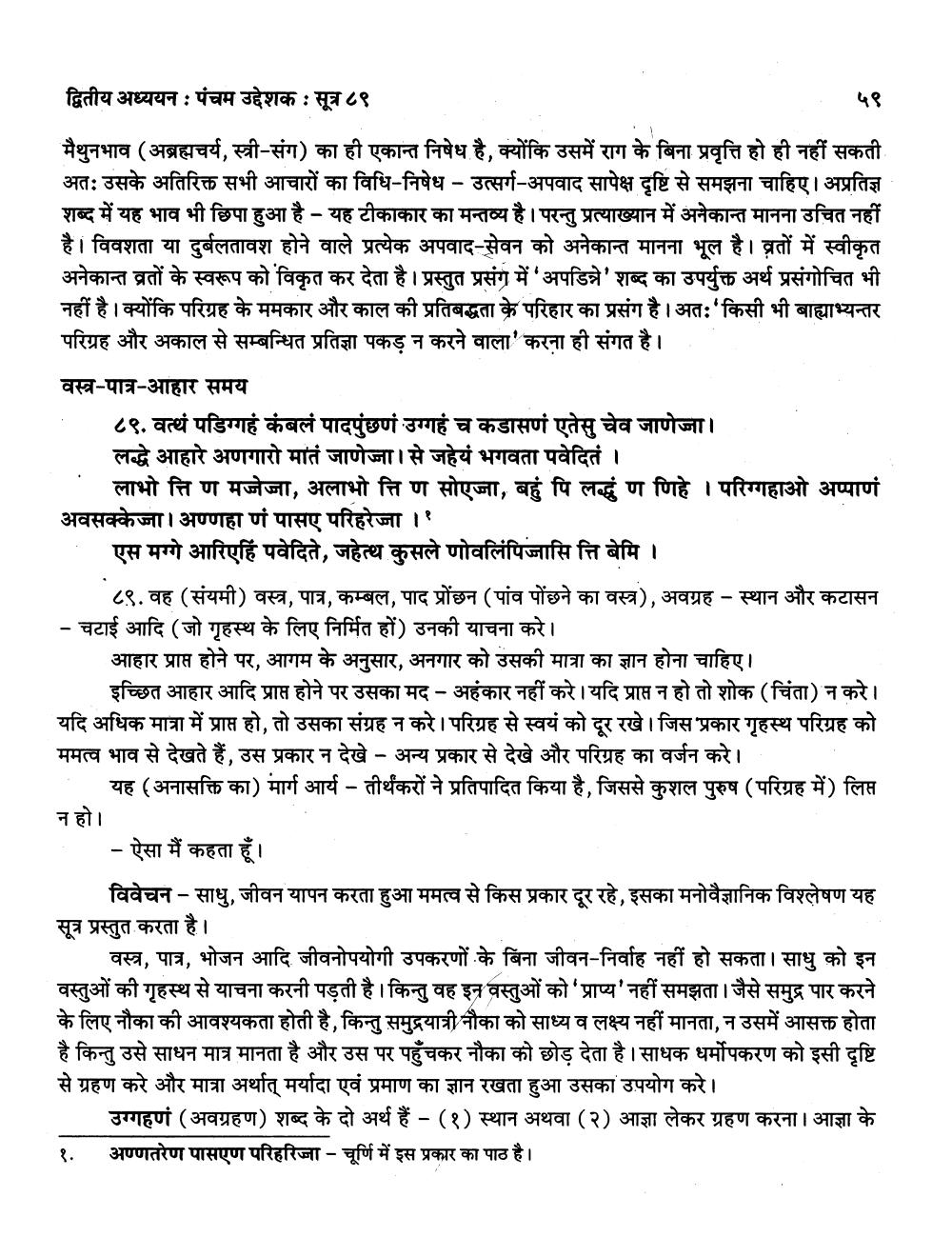________________
द्वितीय अध्ययन : पंचम उद्देशक : सूत्र ८९
मैथुनभाव (अब्रह्मचर्य, स्त्री-संग) का ही एकान्त निषेध है, क्योंकि उसमें राग के बिना प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती अतः उसके अतिरिक्त सभी आचारों का विधि-निषेध - उत्सर्ग-अपवाद सापेक्ष दृष्टि से समझना चाहिए। अप्रतिज्ञ शब्द में यह भाव भी छिपा हुआ है - यह टीकाकार का मन्तव्य है। परन्तु प्रत्याख्यान में अनेकान्त मानना उचित नहीं है। विवशता या दुर्बलतावश होने वाले प्रत्येक अपवाद-सेवन को अनेकान्त मानना भूल है। व्रतों में स्वीकृत अनेकान्त व्रतों के स्वरूप को विकृत कर देता है। प्रस्तुत प्रसंग में 'अपडिन्ने' शब्द का उपर्युक्त अर्थ प्रसंगोचित भी नहीं है । क्योंकि परिग्रह के ममकार और काल की प्रतिबद्धता के परिहार का प्रसंग है। अतः किसी भी बाह्याभ्यन्तर परिग्रह और अकाल से सम्बन्धित प्रतिज्ञा पकड़ न करने वाला' करना ही संगत है। वस्त्र-पात्र-आहार समय
८९. वत्थं पडिग्गहं कंबलं पादपुंछणं उग्गहं च कडासणं एतेसु चेव जाणेजा।
लद्धे आहारे अणगारो मातं जाणेजा।से जहेयं भगवता पवेदितं । - लाभो त्ति ण मज्जेजा, अलाभो त्ति ण सोएजा, बहुं पि लद्धं ण णिहे । परिग्गहाओ अप्पाणं अवसक्केजा। अण्णहा णं पासए परिहरेज्जा ।'
एस मग्गे आरिएहिं पवेदिते, जहेत्थ कुसले णोवलिंपिजासि त्ति बेमि ।
८९. वह (संयमी) वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद प्रोंछन (पांव पोंछने का वस्त्र), अवग्रह - स्थान और कटासन - चटाई आदि (जो गृहस्थ के लिए निर्मित हों) उनकी याचना करे।
आहार प्राप्त होने पर, आगम के अनुसार, अनगार को उसकी मात्रा का ज्ञान होना चाहिए।
इच्छित आहार आदि प्राप्त होने पर उसका मद - अहंकार नहीं करे । यदि प्राप्त न हो तो शोक (चिंता) न करे। यदि अधिक मात्रा में प्राप्त हो, तो उसका संग्रह न करे। परिग्रह से स्वयं को दूर रखे। जिस प्रकार गृहस्थ परिग्रह को ममत्व भाव से देखते हैं, उस प्रकार न देखे - अन्य प्रकार से देखे और परिग्रह का वर्जन करे। ___ यह (अनासक्ति का) मार्ग आर्य - तीर्थंकरों ने प्रतिपादित किया है, जिससे कुशल पुरुष (परिग्रह में) लिप्त न हो।
- ऐसा मैं कहता हूँ।
विवेचन - साधु, जीवन यापन करता हुआ ममत्व से किस प्रकार दूर रहे, इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यह सूत्र प्रस्तुत करता है।
वस्त्र, पात्र, भोजन आदि जीवनोपयोगी उपकरणों के बिना जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता। साधु को इन वस्तुओं की गृहस्थ से याचना करनी पड़ती है। किन्तु वह इन वस्तुओं को प्राप्य' नहीं समझता। जैसे समुद्र पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, किन्तु समुद्रयात्री नौका को साध्य व लक्ष्य नहीं मानता, न उसमें आसक्त होता है किन्तु उसे साधन मात्र मानता है और उस पर पहुंचकर नौका को छोड़ देता है। साधक धर्मोपकरण को इसी दृष्टि से ग्रहण करे और मात्रा अर्थात् मर्यादा एवं प्रमाण का ज्ञान रखता हुआ उसका उपयोग करे।
उग्गहणं (अवग्रहण) शब्द के दो अर्थ हैं - (१) स्थान अथवा (२) आज्ञा लेकर ग्रहण करना। आज्ञा के अण्णतरेण पासएण परिहरिज्जा - चूर्णि में इस प्रकार का पाठ है।