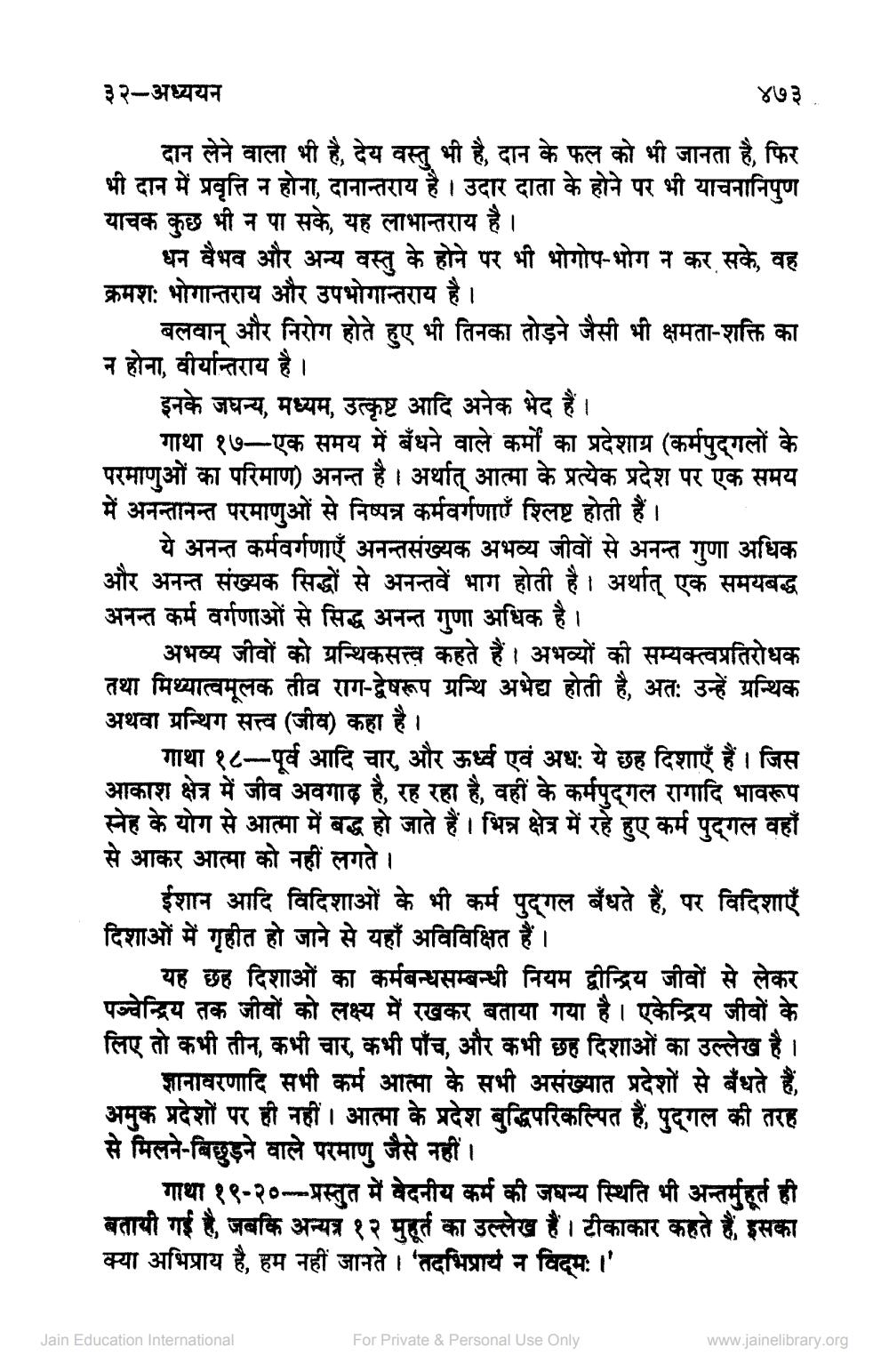________________
३२-अध्ययन
४७३ .
दान लेने वाला भी है, देय वस्तु भी है, दान के फल को भी जानता है, फिर भी दान में प्रवृत्ति न होना, दानान्तराय है। उदार दाता के होने पर भी याचनानिपुण याचक कुछ भी न पा सके, यह लाभान्तराय है।
धन वैभव और अन्य वस्तु के होने पर भी भोगोप-भोग न कर सके, वह क्रमश: भोगान्तराय और उपभोगान्तराय है।
___ बलवान और निरोग होते हए भी तिनका तोड़ने जैसी भी क्षमता-शक्ति का न होना, वीर्यान्तराय है।
इनके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट आदि अनेक भेद हैं।
गाथा १७–एक समय में बँधने वाले कर्मों का प्रदेशाग्र (कर्मपुद्गलों के परमाणुओं का परिमाण) अनन्त है। अर्थात् आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर एक समय में अनन्तानन्त परमाणुओं से निष्पत्र कर्मवर्गणाएँ श्लिष्ट होती हैं।
ये अनन्त कर्मवर्गणाएँ अनन्तसंख्यक अभव्य जीवों से अनन्त गुणा अधिक और अनन्त संख्यक सिद्धों से अनन्तवें भाग होती है। अर्थात् एक समयबद्ध अनन्त कर्म वर्गणाओं से सिद्ध अनन्त गुणा अधिक है।
___ अभव्य जीवों को ग्रन्थिकसत्त्व कहते हैं। अभव्यों की सम्यक्त्वप्रतिरोधक तथा मिथ्यात्वमूलक तीव्र राग-द्वेषरूप ग्रन्थि अभेद्य होती है, अत: उन्हें ग्रन्थिक अथवा ग्रन्थिग सत्त्व (जीव) कहा है।
गाथा १८-पूर्व आदि चार, और ऊर्ध्व एवं अध: ये छह दिशाएँ हैं । जिस आकाश क्षेत्र में जीव अवगाढ़ है, रह रहा है, वहीं के कर्मपुद्गल रागादि भावरूप स्नेह के योग से आत्मा में बद्ध हो जाते हैं । भिन्न क्षेत्र में रहे हुए कर्म पुद्गल वहाँ से आकर आत्मा को नहीं लगते।
ईशान आदि विदिशाओं के भी कर्म पुद्गल बँधते हैं, पर विदिशाएँ दिशाओं में गृहीत हो जाने से यहाँ अविविक्षित हैं।
यह छह दिशाओं का कर्मबन्धसम्बन्धी नियम द्वीन्द्रिय जीवों से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक जीवों को लक्ष्य में रखकर बताया गया है। एकेन्द्रिय जीवों के लिए तो कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच, और कभी छह दिशाओं का उल्लेख है।
ज्ञानावरणादि सभी कर्म आत्मा के सभी असंख्यात प्रदेशों से बँधते हैं, अमुक प्रदेशों पर ही नहीं। आत्मा के प्रदेश बुद्धिपरिकल्पित हैं, पुदगल की तरह से मिलने-बिछुड़ने वाले परमाणु जैसे नहीं।
गाथा १९-२०-~-प्रस्तुत में वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति भी अन्तर्मुहूर्त ही बतायी गई है, जबकि अन्यत्र १२ मुहूर्त का उल्लेख है। टीकाकार कहते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, हम नहीं जानते । 'तदभिप्राय न विद्मः ।'
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org