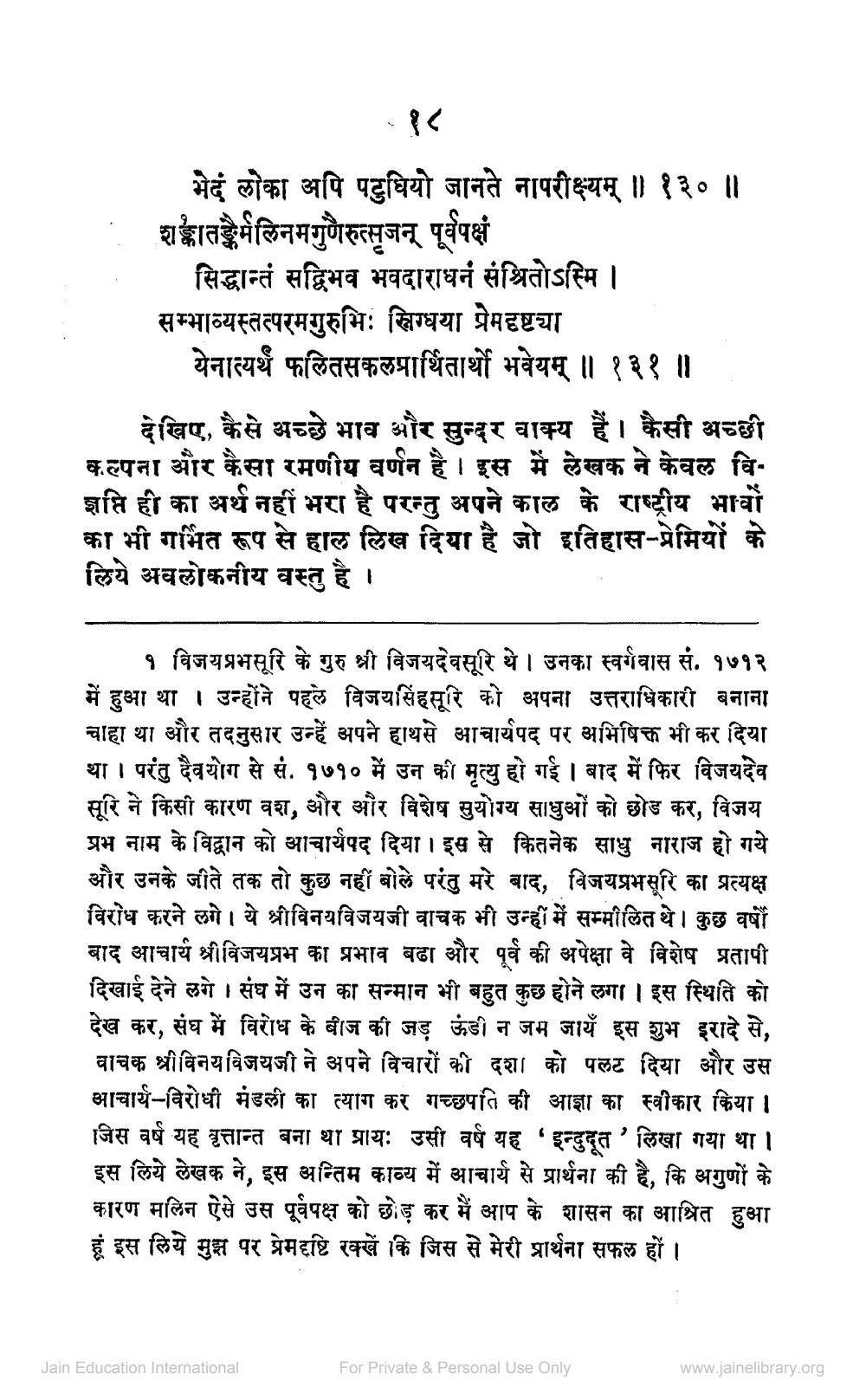________________
भेदं लोका अपि पटुधियो जानते नापरीक्ष्यम् ॥ १३० ॥ शङ्कातडॅमलिनमगुणैरुत्सृजन् पूर्वपक्षं
सिद्धान्तं सद्विभव भवदाराधनं संश्रितोऽस्मि । सम्भाव्यस्तत्परमगुरुभिः स्निग्धया प्रेमदृष्ट्या
येनात्यर्थं फलितसकलप्रार्थितार्थो भवेयम् ॥ १३१ ॥ देखिए, कैसे अच्छे भाव और सुन्दर वाक्य हैं। कैसी अच्छी कल्पना और कैसा रमणीय वर्णन है । इस में लेखक ने केवल वि. ज्ञप्ति ही का अर्थ नहीं भरा है परन्तु अपने काल के राष्ट्रीय भावों का भी गर्मित रूप से हाल लिख दिया है जो इतिहास-प्रेमियों के लिये अवलोकनीय वस्तु है ।
१ विजयप्रभसूरि के गुरु श्री विजयदेवसूरि थे। उनका स्वर्गवास सं. १७१२ में हुआ था । उन्होंने पहले विजयसिंहसूरि को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा था और तदनुसार उन्हें अपने हाथसे आचार्यपद पर अभिषिक्त भी कर दिया था। परंतु दैवयोग से सं. १७१० में उन की मृत्यु हो गई। बाद में फिर विजयदेव सूरि ने किसी कारण वश, और और विशेष सुयोग्य साधुओं को छोड कर, विजय प्रभ नाम के विद्वान को आचार्यपद दिया। इस से कितनेक साधु नाराज हो गये
और उनके जीते तक तो कुछ नहीं बोले परंतु मरे बाद, विजयप्रभसूरि का प्रत्यक्ष विरोध करने लगे। ये श्रीविनयविजयजी वाचक भी उन्हीं में सम्मीलित थे। कुछ वर्षों बाद आचार्य श्री विजयप्रभ का प्रभाव बढा और पूर्व की अपेक्षा वे विशेष प्रतापी दिखाई देने लगे। संघ में उन का सन्मान भी बहुत कुछ होने लगा। इस स्थिति को देख कर, संघ में विरोध के बीज की जड़ ऊंडी न जम जायँ इस शुभ इरादे से, वाचक श्रीविनय विजयजी ने अपने विचारों की दशा को पलट दिया और उस आचार्य-विरोधी मंडली का त्याग कर गच्छपति की आज्ञा का स्वीकार किया। जिस वर्ष यह वृत्तान्त बना था प्रायः उसी वर्ष यह 'इन्दुदूत' लिखा गया था। इस लिये लेखक ने, इस अन्तिम काव्य में आचार्य से प्रार्थना की है, कि अगुणों के कारण मलिन ऐसे उस पूर्वपक्ष को छोड़ कर मैं आप के शासन का आश्रित हुआ हूं इस लिये मुझ पर प्रेमदृष्टि रक्खें कि जिस से मेरी प्रार्थना सफल हो ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org