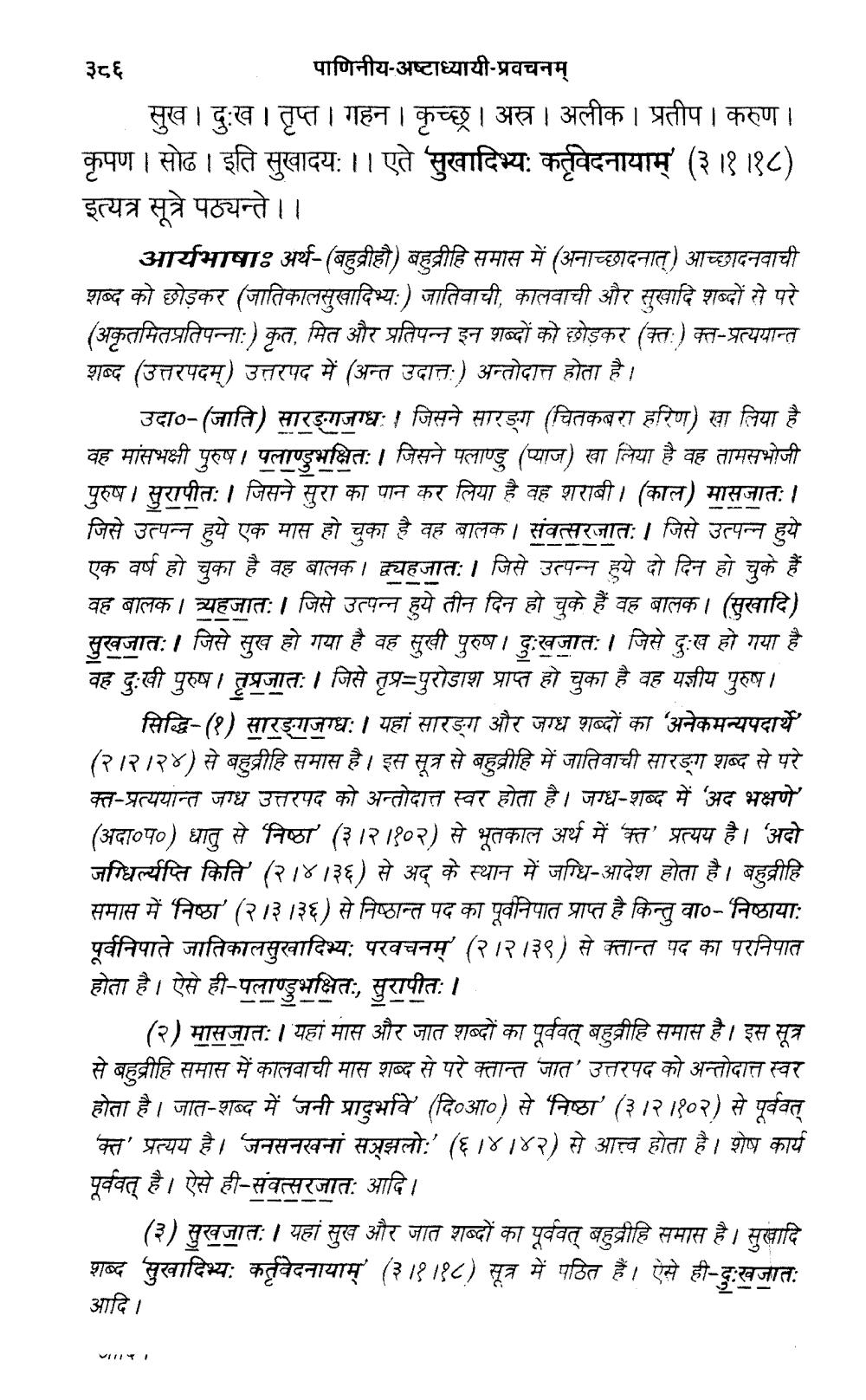________________
३८६
पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम् ___ सुख । दुःख । तृप्त । गहन । कृच्छ्र। अस्र । अलीक। प्रतीप । करुण। कृपण। सोढ । इति सुखादयः ।। एते सुखादिभ्य: कर्तृवेदनायाम् (३।१।१८) इत्यत्र सूत्रे पठ्यन्ते।।
आर्यभाषा अर्थ- (बहुव्रीहौ) बहुव्रीहि समास में (अनाच्छादनात्) आच्छादनवाची शब्द को छोड़कर (जातिकालसुखादिभ्यः) जातिवाची, कालवाची और सुखादि शब्दों से परे (अकृतमितप्रतिपन्नाः) कृत, मित और प्रतिपन्न इन शब्दों को छोड़कर (क्तः) क्त-प्रत्ययान्त शब्द (उत्तरपदम्) उत्तरपद में (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त होता है।
उदा०-(जाति) सारङ्गजग्धः । जिसने सारङ्ग (चितकबरा हरिण) खा लिया है वह मांसभक्षी पुरुष। पलाण्डुभक्षित: । जिसने पलाण्डु (प्याज) खा लिया है वह तामसभोजी पुरुष। सुरापीतः। जिसने सुरा का पान कर लिया है वह शराबी। (काल) मासजातः । जिसे उत्पन्न हुये एक मास हो चुका है वह बालक । संवत्सरजातः । जिसे उत्पन्न हुये एक वर्ष हो चुका है वह बालक। व्यहजातः । जिसे उत्पन्न हुये दो दिन हो चुके हैं वह बालक । व्यहजातः । जिसे उत्पन्न हुये तीन दिन हो चुके हैं वह बालक। (सुखादि) सुखजातः । जिसे सुख हो गया है वह सुखी पुरुष। दुःखजातः । जिसे दुःख हो गया है वह दुःखी पुरुष। तृप्रजातः । जिसे तृप्र-पुरोडाश प्राप्त हो चुका है वह यज्ञीय पुरुष ।
सिद्धि-(१) सारङ्गजग्ध: । यहां सारङ्ग और जग्ध शब्दों का 'अनेकमन्यपदार्थे (२।२।२४) से बहुव्रीहि समास है। इस सूत्र से बहुव्रीहि में जातिवाची सारङ्ग शब्द से परे क्त-प्रत्ययान्त जग्ध उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है। जग्ध-शब्द में 'अद भक्षणे (अदा०प०) धातु से निष्ठा' (३।२।१०२) से भूतकाल अर्थ में 'क्त' प्रत्यय है। 'अदो जग्धिय॑प्ति किति' (२।४।३६) से अद् के स्थान में जग्धि-आदेश होता है। बहुव्रीहि समास में निष्ठा' (२ १३ १३६) से निष्ठान्त पद का पूर्वनिपात प्राप्त है किन्तु वा०-निष्ठाया: पूर्वनिपाते जातिकालसुखादिभ्यः परवचनम् (२।२।३९) से क्तान्त पद का परनिपात होता है। ऐसे ही-पलाण्डुभक्षितः, सुरापीतः ।
(२) मासजात:। यहां मास और जात शब्दों का पूर्ववत् बहुव्रीहि समास है। इस सूत्र से बहुव्रीहि समास में कालवाची मास शब्द से परे क्तान्त जात' उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है। जात-शब्द में जनी प्रादुर्भावे' (दि०आ०) से 'निष्ठा' (३।२।१०२) से पूर्ववत् क्त' प्रत्यय है। जनसनखनां सञ्झलो:' (६।४।४२) से आत्त्व होता है। शेष कार्य पूर्ववत् है। ऐसे ही-संवत्सरजात: आदि।
(३) सुखजातः । यहां सुख और जात शब्दों का पूर्ववत् बहुव्रीहि समास है। सुखादि शब्द 'सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् (३।१।१८) सूत्र में पठित हैं। ऐसे ही-दुःखजात: आदि।