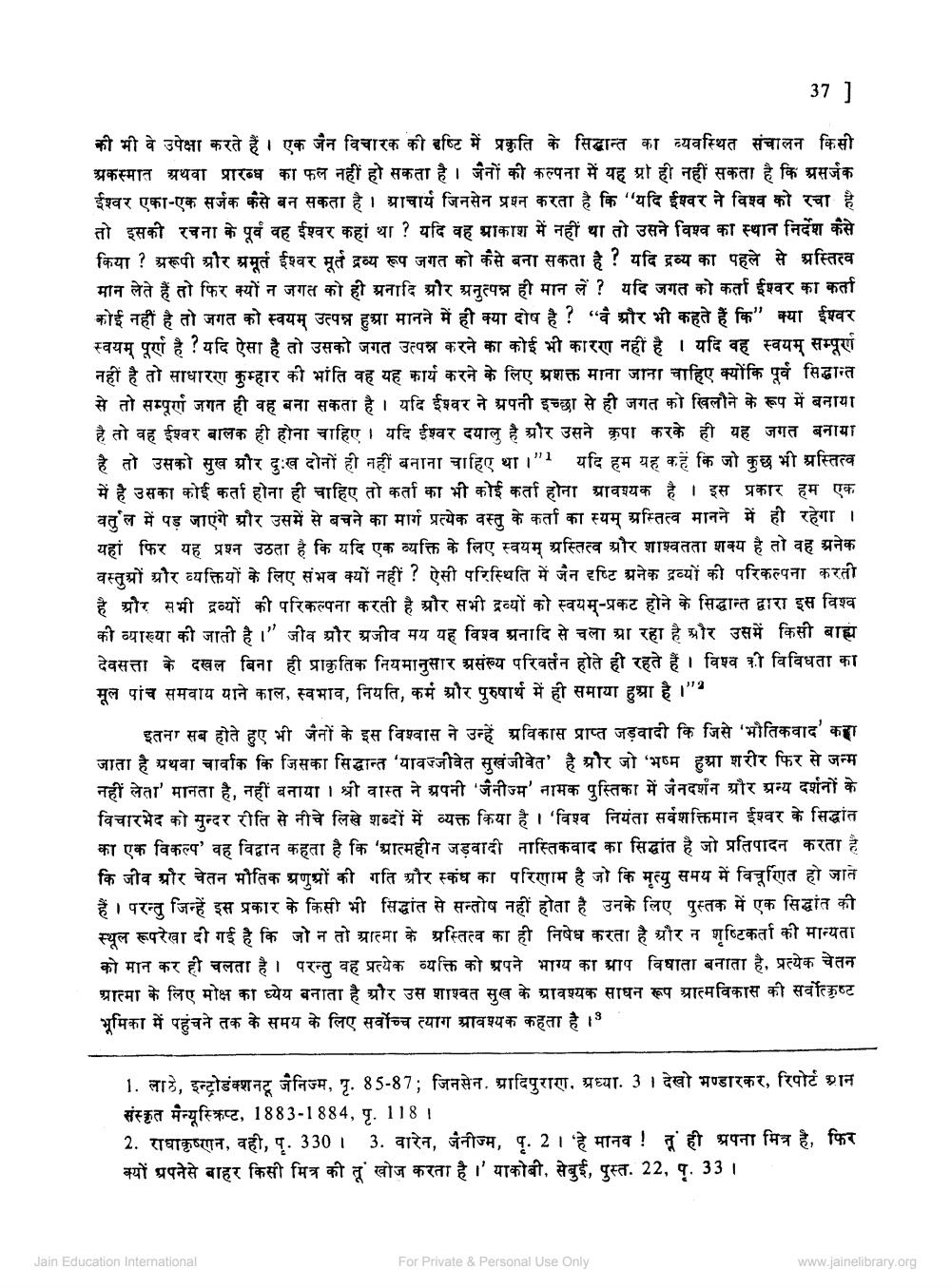________________
37 ]
की भी वे उपेक्षा करते हैं। एक जैन विचारक की दृष्टि में प्रकृति के सिद्धान्त का व्यवस्थित संचालन किसी अकस्मात अथवा प्रारब्ध का फल नहीं हो सकता है। जैनों की कल्पना में यह प्रो ही नहीं सकता है कि असर्जक ईश्वर एका-एक सर्जक कैसे बन सकता है। प्राचार्य जिनसेन प्रश्न करता है कि "यदि ईश्वर ने विश्व को रचा है तो इसकी रचना के पूर्व वह ईश्वर कहां था ? यदि वह पाकाश में नहीं था तो उसने विश्व का स्थान निर्देश कैसे किया ? अरूपी और अमूर्त ईश्वर मूर्त द्रव्य रूप जगत को कैसे बना सकता है ? यदि द्रव्य का पहले से अस्तित्व मान लेते हैं तो फिर क्यों न जगत को ही अनादि और अनुत्पन्न ही मान लें? यदि जगत को कर्ता ईश्वर का कर्ता कोई नहीं है तो जगत को स्वयम् उत्पन्न हुआ मानने में ही क्या दोष है ? “वै और भी कहते हैं कि" क्या ईश्वर स्वयम् पूर्ण है ? यदि ऐसा है तो उसको जगत उत्पन्न करने का कोई भी कारण नहीं है । यदि वह स्वयम् सम्पूर्ण नहीं है तो साधारण कुम्हार की भांति वह यह कार्य करने के लिए अशक्त माना जाना चाहिए क्योंकि पूर्व सिद्धान्त से तो सम्पूर्ण जगत ही वह बना सकता है। यदि ईश्वर ने अपनी इच्छा से ही जगत को खिलौने के रूप में बनाया है तो वह ईश्वर बालक ही होना चाहिए। यदि ईश्वर दयालु है और उसने कृपा करके ही यह जगत बनाया है तो उसको सुख और दुःख दोनों ही नहीं बनाना चाहिए था।"] यदि हम यह कहें कि जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका कोई कर्ता होना ही चाहिए तो कर्ता का भी कोई कर्ता होना आवश्यक है । इस प्रकार हम एक वर्तुल में पड़ जाएंगे और उसमें से बचने का मार्ग प्रत्येक वस्तु के कर्ता का स्यम् अस्तित्व मानने में ही रहेगा । यहां फिर यह प्रश्न उठता है कि यदि एक व्यक्ति के लिए स्वयम् अस्तित्व और शाश्वतता शक्य है तो वह अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए संभव क्यों नहीं? ऐसी परिस्थिति में जैन दृष्टि अनेक द्रव्यों की परिकल्पना करती है और सभी द्रव्यों की परिकल्पना करती है और सभी द्रव्यों को स्वयम्-प्रकट होने के सिद्धान्त द्वारा इस विश्व की व्याख्या की जाती है।" जीव और अजीव मय यह विश्व अनादि से चला आ रहा है और उसमें किसी बाह्य देवसत्ता के दखल बिना ही प्राकृतिक नियमानुसार असंख्य परिवर्तन होते ही रहते हैं। विश्व की विविधता का मूल पांच समवाय याने काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ में ही समाया हुआ है।"
इतना सब होते हुए भी जैनों के इस विश्वास ने उन्हें अविकास प्राप्त जड़वादी कि जिसे 'भौतिकवाद' कहा जाता है अथवा चार्वाक कि जिसका सिद्धान्त 'यावज्जीवेत सूखंजीवेत' है और जो 'भष्म हा शरीर फिर से जन्म नहीं लेता' मानता है, नहीं बनाया । श्री वास्त ने अपनी 'जैनीज्म' नामक पुस्तिका में जैनदर्शन और अन्य दर्शनों के विचारभेद को सुन्दर रीति से नीचे लिखे शब्दों में व्यक्त किया है । 'विश्व नियंता सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिद्धांत का एक विकल्प' वह विद्वान कहता है कि 'आत्महीन जड़वादी नास्तिकवाद का सिद्धांत है जो प्रतिपादन करता है कि जीव और चेतन भौतिक अणूत्रों की गति और स्कंध का परिणाम है जो कि मृत्यु समय में विचूर्णित हो जाते हैं। परन्तु जिन्हें इस प्रकार के किसी भी सिद्धांत से सन्तोष नहीं होता है उनके लिए पुस्तक में एक स्थूल रूपरेखा दी गई है कि जो न तो प्रात्मा के अस्तित्व का ही निषेध करता है और न शष्टिकर्ता की मान्यता को मान कर ही चलता है। परन्तु वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का आप विधाता बनाता है, प्रत्येक चेतन प्रात्मा के लिए मोक्ष का ध्येय बनाता है और उस शाश्वत सुख के प्रावश्यक साधन रूप अात्मविकास की सर्वोत्कृष्ट भूमिका में पहुंचने तक के समय के लिए सर्वोच्च त्याग आवश्यक कहता है।
1. लाठे, इन्ट्रोडक्शनटू जैनिज्म, पृ. 85-87; जिनसेन. प्रादिपुराण, अध्या. 3 । देखो भण्डारकर, रिपोर्ट शान संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट, 1883-1884, पृ. 118 । 2. राधाकृष्णन, वही, पृ. 330। 3. वारेन, जैनीज्म, पृ. 2 । 'हे मानव ! तू ही अपना मित्र है, फिर क्यों प्रपनेसे बाहर किसी मित्र की खोज करता है।' याकोबी, सेबुई, पुस्त. 22, पृ. 33 ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org