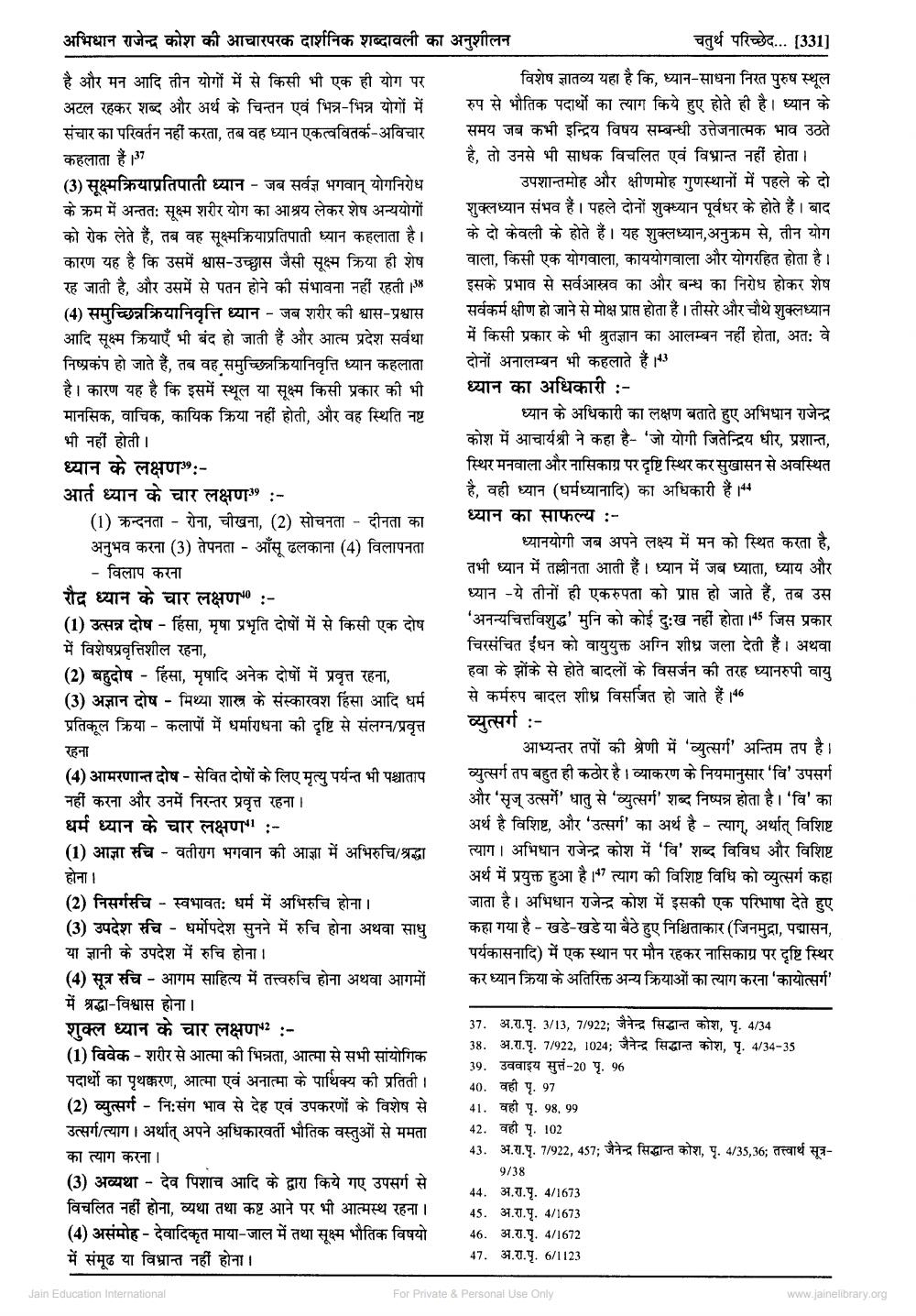________________
अभिधान राजेन्द्र कोश की आचारपरक दार्शनिक शब्दावली का अनुशीलन
चतुर्थ परिच्छेद... [331]
है और मन आदि तीन योगों में से किसी भी एक ही योग पर अटल रहकर शब्द और अर्थ के चिन्तन एवं भिन्न-भिन्न योगों में संचार का परिवर्तन नहीं करता, तब वह ध्यान एकत्ववितर्क-अविचार कहलाता है। (3) सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यान - जब सर्वज्ञ भगवान् योगनिरोध के क्रम में अन्ततः सूक्ष्म शरीर योग का आश्रय लेकर शेष अन्ययोगों को रोक लेते हैं, तब वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यान कहलाता है। कारण यह है कि उसमें श्वास-उच्छ्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया ही शेष रह जाती है, और उसमें से पतन होने की संभावना नहीं रहती।38 (4) समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति ध्यान - जब शरीर की श्वास-प्रश्वास आदि सूक्ष्म क्रियाएँ भी बंद हो जाती हैं और आत्म प्रदेश सर्वथा निष्प्रकंप हो जाते हैं, तब वह समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति ध्यान कहलाता है। कारण यह है कि इसमें स्थूल या सूक्ष्म किसी प्रकार की भी मानसिक, वाचिक, कायिक क्रिया नहीं होती, और वह स्थिति नष्ट भी नहीं होती। ध्यान के लक्षण :आर्त ध्यान के चार लक्षण :(1) क्रन्दनता - रोना, चीखना, (2) सोचनता - दीनता का अनुभव करना (3) तेपनता - आँसू ढलकाना (4) विलापनता - विलाप करना रौद्र ध्यान के चार लक्षण :(1) उत्सन्न दोष - हिंसा, मृषा प्रभृति दोषों में से किसी एक दोष में विशेषप्रवृत्तिशील रहना, (2) बहुदोष - हिंसा, मृषादि अनेक दोषों में प्रवृत्त रहना, (3) अज्ञान दोष - मिथ्या शास्त्र के संस्कारवश हिंसा आदि धर्म प्रतिकूल क्रिया - कलापों में धर्माराधना की दृष्टि से संलग्न/प्रवृत्त रहना (4) आमरणान्त दोष - सेवित दोषों के लिए मृत्यु पर्यन्त भी पश्चाताप नहीं करना और उनमें निरन्तर प्रवृत्त रहना। धर्म ध्यान के चार लक्षण" :(1) आज्ञा संचि - वतीराग भगवान की आज्ञा में अभिरुचि/श्रद्धा होना। (2) निसर्गसंच - स्वभावतः धर्म में अभिरुचि होना। (3) उपदेश चि - धर्मोपदेश सुनने में रुचि होना अथवा साधु या ज्ञानी के उपदेश में रुचि होना। (4) सूत्र संच - आगम साहित्य में तत्त्वरुचि होना अथवा आगमों में श्रद्धा-विश्वास होना। शुक्ल ध्यान के चार लक्षण :(1) विवेक - शरीर से आत्मा की भिन्नता, आत्मा से सभी सांयोगिक पदार्थो का पृथक्करण, आत्मा एवं अनात्मा के पार्थिक्य की प्रतिती। (2) व्युत्सर्ग - नि:संग भाव से देह एवं उपकरणों के विशेष से उत्सर्ग/त्याग । अर्थात् अपने अधिकारवर्ती भौतिक वस्तुओं से ममता का त्याग करना। (3) अव्यथा - देव पिशाच आदि के द्वारा किये गए उपसर्ग से विचलित नहीं होना, व्यथा तथा कष्ट आने पर भी आत्मस्थ रहना । (4) असंमोह- देवादिकृत माया-जाल में तथा सूक्ष्म भौतिक विषयो में संमूढ या विभ्रान्त नहीं होना।
__विशेष ज्ञातव्य यहा है कि, ध्यान-साधना निरत पुरुष स्थूल रुप से भौतिक पदार्थो का त्याग किये हुए होते ही है। ध्यान के समय जब कभी इन्द्रिय विषय सम्बन्धी उत्तेजनात्मक भाव उठते है, तो उनसे भी साधक विचलित एवं विभ्रान्त नहीं होता।
उपशान्तमोह और क्षीणमोह गुणस्थानों में पहले के दो शुक्लध्यान संभव हैं। पहले दोनों शुक्ध्यान पूर्वधर के होते हैं। बाद के दो केवली के होते हैं। यह शुक्लध्यान,अनुक्रम से, तीन योग वाला, किसी एक योगवाला, काययोगवाला और योगरहित होता है। इसके प्रभाव से सर्वआस्रव का और बन्ध का निरोध होकर शेष सर्वकर्म क्षीण हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता हैं। तीसरे और चौथे शुक्लध्यान में किसी प्रकार के भी श्रुतज्ञान का आलम्बन नहीं होता, अतः वे दोनों अनालम्बन भी कहलाते हैं।43 ध्यान का अधिकारी :
ध्यान के अधिकारी का लक्षण बताते हुए अभिधान राजेन्द्र कोश में आचार्यश्री ने कहा है- 'जो योगी जितेन्द्रिय धीर, प्रशान्त, स्थिर मनवाला और नासिकाग्र पर दृष्टि स्थिर कर सुखासन से अवस्थित है, वही ध्यान (धर्मध्यानादि) का अधिकारी हैं।44 ध्यान का साफल्य :
ध्यानयोगी जब अपने लक्ष्य में मन को स्थित करता है, तभी ध्यान में तल्लीनता आती हैं। ध्यान में जब ध्याता, ध्याय और ध्यान -ये तीनों ही एकरुपता को प्राप्त हो जाते हैं, तब उस 'अनन्यचित्तविशुद्ध' मुनि को कोई दुःख नहीं होता।45 जिस प्रकार चिरसंचित ईंधन को वायुयुक्त अग्नि शीध्र जला देती हैं। अथवा हवा के झोंके से होते बादलों के विसर्जन की तरह ध्यानरुपी वायु से कर्मरुप बादल शीध्र विसर्जित हो जाते हैं।46 व्युत्सर्ग :
आभ्यन्तर तपों की श्रेणी में 'व्युत्सर्ग' अन्तिम तप है। व्युत्सर्ग तप बहुत ही कठोर है। व्याकरण के नियमानुसार 'वि' उपसर्ग और 'सृज् उत्सर्गे' धातु से 'व्युत्सर्ग' शब्द निष्पन्न होता है। 'वि' का अर्थ है विशिष्ट, और 'उत्सर्ग' का अर्थ है - त्याग, अर्थात् विशिष्ट त्याग। अभिधान राजेन्द्र कोश में 'वि' शब्द विविध और विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। त्याग की विशिष्ट विधि को व्युत्सर्ग कहा जाता है। अभिधान राजेन्द्र कोश में इसकी एक परिभाषा देते हुए कहा गया है - खडे-खडे या बैठे हुए निश्चिताकार (जिनमुद्रा, पद्मासन, पर्यकासनादि) में एक स्थान पर मौन रहकर नासिकाग्र पर दृष्टि स्थिर कर ध्यान क्रिया के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं का त्याग करना 'कायोत्सर्ग'
37. अ.रा.पृ. 3/13, 7/922; जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, पृ. 4/34 38. अ.रा.पृ. 7/922, 1024; जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, पृ. 4/34-35 39. उववाइय सुत्तं-20 पृ. 96 40. वही पृ. 97 41. वही पृ. 98. 99
वही पृ. 102 43. अ.रा.पृ. 7/922, 457; जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, पृ. 4/35,36; तत्त्वार्थ सूत्र
9/38 44. अ.रा.पृ. 4/1673 45. अ.रा.पृ. 4/1673 46. अ.रा.पृ. 4/1672 47. अ.रा.पृ. 6/1123
42.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org