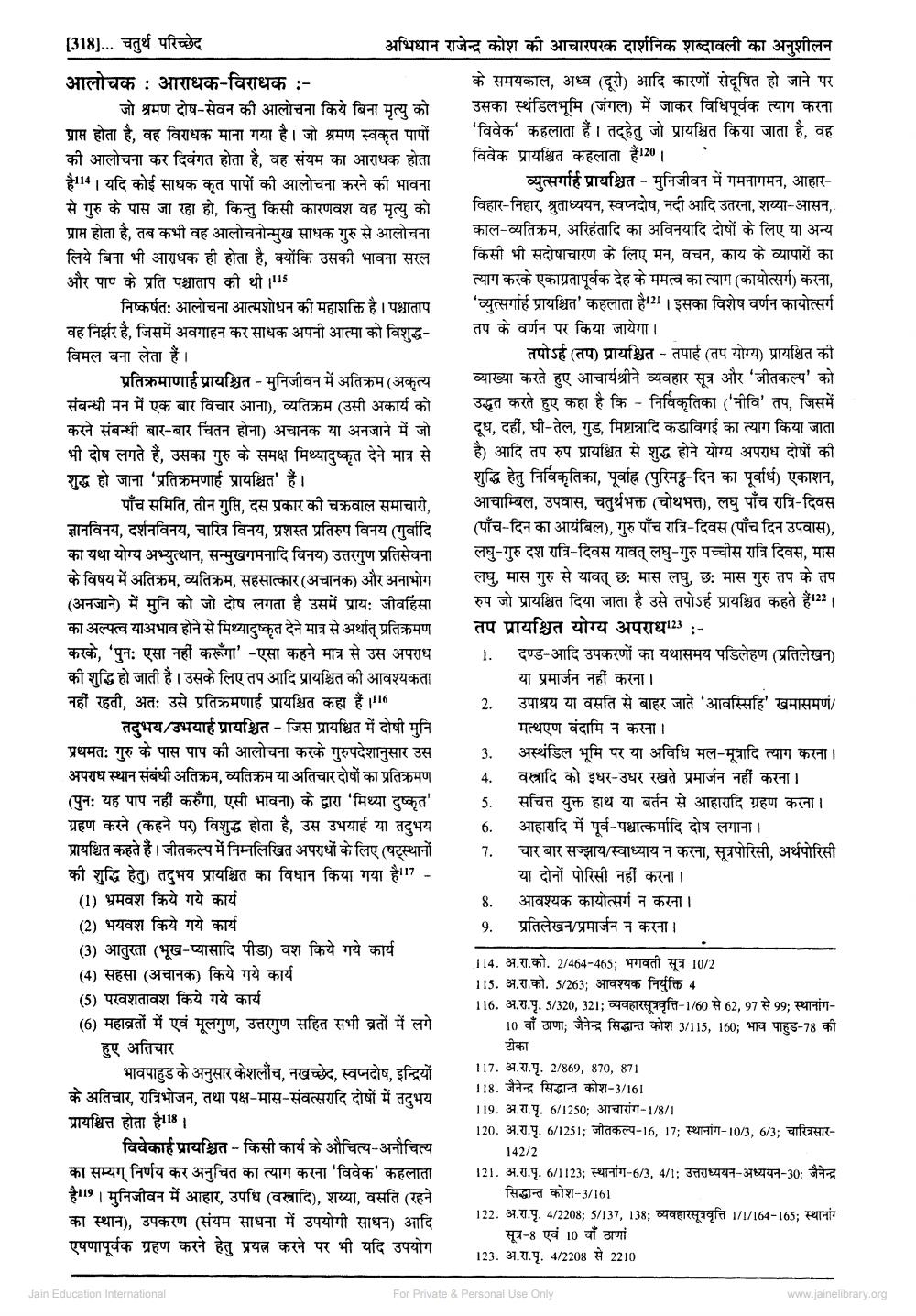________________
[318]... चतुर्थ परिच्छेद
अभिधान राजेन्द्र कोश की आचारपरक दार्शनिक शब्दावली का अनुशीलन आलोचक : आराधक-विराधक :
के समयकाल, अध्व (दूरी) आदि कारणों सेदूषित हो जाने पर जो श्रमण दोष-सेवन की आलोचना किये बिना मृत्यु को उसका स्थंडिलभूमि (जंगल) में जाकर विधिपूर्वक त्याग करना प्राप्त होता है, वह विराधक माना गया है। जो श्रमण स्वकृत पापों
'विवेक' कहलाता हैं। तद्हेतु जो प्रायश्चित किया जाता है, वह की आलोचना कर दिवंगत होता है, वह संयम का आराधक होता विवेक प्रायश्चित कहलाता हैं।20। है।14। यदि कोई साधक कृत पापों की आलोचना करने की भावना
व्युत्सर्हि प्रायश्चित - मुनिजीवन में गमनागमन, आहारसे गुरु के पास जा रहा हो, किन्तु किसी कारणवश वह मृत्यु को विहार-निहार, श्रुताध्ययन, स्वप्नदोष, नदी आदि उतरना, शय्या-आसन, प्राप्त होता है, तब कभी वह आलोचनोन्मुख साधक गुरु से आलोचना काल-व्यतिक्रम, अरिहंतादि का अविनयादि दोषों के लिए या अन्य लिये बिना भी आराधक ही होता है, क्योंकि उसकी भावना सरल किसी भी सदोषाचारण के लिए मन, वचन, काय के व्यापारों का और पाप के प्रति पश्चाताप की थी ।।15
त्याग करके एकाग्रतापूर्वक देह के ममत्व का त्याग (कायोत्सर्ग) करना, निष्कर्षत: आलोचना आत्मशोधन की महाशक्ति है। पश्चाताप 'व्युत्सर्गार्ह प्रायश्चित' कहलाता है।21 | इसका विशेष वर्णन कायोत्सर्ग वह निर्झर है, जिसमें अवगाहन कर साधक अपनी आत्मा को विशुद्ध- तप के वर्णन पर किया जायेगा। विमल बना लेता हैं।
तपोऽर्ह (तप) प्रायश्चित - तपार्ह (तप योग्य) प्रायश्चित की प्रतिक्रमाणार्ह प्रायश्चित - मुनिजीवन में अतिक्रम (अकृत्य व्याख्या करते हुए आचार्यश्रीने व्यवहार सूत्र और 'जीतकल्प' को संबन्धी मन में एक बार विचार आना), व्यतिक्रम (उसी अकार्य को उद्धृत करते हुए कहा है कि - निर्विकृतिका ('नीवि' तप, जिसमें करने संबन्धी बार-बार चिंतन होना) अचानक या अनजाने में जो दूध, दही, घी-तेल, गुड, मिष्टान्नादि कडाविगई का त्याग किया जाता भी दोष लगते हैं, उसका गुरु के समक्ष मिथ्यादुष्कृत देने मात्र से है) आदि तप रुप प्रायश्चित से शुद्ध होने योग्य अपराध दोषों की शुद्ध हो जाना 'प्रतिक्रमणाई प्रायश्चित' हैं।।
शुद्धि हेतु निविकृतिका, पूर्वाह्न (पुरिम-दिन का पूर्वार्ध) एकाशन, पाँच समिति, तीन गुप्ति, दस प्रकार की चक्रवाल समाचारी, आचाम्बिल, उपवास, चतुर्थभक्त (चोथभत्त), लघु पाँच रात्रि-दिवस ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्र विनय, प्रशस्त प्रतिरुप विनय (गुर्वादि (पाँच-दिन का आयंबिल), गुरु पाँच रात्रि-दिवस (पाँच दिन उपवास), का यथा योग्य अभ्युत्थान, सन्मुखगमनादि विनय) उत्तरगुण प्रतिसेवना लघु-गुरु दश रात्रि-दिवस यावत् लघु-गुरु पच्चीस रात्रि दिवस, मास के विषय में अतिक्रम, व्यतिक्रम, सहसात्कार (अचानक) और अनाभोग लघु, मास गुरु से यावत् छ: मास लघु, छ: मास गुरु तप के तप (अनजाने) में मुनि को जो दोष लगता है उसमें प्रायः जीवहिंसा रुप जो प्रायश्चित दिया जाता है उसे तपोऽहं प्रायश्चित कहते हैं।22 । का अल्पत्व याअभाव होने से मिथ्यादुष्कृत देने मात्र से अर्थात् प्रतिक्रमण तप प्रायश्चित योग्य अपराध:23 :करके, 'पुनः एसा नहीं करूंगा' -एसा कहने मात्र से उस अपराध 1. दण्ड-आदि उपकरणों का यथासमय पडिलेहण (प्रतिलेखन) की शुद्धि हो जाती है। उसके लिए तप आदि प्रायश्चित की आवश्यकता
या प्रमार्जन नहीं करना। नहीं रहती, अतः उसे प्रतिक्रमणार्ह प्रायश्चित कहा हैं ।।16
उपाश्रय या वसति से बाहर जाते 'आवस्सिहि' खमासमणं/ तदुभय/उभयाई प्रायश्चित - जिस प्रायश्चित में दोषी मुनि
मत्थएण वंदामि न करना। प्रथमतः गुरु के पास पाप की आलोचना करके गुरुपदेशानुसार उस
अस्थंडिल भूमि पर या अविधि मल-मूत्रादि त्याग करना। अपराध स्थान संबंधी अतिक्रम, व्यतिक्रम या अतिचार दोषों का प्रतिक्रमण
वस्त्रादि को इधर-उधर रखते प्रमार्जन नहीं करना। (पुन: यह पाप नहीं करूँगा, एसी भावना) के द्वारा 'मिथ्या दुष्कृत'
सचित्त युक्त हाथ या बर्तन से आहारादि ग्रहण करना। ग्रहण करने (कहने पर) विशुद्ध होता है, उस उभयार्ह या तदुभय आहारादि में पूर्व-पश्चात्कर्मादि दोष लगाना। प्रायश्चित कहते हैं। जीतकल्प में निम्नलिखित अपराधों के लिए (षट्स्थानों
चार बार सज्झाय/स्वाध्याय न करना, सूत्रपोरिसी, अर्थपोरिसी की शुद्धि हेतु) तदुभय प्रायश्चित का विधान किया गया है।17 -
या दोनों पोरिसी नहीं करना। (1) भ्रमवश किये गये कार्य
8. आवश्यक कायोत्सर्ग न करना। (2) भयवश किये गये कार्य
9. प्रतिलेखन/प्रमार्जन न करना। (3) आतुरता (भूख-प्यासादि पीडा) वश किये गये कार्य
114. अ.रा.को. 2/464-465; भगवती सूत्र 10/2 (4) सहसा (अचानक) किये गये कार्य
115. अ.रा.को. 5/263; आवश्यक नियुक्ति 4 (5) परवशतावश किये गये कार्य
116, अ.रा.पृ. 5/320, 321; व्यवहारसूत्रवृत्ति-1/60 से 62, 97 से 99; स्थानांग(6) महाव्रतों में एवं मूलगुण, उत्तरगुण सहित सभी व्रतों में लगे 10 वाँ ठाणा; जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 3/115, 160; भाव पाहुड-78 की हुए अतिचार
टीका भावपाहुड के अनुसार केशलौंच, नखच्छेद, स्वप्नदोष, इन्द्रियों
117. अ.रा.पृ. 2/869,870,871 के अतिचार, रात्रिभोजन, तथा पक्ष-मास-संवत्सरादि दोषों में तदुभय
118. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश-3/161
119. अ.रा.पृ. 6/1250; आचारांग-1/8/1 प्रायश्चित्त होता है।
120. अ.रा.पृ. 6/1251; जीतकल्प-16, 173 स्थानांग-10/3, 6/3; चारित्रसारविवेकाह प्रायश्चित- किसी कार्य के औचित्य-अनौचित्य
142/2 का सम्यग् निर्णय कर अनुचित का त्याग करना 'विवेक' कहलाता 121. अ.रा.पृ. 6/1123; स्थानांग-6/3, 4/1; उत्तराध्ययन-अध्ययन-30; जैनेन्द्र है। । मुनिजीवन में आहार, उपधि (वस्त्रादि), शय्या, वसति (रहने
सिद्धान्त कोश-3/161 का स्थान), उपकरण (संयम साधना में उपयोगी साधन) आदि
122. अ.रा.पृ. 4/2208; 5/137, 138; व्यवहारसूत्रवृत्ति 1/1/164-165; स्थानांग
सूत्र-8 एवं 10 वाँ ठाणां एषणापूर्वक ग्रहण करने हेतु प्रयत्न करने पर भी यदि उपयोग
123. अ.रा.पृ. 4/2208 से 2210
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org