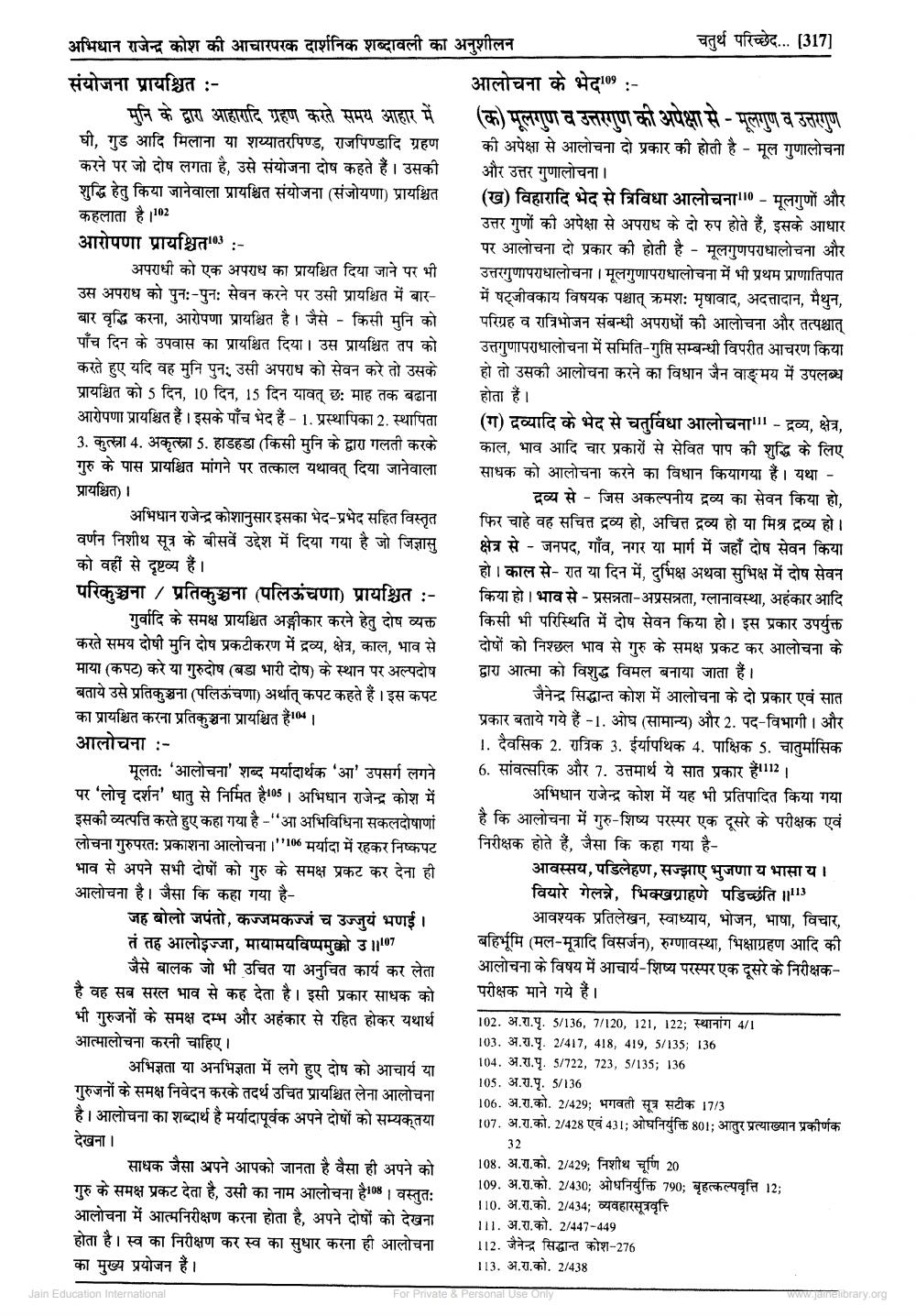________________
चतुर्थ परिच्छेद... [317] अभिधान राजेन्द्र कोश की आचारपरक दार्शनिक शब्दावली का अनुशीलन संयोजना प्रायश्चित :
आलोचना के भेद :____ मुनि के द्वारा आहारादि ग्रहण करते समय आहार में (क) मूलगुण व उत्तरगुण की अपेक्षा से - मूलगुण व उत्तरगुण घी, गुड आदि मिलाना या शय्यातरपिण्ड, राजपिण्डादि ग्रहण की अपेक्षा से आलोचना दो प्रकार की होती है - मूल गुणालोचना करने पर जो दोष लगता है, उसे संयोजना दोष कहते हैं। उसकी और उत्तर गुणालोचना। शुद्धि हेतु किया जानेवाला प्रायश्चित संयोजना (संजोयणा) प्रायश्चित (ख) विहारादि भेद से त्रिविधा आलोचना।10 - मूलगुणों और कहलाता है।102
उत्तर गुणों की अपेक्षा से अपराध के दो रुप होते हैं, इसके आधार आरोपणा प्रायश्चित :
पर आलोचना दो प्रकार की होती है - मूलगुणपराधालोचना और अपराधी को एक अपराध का प्रायश्चित दिया जाने पर भी उत्तरगुणापराधालोचना । मूलगुणापराधालोचना में भी प्रथम प्राणातिपात उस अपराध को पुनः-पुनः सेवन करने पर उसी प्रायश्चित में बार- में षट्जीवकाय विषयक पश्चात् क्रमशः मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, बार वृद्धि करना, आरोपणा प्रायश्चित है। जैसे - किसी मुनि को परिग्रह व रात्रिभोजन संबन्धी अपराधों की आलोचना और तत्पश्चात् पाँच दिन के उपवास का प्रायश्चित दिया। उस प्रायश्चित तप को उत्तगुणापराधालोचना में समिति-गुप्ति सम्बन्धी विपरीत आचरण किया करते हुए यदि वह मुनि पुनः उसी अपराध को सेवन करे तो उसके हो तो उसकी आलोचना करने का विधान जैन वाङ्मय में उपलब्ध प्रायश्चित को 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन यावत् छ: माह तक बढाना होता हैं। आरोपणा प्रायश्चित हैं। इसके पाँच भेद हैं - 1. प्रस्थापिका 2. स्थापिता (ग) द्रव्यादि के भेद से चतुर्विधा आलोचना|| - द्रव्य, क्षेत्र, 3. कुत्स्ना 4. अकृत्स्ना 5. हाडहडा (किसी मुनि के द्वारा गलती करके काल, भाव आदि चार प्रकारों से सेवित पाप की शुद्धि के लिए गुरु के पास प्रायश्चित मांगने पर तत्काल यथावत् दिया जानेवाला साधक को आलोचना करने का विधान कियागया हैं। यथा - प्रायश्चित)।
दव्य से - जिस अकल्पनीय द्रव्य का सेवन किया हो, अभिधान राजेन्द्र कोशानुसार इसका भेद-प्रभेद सहित विस्तृत फिर चाहे वह सचित्त द्रव्य हो, अचित्त द्रव्य हो या मिश्र द्रव्य हो। वर्णन निशीथ सूत्र के बीसवें उद्देश में दिया गया है जो जिज्ञासु क्षेत्र से - जनपद, गाँव, नगर या मार्ग में जहाँ दोष सेवन किया को वहीं से दृष्टव्य हैं।
हो । काल से- रात या दिन में, दुर्भिक्ष अथवा सुभिक्ष में दोष सेवन परिकुञ्चना / प्रतिकुञ्चना (पलिऊंचणा) प्रायश्चित :- किया हो। भाव से - प्रसन्नता-अप्रसन्नता, ग्लानावस्था, अहंकार आदि
गुर्वादि के समक्ष प्रायश्चित अङ्गीकार करने हेतु दोष व्यक्त किसी भी परिस्थिति में दोष सेवन किया हो। इस प्रकार उपर्युक्त करते समय दोषी मुनि दोष प्रकटीकरण में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से दोषों को निश्छल भाव से गुरु के समक्ष प्रकट कर आलोचना के माया (कपट) करे या गुरुदोष (बडा भारी दोष) के स्थान पर अल्पदोष द्वारा आत्मा को विशुद्ध विमल बनाया जाता हैं। बताये उसे प्रतिकुञ्चना (पलिऊंचणा) अर्थात् कपट कहते हैं । इस कपट
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश में आलोचना के दो प्रकार एवं सात का प्रायश्चित करना प्रतिकुञ्चना प्रायश्चित है।।
प्रकार बताये गये हैं -1. ओघ (सामान्य) और 2. पद-विभागी। और आलोचना :
1. दैवसिक 2. रात्रिक 3. ईर्यापथिक 4. पाक्षिक 5. चातुर्मासिक मूलतः 'आलोचना' शब्द मर्यादार्थक 'आ' उपसर्ग लगने
6. सांवत्सरिक और 7. उत्तमार्थ ये सात प्रकार हैं।12। पर 'लोचू दर्शन' धातु से निर्मित है105 | अभिधान राजेन्द्र कोश में
अभिधान राजेन्द्र कोश में यह भी प्रतिपादित किया गया इसकी व्यत्पत्ति करते हुए कहा गया है -"आ अभिविधिना सकलदोषाणां
है कि आलोचना में गुरु-शिष्य परस्पर एक दूसरे के परीक्षक एवं लोचना गुरुपरतः प्रकाशना आलोचना।"106 मर्यादा में रहकर निष्कपट
निरीक्षक होते हैं, जैसा कि कहा गया हैभाव से अपने सभी दोषों को गुरु के समक्ष प्रकट कर देना ही
आवस्सय, पडिलेहण, सज्झाए भुजणा य भासा य । आलोचना है। जैसा कि कहा गया है
वियारे गेलन्ने, भिक्खग्राहणे पडिच्छंति ॥10 जह बोलो जपंतो, कज्जमकज्जं च उज्जुयं भणई।
आवश्यक प्रतिलेखन, स्वाध्याय, भोजन, भाषा, विचार, तं तह आलोइज्जा, मायामयविप्पमुक्को उ॥107
बहिर्भूमि (मल-मूत्रादि विसर्जन), रुग्णावस्था, भिक्षाग्रहण आदि की जैसे बालक जो भी उचित या अनुचित कार्य कर लेता
आलोचना के विषय में आचार्य-शिष्य परस्पर एक दूसरे के निरीक्षकहै वह सब सरल भाव से कह देता है। इसी प्रकार साधक को
परीक्षक माने गये हैं। भी गुरुजनों के समक्ष दम्भ और अहंकार से रहित होकर यथार्थ 102. अ.रा.पृ. 5/136, 7/120, 121, 122; स्थानांग 4/1 आत्मालोचना करनी चाहिए।
103. अ.रा.पृ. 2/417, 418, 419, 5/135; 136 अभिज्ञता या अनभिज्ञता में लगे हुए दोष को आचार्य या
104. अ.रा.पृ. 5/722, 723, 5/1353; 136
105. अ.रा.पृ. 5/136 गुरुजनों के समक्ष निवेदन करके तदर्थ उचित प्रायश्चित लेना आलोचना
106. अ.रा.को. 2/429; भगवती सूत्र सटीक 17/3 है। आलोचना का शब्दार्थ है मर्यादापूर्वक अपने दोषों को सम्यक्तया 107. अ.रा.को. 2/428 एवं 431; ओघनियुक्ति 801; आतुर प्रत्याख्यान प्रकीर्णक देखना। साधक जैसा अपने आपको जानता है वैसा ही अपने को
108. अ.रा.को. 2/429; निशीथ चूणि 20
109. अ.रा.को. 2/430; ओधनियुक्ति 790; बृहत्कल्पवृत्ति 12; गुरु के समक्ष प्रकट देता है, उसी का नाम आलोचना है108 । वस्तुतः
110. अ.रा.को. 2/434; व्यवहारसूत्रवृत्ति आलोचना में आत्मनिरीक्षण करना होता है, अपने दोषों को देखना
111. अ.रा.को. 2/447-449 होता है। स्व का निरीक्षण कर स्व का सुधार करना ही आलोचना 112. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश-276 का मुख्य प्रयोजन हैं।
113. अ.रा.को. 2/438 For Private & Personal use only
www.atelibrary.org
Jain Education International