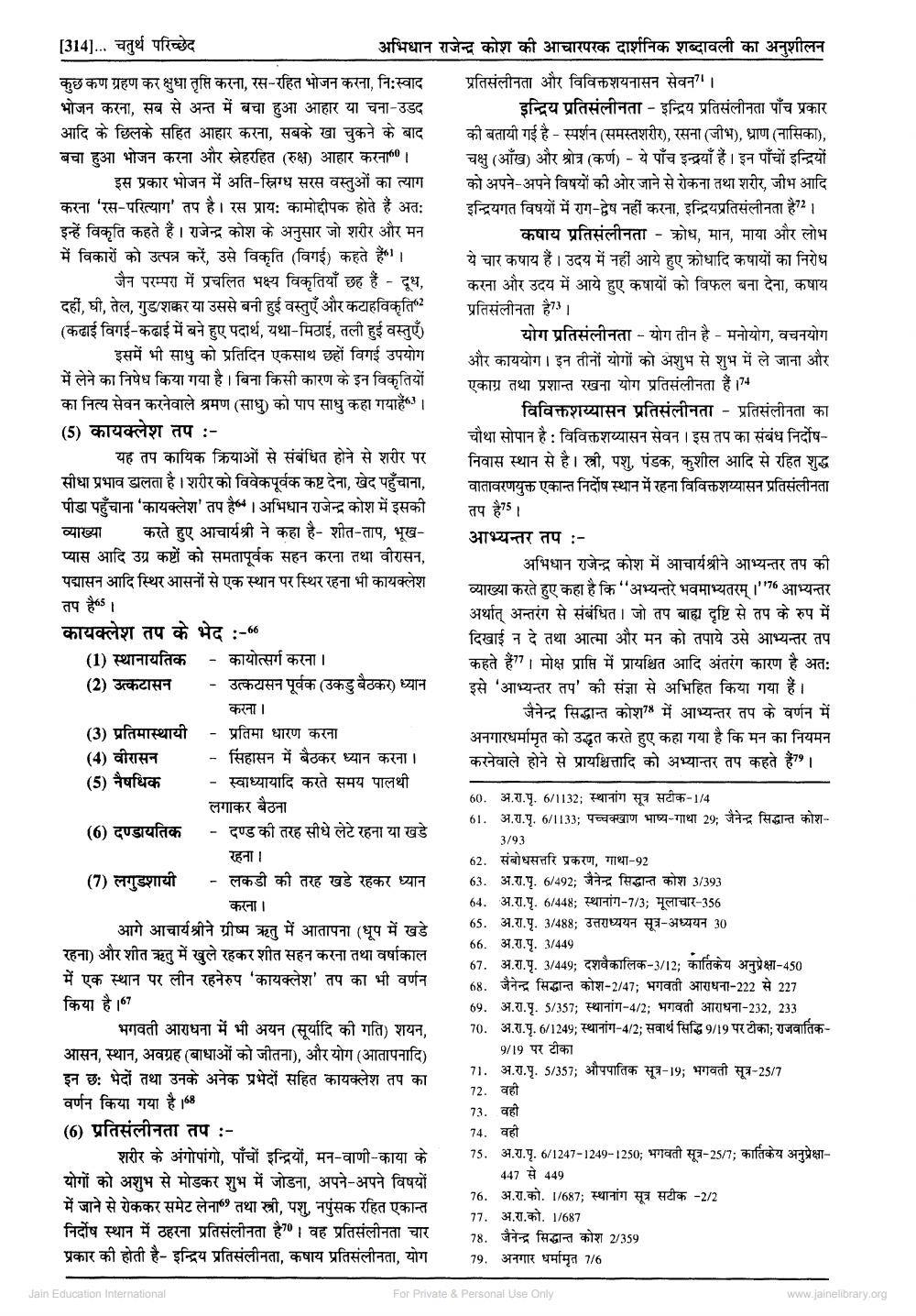________________
[314]... चतुर्थ परिच्छेद
कुछ कण ग्रहण कर क्षुधा तृप्ति करना, रस-रहित भोजन करना, निःस्वाद भोजन करना, सब से अन्त में बचा हुआ आहार या चना - उडद आदि के छिलके सहित आहार करना, सबके खा चुकने के बाद बचा हुआ भोजन करना और स्नेहरहित (रुक्ष) आहार करना" ।
अभिधान राजेन्द्र कोश की आचारपरक दार्शनिक शब्दावली का अनुशीलन प्रतिसंलीनता और विविक्तशयनासन सेवन ' ' ।
इन्द्रिय प्रतिसंलीनता - इन्द्रिय प्रतिसंलीनता पाँच प्रकार की बतायी गई है - स्पर्शन (समस्तशरीर), रसना (जीभ), ध्राण (नासिका), चक्षु (आँख) और श्रोत्र (कर्ण) - ये पाँच इन्द्रयाँ हैं। इन पाँचों इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों की ओर जाने से रोकना तथा शरीर, जीभ आदि इन्द्रियगत विषयों में राग-द्वेष नहीं करना, इन्द्रियप्रतिसंलीनता है 72 ।
इस प्रकार भोजन में अति स्निग्ध सरस वस्तुओं का त्याग करना 'रस- परित्याग' तप है। रस प्रायः कामोद्दीपक होते हैं अतः इन्हें विकृति कहते हैं । राजेन्द्र कोश के अनुसार जो शरीर और मन में विकारों को उत्पन्न करें, उसे विकृति (विगई) कहते हैं" ।
जैन परम्परा में प्रचलित भक्ष्य विकृतियाँ छह हैं- दूध, दहीं, घी, तेल, गुड/ शक्कर या उससे बनी हुई वस्तुएँ और कटाहविकृति "2 (कढाई विगई- कढाई में बने हुए पदार्थ, यथा-मिठाई, तली हुई वस्तुएँ)
इसमें भी साधु को प्रतिदिन एकसाथ छहों विगई उपयोग में लेने का निषेध किया गया है। बिना किसी कारण के इन विकृतियों का नित्य सेवन करनेवाले श्रमण (साधु) को पाप साधु कहा गया है। (5) कायक्लेश तप :
यह तप कायिक क्रियाओं से संबंधित होने से शरीर पर सीधा प्रभाव डालता है। शरीर को विवेकपूर्वक कष्ट देना, खेद पहुँचाना, पीडा पहुँचाना 'कायक्लेश' तप है" । अभिधान राजेन्द्र कोश में इसकी व्याख्या करते हुए आचार्यश्री ने कहा है- शीत- ताप, भूखप्यास आदि उग्र कष्टों को समतापूर्वक सहन करना तथा वीरासन, पद्मासन आदि स्थिर आसनों से एक स्थान पर स्थिर रहना भी कायक्लेश तप है । कायक्लेश तप के भेद :- 6 (1) स्थानायतिक
कायोत्सर्ग करना ।
(2) उत्कटासन
उत्कटासन पूर्वक (उकडु बैठकर) ध्यान
करना ।
प्रतिमा धारण करना
सिंहासन में बैठकर ध्यान करना । स्वाध्यायादि करते समय पालथी लगाकर बैठना
दण्ड की तरह सीधे लेटे रहना या खडे रहना ।
लकड़ी की तरह खड़े रहकर ध्यान
(3) प्रतिमास्थायी (4) वीरासन
(5) नैषधिक
(6) दण्डायतिक
(7) लगुडशायी
करना ।
आगे आचार्य श्रीने ग्रीष्म ऋतु में आतापना (धूप में खडे रहना) और शीत ऋतु में खुले रहकर शीत सहन करना तथा वर्षाकाल में एक स्थान पर लीन रहनेरुप 'कायक्लेश' तप का भी वर्णन किया है। 67
भगवती आराधना में भी अयन (सूर्यादि की गति) शयन, आसन, स्थान, अवग्रह (बाधाओं को जीतना), और योग (आतापनादि) इन छः भेदों तथा उनके अनेक प्रभेदों सहित कायक्लेश तप का वर्णन किया गया है। 68
Jain Education International
(6) प्रतिसंलीनता तप :
शरीर के अंगोपांगो, पाँचों इन्द्रियों, मन-वाणी-काया के योगों को अशुभ से मोडकर शुभ में जोडना, अपने-अपने विषयों में जाने से रोककर समेट लेना तथा स्त्री, पशु, नपुंसक रहित एकान्त निर्दोष स्थान में ठहरना प्रतिसंलीनता है। वह प्रतिसंलीनता चार प्रकार की होती है- इन्द्रिय प्रतिसंलीनता, कषाय प्रतिसंलीनता, योग
कषाय प्रतिसंलीनता क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय हैं। उदय में नहीं आये हुए क्रोधादि कषायों का निरोध करना और उदय में आये हुए कषायों को विफल बना देना, कषाय प्रतिसंलीनता है 73 |
योग प्रतिसंलीनता - योग तीन है मनोयोग, वचनयोग और काययोग। इन तीनों योगों को अशुभ से शुभ में ले जाना और एकाग्र तथा प्रशान्त रखना योग प्रतिसंलीनता हैं। 74
विविक्तशय्यासन प्रतिसंलीनता प्रतिसंलीनता का चौथा सोपान है : विविक्तशय्यासन सेवन । इस तप का संबंध निर्दोषनिवास स्थान से है। स्त्री, पशु, पंडक, कुशील आदि से रहित शुद्ध वातावरणयुक्त एकान्त निर्दोष स्थान में रहना विविक्तशय्यासन प्रतिसंलीनता तप है 75
आभ्यन्तर तप :
अभिधान राजेन्द्र कोश में आचार्यश्रीने आभ्यन्तर तप की व्याख्या करते हुए कहा है कि "अभ्यन्तरे भवमाभ्यतरम् । 76 आभ्यन्तर अर्थात् अन्तरंग से संबंधित । जो तप बाह्य दृष्टि से तप के रुप में दिखाई न दे तथा आत्मा और मन को तपाये उसे आभ्यन्तर तप कहते हैं " । मोक्ष प्राप्ति में प्रायश्चित आदि अंतरंग कारण है अतः इसे 'आभ्यन्तर तप' की संज्ञा से अभिहित किया गया है।
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश" में आभ्यन्तर तप के वर्णन में अनगारधर्मामृत को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि मन का नियमन करनेवाले होने से प्रायश्चित्तादि को अभ्यान्तर तप कहते हैं" ।
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
अ.रा.पू. 6/1132; स्थानांग सूत्र सटीक - 1/4
अ. रा.पू. 6/1133; पच्चक्खाण भाष्य-गाथा 29; जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश
3/93
संबोधसत्तरि प्रकरण, गाथा - 92
अ.रा. पृ. 6/492; जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 3/393
अ.रा. पृ. 6/448; स्थानांग-7/3; मूलाचार - 356
अ.रा. पृ. 3/488; उत्तराध्ययन सूत्र - अध्ययन 30 अ.रा. पृ. 3/449
अ.रा. पृ. 3/449; दशवैकालिक - 3 / 12; कार्तिकेय अनुप्रेक्षा - 450 जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश-2/47; भगवती आराधना-222 से 227
अ. रा. पृ. 5/357; स्थानांग - 4/2; भगवती आराधना-232, 233
अ.रा. पृ. 6/1249; स्थानांग - 4/2; सवार्थ सिद्धि 9/19 पर टीका; राजवार्तिक9/19 पर टीका
71. अ. रा. पृ. 5/357; औपपातिक सूत्र- 19; भगवती सूत्र - 25/7 72. वही
73. वही
74. वही
75.
अ. रा. पृ. 6/1247-1249-1250; भगवती सूत्र - 25/7; कार्तिकेय अनुप्रेक्षा447 से 449
76. अ.रा.को. 1/687; स्थानांग सूत्र सटीक - 2/2
77.
अ.रा.को. 1/687
78.
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 2/359
79.
अनगार धर्मामृत 7/6
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org