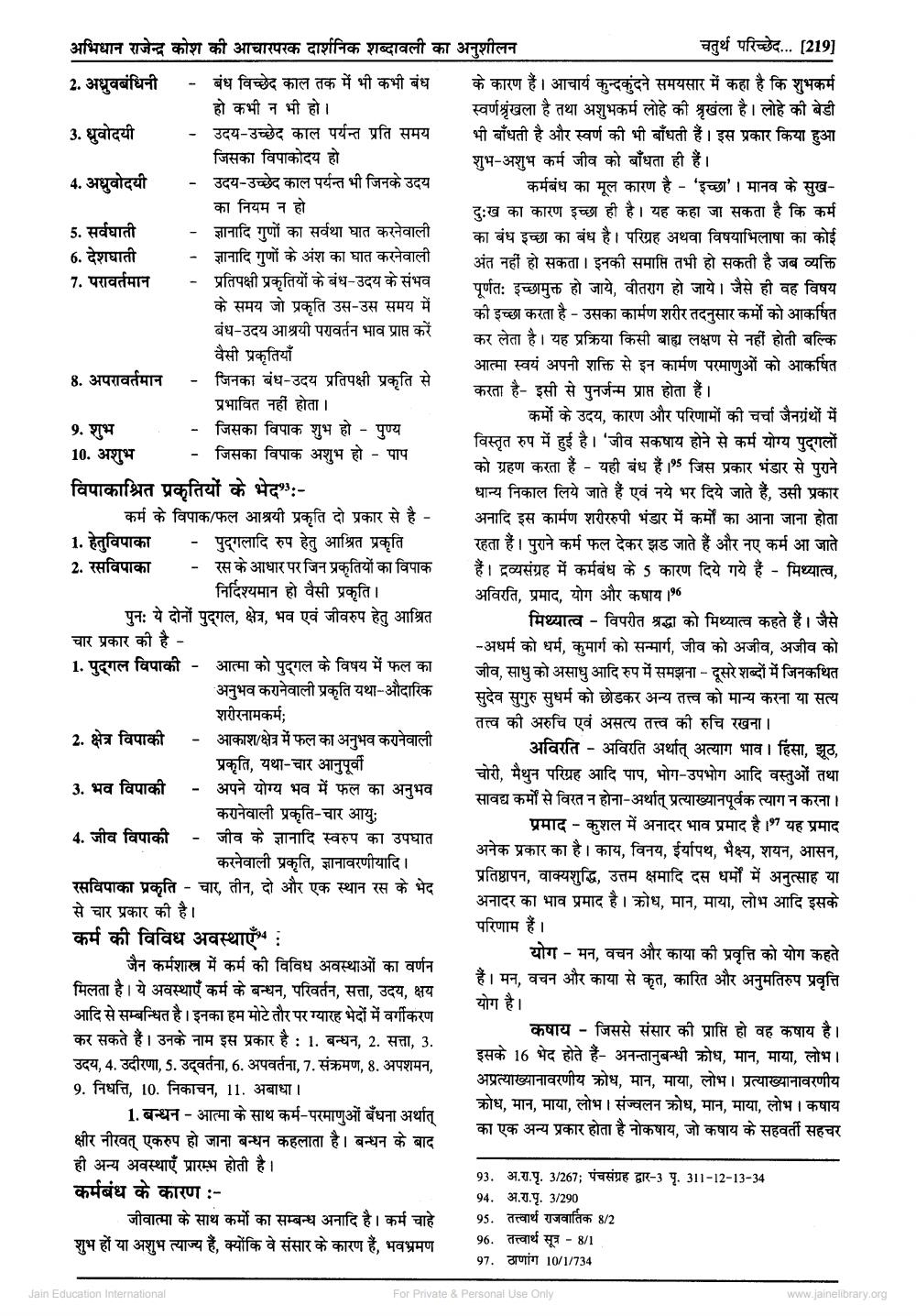________________
अभिधान राजेन्द्र कोश की आचारपरक दार्शनिक शब्दावली का अनुशीलन
चतुर्थ परिच्छेद... [219] 2. अध्रुवबंधिनी - बंध विच्छेद काल तक में भी कभी बंध के कारण हैं। आचार्य कुन्दकुंदने समयसार में कहा है कि शुभकर्म हो कभी न भी हो।
स्वर्णश्रृंखला है तथा अशुभकर्म लोहे की श्रृखंला है। लोहे की बेडी 3. ध्रुवोदयी उदय-उच्छेद काल पर्यन्त प्रति समय भी बाँधती है और स्वर्ण की भी बाँधती हैं। इस प्रकार किया हुआ जिसका विपाकोदय हो
शुभ-अशुभ कर्म जीव को बाँधता ही हैं। 4. अध्रुवोदयी - उदय-उच्छेद काल पर्यन्त भी जिनके उदय
कर्मबंध का मूल कारण है - 'इच्छा' । मानव के सुखका नियम न हो
दुःख का कारण इच्छा ही है। यह कहा जा सकता है कि कर्म 5. सर्वघाती - ज्ञानादि गुणों का सर्वथा घात करनेवाली
का बंध इच्छा का बंध है। परिग्रह अथवा विषयाभिलाषा का कोई 6. देशघाती - ज्ञानादि गुणों के अंश का घात करनेवाली
अंत नहीं हो सकता। इनकी समाप्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति 7. परावर्तमान प्रतिपक्षी प्रकृतियों के बंध-उदय के संभव
पूर्णतः इच्छामुक्त हो जाये, वीतराग हो जाये। जैसे ही वह विषय के समय जो प्रकृति उस-उस समय में
की इच्छा करता है - उसका कार्मण शरीर तदनुसार कर्मो को आकर्षित बंध-उदय आश्रयी परावर्तन भाव प्राप्त करें
कर लेता है। यह प्रक्रिया किसी बाह्य लक्षण से नहीं होती बल्कि वैसी प्रकृतियाँ
आत्मा स्वयं अपनी शक्ति से इन कार्मण परमाणुओं को आकर्षित 8. अपरावर्तमान - जिनका बंध-उदय प्रतिपक्षी प्रकृति से
करता है- इसी से पुनर्जन्म प्राप्त होता हैं। प्रभावित नहीं होता।
कर्मो के उदय, कारण और परिणामों की चर्चा जैनग्रंथों में 9. शुभ . - जिसका विपाक शुभ हो - पुण्य
विस्तृत रुप में हुई है। 'जीव सकषाय होने से कर्म योग्य पुद्गलों 10. अशुभ - जिसका विपाक अशुभ हो - पाप
को ग्रहण करता हैं - यही बंध हैं। जिस प्रकार भंडार से पुराने विपाकाश्रित प्रकृतियों के भेद::
धान्य निकाल लिये जाते हैं एवं नये भर दिये जाते हैं, उसी प्रकार कर्म के विपाक/फल आश्रयी प्रकृति दो प्रकार से है - अनादि इस कार्मण शरीररुपी भंडार में कर्मों का आना जाना होता 1. हेतुविपाका - पुद्गलादि रुप हेतु आश्रित प्रकृति रहता हैं। पुराने कर्म फल देकर झड जाते हैं और नए कर्म आ जाते 2. रसविपाका - रस के आधार पर जिन प्रकृतियों का विपाक हैं। द्रव्यसंग्रह में कर्मबंध के 5 कारण दिये गये हैं - मिथ्यात्व, निर्दिश्यमान हो वैसी प्रकृति।
अविरति, प्रमाद, योग और कषाय। पुन: ये दोनों पुद्गल, क्षेत्र, भव एवं जीवरुप हेतु आश्रित
मिथ्यात्व - विपरीत श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे चार प्रकार की है -
-अधर्म को धर्म, कुमार्ग को सन्मार्ग, जीव को अजीव, अजीव को 1. पुद्गल विपाकी - आत्मा को पुद्गल के विषय में फल का
जीव, साधु को असाधु आदि रुप में समझना - दूसरे शब्दों में जिनकथित अनुभव करानेवाली प्रकृति यथा-औदारिक
सुदेव सुगुरु सुधर्म को छोडकर अन्य तत्त्व को मान्य करना या सत्य शरीरनामकर्म;
तत्त्व की अरुचि एवं असत्य तत्त्व की रुचि रखना। 2. क्षेत्र विपाकी - आकाश/क्षेत्र में फल का अनुभव करानेवाली
अविरति - अविरति अर्थात् अत्याग भाव। हिंसा, झूठ, प्रकृति, यथा-चार आनुपूर्वी
चोरी, मैथुन परिग्रह आदि पाप, भोग-उपभोग आदि वस्तुओं तथा 3. भव विपाकी - अपने योग्य भव में फल का अनुभव
सावध कर्मों से विरत न होना-अर्थात् प्रत्याख्यानपूर्वक त्याग न करना। करानेवाली प्रकृति-चार आयु;
प्रमाद - कुशल में अनादर भाव प्रमाद है। यह प्रमाद 4. जीव विपाकी - जीव के ज्ञानादि स्वरुप का उपघात
अनेक प्रकार का है। काय, विनय, ईर्यापथ, भैक्ष्य, शयन, आसन, करनेवाली प्रकृति, ज्ञानावरणीयादि।
प्रतिष्ठापन, वाक्यशुद्धि, उत्तम क्षमादि दस धर्मों में अनुत्साह या रसविपाका प्रकृति - चार, तीन, दो और एक स्थान रस के भेद
अनादर का भाव प्रमाद है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि इसके से चार प्रकार की है।
परिणाम हैं। कर्म की विविध अवस्थाएँ:
योग - मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को योग कहते जैन कर्मशास्त्र में कर्म की विविध अवस्थाओं का वर्णन
हैं। मन, वचन और काया से कृत, कारित और अनुमतिरुप प्रवृत्ति मिलता है। ये अवस्थाएँ कर्म के बन्धन, परिवर्तन, सत्ता, उदय, क्षय
योग है। आदि से सम्बन्धित है। इनका हम मोटे तौर पर ग्यारह भेदों में वर्गीकरण
कषाय - जिससे संसार की प्राप्ति हो वह कषाय है। कर सकते हैं। उनके नाम इस प्रकार है : 1. बन्धन, 2. सत्ता, 3. उदय, 4. उदीरणा, 5. उद्वर्तना, 6. अपवर्तना, 7. संक्रमण, 8. अपशमन,
इसके 16 भेद होते हैं- अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ । 9. निधत्ति, 10. निकाचन, 11. अबाधा ।
अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ । प्रत्याख्यानावरणीय
क्रोध, मान, माया, लोभ । संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ । कषाय 1.बन्धन- आत्मा के साथ कर्म-परमाणुओं बँधना अर्थात्
का एक अन्य प्रकार होता है नोकषाय, जो कषाय के सहवर्ती सहचर क्षीर नीरवत् एकरुप हो जाना बन्धन कहलाता है। बन्धन के बाद ही अन्य अवस्थाएँ प्रारम्भ होती है।
93. अ.रा.पृ. 3/2673; पंचसंग्रह द्वार-3 पृ. 311-12-13-34 कर्मबंध के कारण :
94. अ.रा.पृ. 3/290 जीवात्मा के साथ कर्मो का सम्बन्ध अनादि है। कर्म चाहे 95. तत्त्वार्थ राजवार्तिक 8/2 शुभ हों या अशुभ त्याज्य हैं, क्योंकि वे संसार के कारण हैं, भवभ्रमण
96. तत्त्वार्थ सूत्र - 8/1 97. ठाणांग 10/1/734
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org