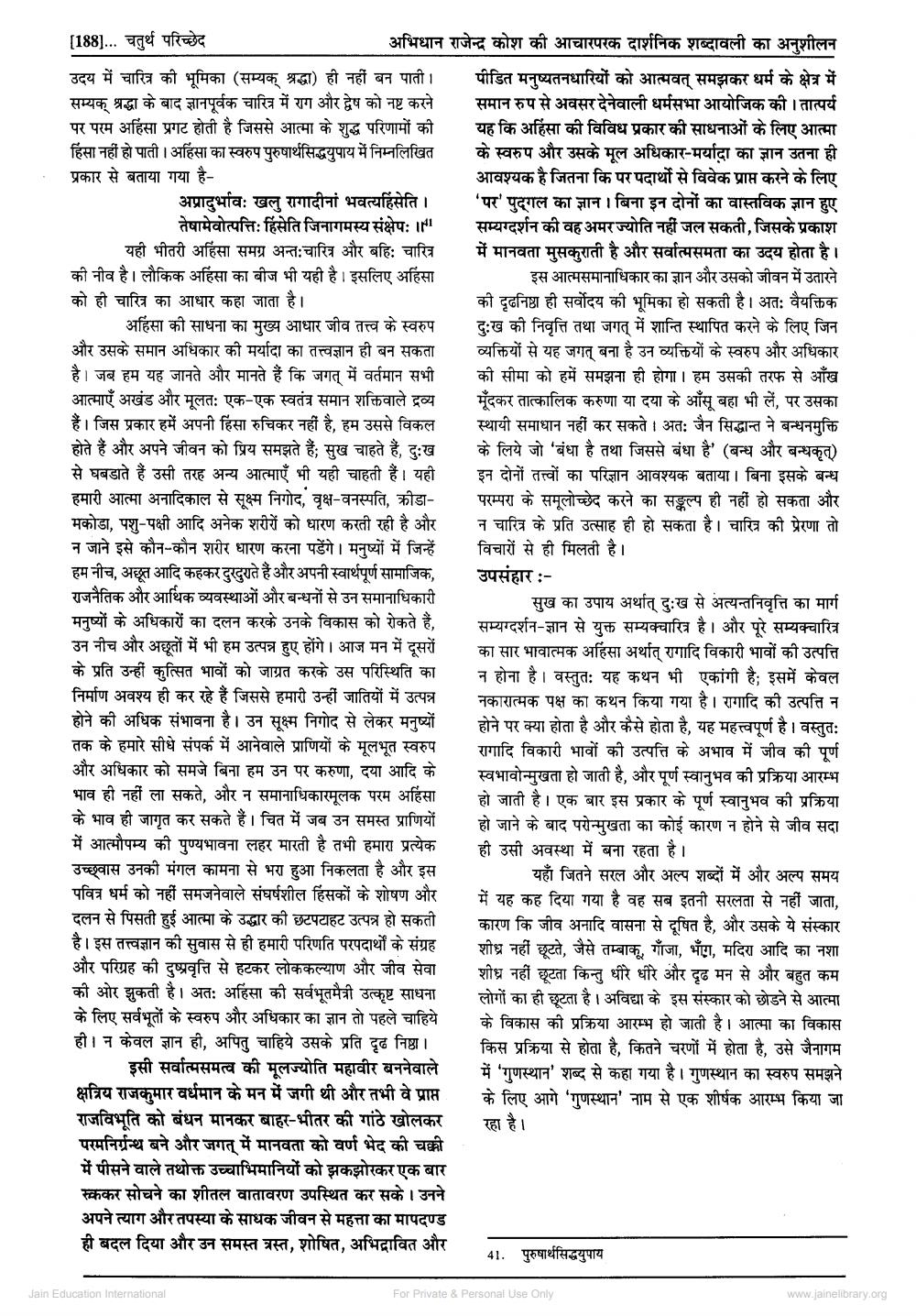________________
[188]... चतुर्थ परिच्छेद
अभिधान राजेन्द्र कोश की आचारपरक दार्शनिक शब्दावली का अनुशीलन उदय में चारित्र की भूमिका (सम्यक् श्रद्धा) ही नहीं बन पाती। पीडित मनुष्यतनधारियों को आत्मवत् समझकर धर्म के क्षेत्र में सम्यक् श्रद्धा के बाद ज्ञानपूर्वक चारित्र में राग और द्वेष को नष्ट करने समान रूप से अवसर देनेवाली धर्मसभा आयोजिक की। तात्पर्य पर परम अहिंसा प्रगट होती है जिससे आत्मा के शुद्ध परिणामों की यह कि अहिंसा की विविध प्रकार की साधनाओं के लिए आत्मा हिंसा नहीं हो पाती । अहिंसा का स्वरुप पुरुषार्थसिद्धयुपाय में निम्नलिखित के स्वरुप और उसके मूल अधिकार-मर्यादा का ज्ञान उतना ही प्रकार से बताया गया है
आवश्यक है जितना कि पर पदार्थो से विवेक प्राप्त करने के लिए अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति । 'पर' पुद्गल का ज्ञान । बिना इन दोनों का वास्तविक ज्ञान हुए
तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ।। सम्यग्दर्शन की वह अमरज्योति नहीं जल सकती, जिसके प्रकाश यही भीतरी अहिंसा समग्र अन्त:चारित्र और बहि: चारित्र में मानवता मुसकुराती है और सर्वात्मसमता का उदय होता है। की नीव है। लौकिक अहिंसा का बीज भी यही है। इसलिए अहिंसा
इस आत्मसमानाधिकार का ज्ञान और उसको जीवन में उतारने को ही चारित्र का आधार कहा जाता है।
की दृढनिष्ठा ही सर्वोदय की भूमिका हो सकती है। अतः वैयक्तिक अहिंसा की साधना का मुख्य आधार जीव तत्त्व के स्वरुप दुःख की निवृत्ति तथा जगत् में शान्ति स्थापित करने के लिए जिन और उसके समान अधिकार की मर्यादा का तत्त्वज्ञान ही बन सकता व्यक्तियों से यह जगत् बना है उन व्यक्तियों के स्वरुप और अधिकार है। जब हम यह जानते और मानते हैं कि जगत् में वर्तमान सभी की सीमा को हमें समझना ही होगा। हम उसकी तरफ से आँख आत्माएँ अखंड और मूलतः एक-एक स्वतंत्र समान शक्तिवाले द्रव्य मूंदकर तात्कालिक करुणा या दया के आँसू बहा भी लें, पर उसका हैं। जिस प्रकार हमें अपनी हिंसा रुचिकर नहीं है, हम उससे विकल स्थायी समाधान नहीं कर सकते । अतः जैन सिद्धान्त ने बन्धनमुक्ति होते हैं और अपने जीवन को प्रिय समझते हैं; सुख चाहते हैं, दुःख के लिये जो 'बंधा है तथा जिससे बंधा है' (बन्ध और बन्धकृत) से घबडाते हैं उसी तरह अन्य आत्माएँ भी यही चाहती हैं। यही इन दोनों तत्त्वों का परिज्ञान आवश्यक बताया। बिना इसके बन्ध हमारी आत्मा अनादिकाल से सूक्ष्म निगोद, वृक्ष-वनस्पति, क्रीडा- परम्परा के समूलोच्छेद करने का सङ्कल्प ही नहीं हो सकता और मकोडा, पशु-पक्षी आदि अनेक शरीरों को धारण करती रही है और न चारित्र के प्रति उत्साह ही हो सकता है। चारित्र की प्रेरणा तो न जाने इसे कौन-कौन शरीर धारण करना पडेंगे। मनुष्यों में जिन्हें विचारों से ही मिलती है। हम नीच, अछूत आदि कहकर दुरदुराते हैं और अपनी स्वार्थपूर्ण सामाजिक, उपसंहार :राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं और बन्धनों से उन समानाधिकारी
सुख का उपाय अर्थात् दुःख से अत्यन्तनिवृत्ति का मार्ग मनुष्यों के अधिकारों का दलन करके उनके विकास को रोकते हैं,
सम्यग्दर्शन-ज्ञान से युक्त सम्यक्चारित्र है। और पूरे सम्यक्चारित्र उन नीच और अछूतों में भी हम उत्पन्न हुए होंगे। आज मन में दूसरों
का सार भावात्मक अहिंसा अर्थात् रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति के प्रति उन्हीं कुत्सित भावों को जाग्रत करके उस परिस्थिति का
न होना है। वस्तुतः यह कथन भी एकांगी है; इसमें केवल निर्माण अवश्य ही कर रहे हैं जिससे हमारी उन्हीं जातियों में उत्पन्न
नकारात्मक पक्ष का कथन किया गया है। रागादि की उत्पत्ति न होने की अधिक संभावना है। उन सूक्ष्म निगोद से लेकर मनुष्यों होने पर क्या होता है और कैसे होता है, यह महत्त्वपूर्ण है। वस्तुतः तक के हमारे सीधे संपर्क में आनेवाले प्राणियों के मूलभूत स्वरुप रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति के अभाव में जीव की पूर्ण
और अधिकार को समजे बिना हम उन पर करुणा, दया आदि के स्वभावोन्मुखता हो जाती है, और पूर्ण स्वानुभव की प्रक्रिया आरम्भ भाव ही नहीं ला सकते, और न समानाधिकारमूलक परम अहिंसा
हो जाती है। एक बार इस प्रकार के पूर्ण स्वानुभव की प्रक्रिया के भाव ही जागृत कर सकते हैं। चित में जब उन समस्त प्राणियों हो जाने के बाद परोन्मुखता का कोई कारण न होने से जीव सदा में आत्मौपम्य की पुण्यभावना लहर मारती है तभी हमारा प्रत्येक
ही उसी अवस्था में बना रहता है। उच्छ्वास उनकी मंगल कामना से भरा हुआ निकलता है और इस
यहाँ जितने सरल और अल्प शब्दों में और अल्प समय पवित्र धर्म को नहीं समजनेवाले संघर्षशील हिंसकों के शोषण और
में यह कह दिया गया है वह सब इतनी सरलता से नहीं जाता, दलन से पिसती हुई आत्मा के उद्धार की छटपटाहट उत्पन्न हो सकती कारण कि जीव अनादि वासना से दूषित है, और उसके ये संस्कार है। इस तत्त्वज्ञान की सुवास से ही हमारी परिणति परपदार्थों के संग्रह
शीध्र नहीं छूटते, जैसे तम्बाकू, गाँजा, भाँग, मदिरा आदि का नशा और परिग्रह की दुष्प्रवृत्ति से हटकर लोककल्याण और जीव सेवा
शीध्र नहीं छूटता किन्तु धीरे धीरे और दृढ मन से और बहुत कम की ओर झुकती है। अतः अहिंसा की सर्वभूतमैत्री उत्कृष्ट साधना लोगों का ही छूटता है। अविद्या के इस संस्कार को छोड़ने से आत्मा के लिए सर्वभूतों के स्वरुप और अधिकार का ज्ञान तो पहले चाहिये के विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। आत्मा का विकास ही। न केवल ज्ञान ही, अपितु चाहिये उसके प्रति दृढ निष्ठा।। किस प्रक्रिया से होता है, कितने चरणों में होता है, उसे जैनागम इसी सर्वात्मसमत्व की मूलज्योति महावीर बननेवाले
में 'गुणस्थान' शब्द से कहा गया है। गुणस्थान का स्वरुप समझने क्षत्रिय राजकुमार वर्धमान के मन में जगी थी और तभी वे प्राप्त
के लिए आगे 'गुणस्थान' नाम से एक शीर्षक आरम्भ किया जा राजविभूति को बंधन मानकर बाहर-भीतर की गांठे खोलकर रहा है। परमनिर्ग्रन्थ बने और जगत् में मानवता को वर्ण भेद की चक्की में पीसने वाले तथोक्त उच्चाभिमानियों को झकझोरकर एक बार स्ककर सोचने का शीतल वातावरण उपस्थित कर सके । उनने अपने त्याग और तपस्या के साधक जीवन से महत्ता का मापदण्ड ही बदल दिया और उन समस्त त्रस्त, शोषित, अभिद्रावित और
41. पुरुषार्थसिद्धयुपाय
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org