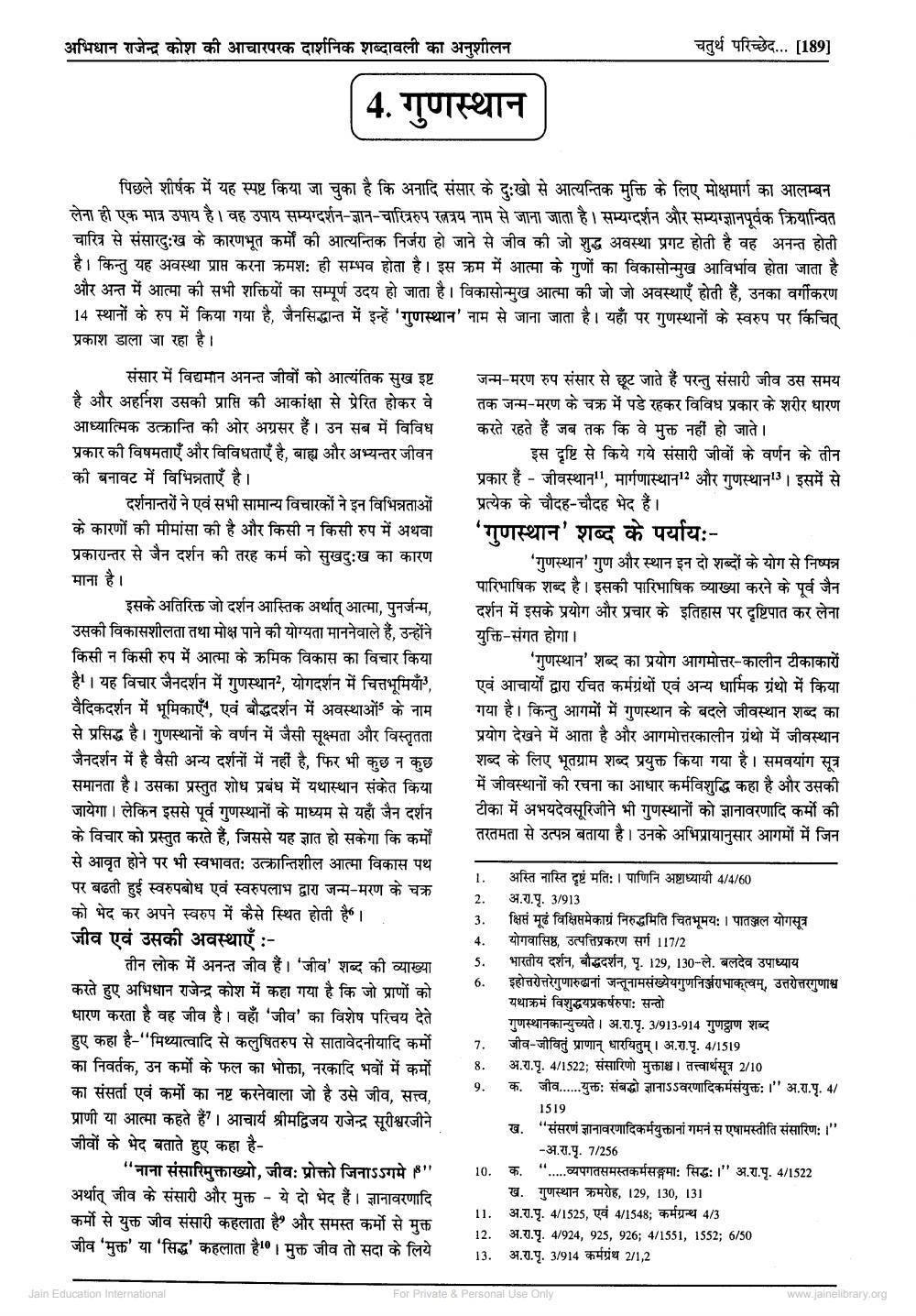________________
अभिधान राजेन्द्र कोश की आचारपरक दार्शनिक शब्दावली का अनुशीलन
चतुर्थ परिच्छेद... [189]
| 4. गुणस्थान |
पिछले शीर्षक में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अनादि संसार के दुःखो से आत्यन्तिक मुक्ति के लिए मोक्षमार्ग का आलम्बन लेना ही एक मात्र उपाय है। वह उपाय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररुप रत्नत्रय नाम से जाना जाता है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानपूर्वक क्रियान्वित चारित्र से संसारदुःख के कारणभूत कर्मों की आत्यन्तिक निर्जरा हो जाने से जीव की जो शुद्ध अवस्था प्रगट होती है वह अनन्त होती है। किन्तु यह अवस्था प्राप्त करना क्रमशः ही सम्भव होता है। इस क्रम में आत्मा के गुणों का विकासोन्मुख आविर्भाव होता जाता है
और अन्त में आत्मा की सभी शक्तियों का सम्पूर्ण उदय हो जाता है। विकासोन्मुख आत्मा की जो जो अवस्थाएँ होती हैं, उनका वर्गीकरण 14 स्थानों के रुप में किया गया है, जैनसिद्धान्त में इन्हें 'गुणस्थान' नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गुणस्थानों के स्वरुप पर किंचित् प्रकाश डाला जा रहा है।
संसार में विद्यमान अनन्त जीवों को आत्यंतिक सुख इष्ट जन्म-मरण रुप संसार से छूट जाते हैं परन्तु संसारी जीव उस समय है और अहर्निश उसकी प्राप्ति की आकांक्षा से प्रेरित होकर वे तक जन्म-मरण के चक्र में पड़े रहकर विविध प्रकार के शरीर धारण आध्यात्मिक उत्क्रान्ति की ओर अग्रसर हैं। उन सब में विविध करते रहते हैं जब तक कि वे मुक्त नहीं हो जाते। प्रकार की विषमताएँ और विविधताएँ है, बाह्य और अभ्यन्तर जीवन
इस दृष्टि से किये गये संसारी जीवों के वर्णन के तीन की बनावट में विभिन्नताएँ है।
प्रकार हैं - जीवस्थान, मार्गणास्थान और गणस्थान। इसमें से दर्शनान्तरों ने एवं सभी सामान्य विचारकों ने इन विभिन्नताओं प्रत्येक के चौदह-चौदह भेद हैं। के कारणों की मीमांसा की है और किसी न किसी रूप में अथवा 'गुणस्थान' शब्द के पर्यायःप्रकारान्तर से जैन दर्शन की तरह कर्म को सुखदुःख का कारण
'गुणस्थान' गुण और स्थान इन दो शब्दों के योग से निष्पन्न माना है।
पारिभाषिक शब्द है। इसकी पारिभाषिक व्याख्या करने के पूर्व जैन इसके अतिरिक्त जो दर्शन आस्तिक अर्थात् आत्मा, पुनर्जन्म, दर्शन में इसके प्रयोग और प्रचार के इतिहास पर दृष्टिपात कर लेना उसकी विकासशीलता तथा मोक्ष पाने की योग्यता माननेवाले हैं, उन्होंने युक्ति-संगत होगा। किसी न किसी रूप में आत्मा के क्रमिक विकास का विचार किया
'गुणस्थान' शब्द का प्रयोग आगमोत्तर-कालीन टीकाकारों है। यह विचार जैनदर्शन में गुणस्थान, योगदर्शन में चित्तभूमियाँ', एवं आचार्यों द्वारा रचित कर्मग्रंथों एवं अन्य धार्मिक ग्रंथो में किया वैदिकदर्शन में भूमिकाएँ', एवं बौद्धदर्शन में अवस्थाओं के नाम गया है। किन्तु आगमों में गुणस्थान के बदले जीवस्थान शब्द का से प्रसिद्ध है। गुणस्थानों के वर्णन में जैसी सूक्ष्मता और विस्तृतता प्रयोग देखने में आता है और आगमोत्तरकालीन ग्रंथो में जीवस्थान जैनदर्शन में है वैसी अन्य दर्शनों में नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ शब्द के लिए भूतग्राम शब्द प्रयुक्त किया गया है। समवयांग सूत्र समानता है। उसका प्रस्तुत शोध प्रबंध में यथास्थान संकेत किया में जीवस्थानों की रचना का आधार कर्मविशुद्धि कहा है और उसकी जायेगा। लेकिन इससे पूर्व गुणस्थानों के माध्यम से यहाँ जैन दर्शन टीका में अभयदेवसूरिजीने भी गुणस्थानों को ज्ञानावरणादि कर्मो की के विचार को प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह ज्ञात हो सकेगा कि कर्मों
तरतमता से उत्पन्न बताया है। उनके अभिप्रायानुसार आगमों में जिन से आवृत होने पर भी स्वभावतः उत्क्रान्तिशील आत्मा विकास पथ
1. अस्ति नास्ति दृष्टं मतिः । पाणिनि अष्टाध्यायी 4/4/60 पर बढती हुई स्वरुपबोध एवं स्वरुपलाभ द्वारा जन्म-मरण के चक्र
2. अ.रा.पृ. 3/913 को भेद कर अपने स्वरुप में कैसे स्थित होती है। .
3. क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चितभूमयः । पातञ्जल योगसूत्र जीव एवं उसकी अवस्थाएँ :
योगवासिष्ठ, उत्पत्तिप्रकरण सर्ग 117/2 तीन लोक में अनन्त जीव हैं। 'जीव' शब्द की व्याख्या
भारतीय दर्शन, बौद्धदर्शन, पृ. 129, 130-ले. बलदेव उपाध्याय करते हुए अभिधान राजेन्द्र कोश में कहा गया है कि जो प्राणों को
इहोत्तरोत्तरेगुणारुढानां जन्तूनामसंख्येयगुणनि राभाक्त्वम्, उत्तरोत्तरगुणाश्व
यथाक्रमं विशुद्धयप्रकर्षरुपाः सन्तो धारण करता है वह जीव है। वहाँ 'जीव' का विशेष परिचय देते
गुणस्थानकान्युच्यते । अ.रा.पृ. 3/913-914 गुणट्ठाण शब्द हुए कहा है-"मिथ्यात्वादि से कलुषितरुप से सातावेदनीयादि कर्मों 7. जीव-जीवितुं प्राणान् धारयितुम् । अ.रा.पृ. 4/1519 का निवर्तक, उन कर्मो के फल का भोक्ता, नरकादि भवों में कर्मो 8. अ.रा.पृ. 4/1522; संसारिणो मुक्ताश्च । तत्त्वार्थसूत्र 2/10 का संसर्ता एवं कर्मों का नष्ट करनेवाला जो है उसे जीव, सत्त्व,
9. क. जीव......युक्तः संबद्धो ज्ञानाऽऽवरणादिकर्मसंयुक्तः।" अ.रा.पृ. 4/
1519 प्राणी या आत्मा कहते हैं। आचार्य श्रीमद्विजय राजेन्द्र सूरीश्वरजीने
ख. "संसरणं ज्ञानावरणादिकर्मयुक्तानां गमनं स एषामस्तीति संसारिणः।" जीवों के भेद बताते हुए कहा है
-अ.रा.पृ. 7/256 "नाना संसारिमुक्ताख्यो, जीवः प्रोक्तो जिनाऽऽगमे" क. ".....व्यपगतसमस्तकर्मसङ्गमाः सिद्धः।" अ.रा.पृ. 4/1522 अर्थात् जीव के संसारी और मुक्त - ये दो भेद हैं। ज्ञानावरणादि
ख. गुणस्थान क्रमरोह, 129, 130, 131
11. अ.रा.पृ. 4/1525, एवं 4/1548; कर्मग्रन्थ 4/3 कर्मो से युक्त जीव संसारी कहलाता है और समस्त कर्मो से मुक्त
12. अ.रा.पृ. 4/924, 925, 926; 4/1551, 1552; 6/50 जीव 'मुक्त' या 'सिद्ध' कहलाता है। 1 मुक्त जीव तो सदा के लिये
13. अ.रा.पृ. 3/914 कर्मग्रंथ 2/1,2
Jain Education International
For Private & Personal use only
www.jainelibrary.org