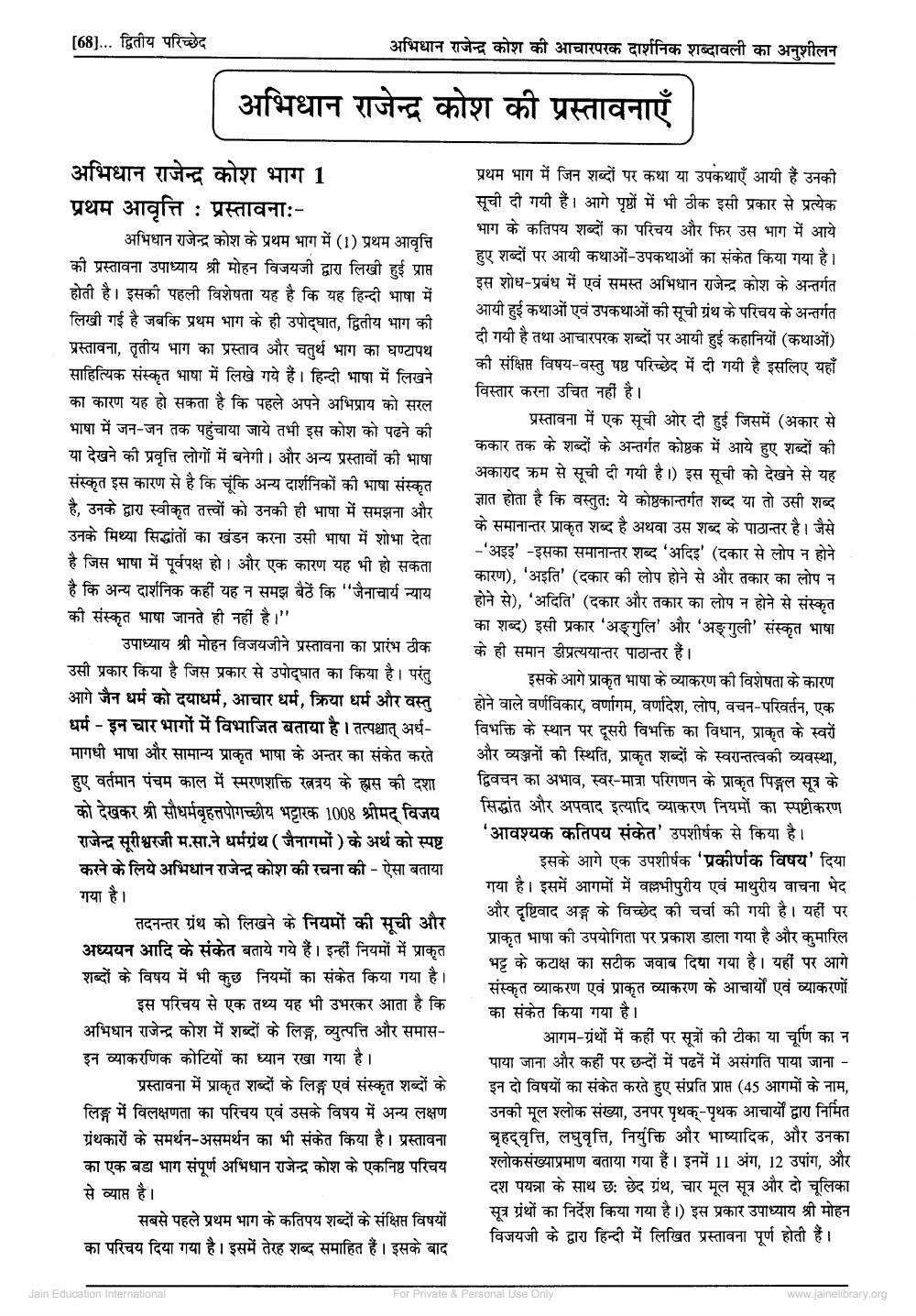________________
[68]... द्वितीय परिच्छेद
अभिधान राजेन्द्र कोश की आचारपरक दार्शनिक शब्दावली का अनुशीलन
अभिधान राजेन्द्र कोश की प्रस्तावनाएँ
अभिधान राजेन्द्र कोश भाग 1 प्रथम आवृत्ति : प्रस्तावनाः
अभिधान राजेन्द्र कोश के प्रथम भाग में (1) प्रथम आवृत्ति की प्रस्तावना उपाध्याय श्री मोहन विजयजी द्वारा लिखी हुई प्राप्त होती है। इसकी पहली विशेषता यह है कि यह हिन्दी भाषा में लिखी गई है जबकि प्रथम भाग के ही उपोद्घात, द्वितीय भाग की प्रस्तावना, तृतीय भाग का प्रस्ताव और चतुर्थ भाग का घण्टापथ साहित्यिक संस्कृत भाषा में लिखे गये हैं। हिन्दी भाषा में लिखने का कारण यह हो सकता है कि पहले अपने अभिप्राय को सरल भाषा में जन-जन तक पहुंचाया जाये तभी इस कोश को पढने की या देखने की प्रवृत्ति लोगों में बनेगी। और अन्य प्रस्तावों की भाषा संस्कृत इस कारण से है कि चूंकि अन्य दार्शनिकों की भाषा संस्कृत है, उनके द्वारा स्वीकृत तत्त्वों को उनकी ही भाषा में समझना और उनके मिथ्या सिद्धांतों का खंडन करना उसी भाषा में शोभा देता है जिस भाषा में पूर्वपक्ष हो। और एक कारण यह भी हो सकता है कि अन्य दार्शनिक कहीं यह न समझ बैठें कि "जैनाचार्य न्याय की संस्कृत भाषा जानते ही नहीं है।"
उपाध्याय श्री मोहन विजयजीने प्रस्तावना का प्रारंभ ठीक उसी प्रकार किया है जिस प्रकार से उपोद्घात का किया है। परंतु आगे जैन धर्म को दयाधर्म, आचार धर्म, क्रिया धर्म और वस्तु धर्म - इन चार भागों में विभाजित बताया है। तत्पश्चात् अर्धमागधी भाषा और सामान्य प्राकृत भाषा के अन्तर का संकेत करते हुए वर्तमान पंचम काल में स्मरणशक्ति रत्नत्रय के ह्रास की दशा को देखकर श्री सौधर्म बृहत्तपोगच्छीय भट्टारक 1008 श्रीमद् विजय राजेन्द्र सूरीश्वरजी म.सा. ने धर्मग्रंथ (जैनागमों) के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये अभिधान राजेन्द्र कोश की रचना की ऐसा बताया गया है ।
तदनन्तर ग्रंथ को लिखने के नियमों की सूची और अध्ययन आदि के संकेत बताये गये हैं। इन्हीं नियमों में प्राकृत शब्दों के विषय में भी कुछ नियमों का संकेत किया गया है।
इस परिचय से एक तथ्य यह भी उभरकर आता है कि अभिधान राजेन्द्र कोश में शब्दों के लिङ्ग, व्युत्पत्ति और समासइन व्याकरणिक कोटियों का ध्यान रखा गया है।
प्रस्तावना में प्राकृत शब्दों के लिङ्ग एवं संस्कृत शब्दों के लिङ्ग में विलक्षणता का परिचय एवं उसके विषय में अन्य लक्षण ग्रंथकारों के समर्थन - असमर्थन का भी संकेत किया है। प्रस्तावना का एक बडा भाग संपूर्ण अभिधान राजेन्द्र कोश के एकनिष्ठ परिचय से व्याप्त है।
Jain Education International
सबसे पहले प्रथम भाग के कतिपय शब्दों के संक्षिप्त विषयों का परिचय दिया गया है। इसमें तेरह शब्द समाहित हैं। इसके बाद
प्रथम भाग में जिन शब्दों पर कथा या उपकथाएँ आयी हैं उनकी सूची दी गयी हैं। आगे पृष्ठों में भी ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक भाग के कतिपय शब्दों का परिचय और फिर उस भाग में आये हुए शब्दों पर आयी कथाओं-उपकथाओं का संकेत किया गया है। इस शोध-प्रबंध में एवं समस्त अभिधान राजेन्द्र कोश के अन्तर्गत आयी हुई कथाओं एवं उपकथाओं की सूची ग्रंथ के परिचय के अन्तर्गत दी गयी है तथा आचारपरक शब्दों पर आयी हुई कहानियों (कथाओं) की संक्षिप्त विषय-वस्तु षष्ठ परिच्छेद में दी गयी है इसलिए यहाँ विस्तार करना उचित नहीं है।
प्रस्तावना में एक सूची ओर दी हुई जिसमें (अकार से ककार तक के शब्दों के अन्तर्गत कोष्ठक में आये हुए शब्दों की अकाराद क्रम से सूची दी गयी है ।) इस सूची को देखने से यह ज्ञात होता है कि वस्तुतः ये कोष्ठकान्तर्गत शब्द या तो उसी शब्द के समानान्तर प्राकृत शब्द है अथवा उस शब्द के पाठान्तर है। जैसे -'अइइ' इसका समानान्तर शब्द 'अदिइ' (दकार से लोप न होने कारण), 'अइति' (दकार की लोप होने से और तकार का लोप न होने से ), 'अदिति' (दकार और तकार का लोप न होने से संस्कृत का शब्द) इसी प्रकार 'अङ्गुलि' और 'अङ्गुली' संस्कृत भाषा के ही समान डीप्रत्ययान्तर पाठान्तर हैं।
इसके आगे प्राकृत भाषा के व्याकरण की विशेषता के कारण होने वाले वर्णविकार, वर्णागम, वर्णादेश, लोप, वचन - परिवर्तन, एक विभक्ति के स्थान पर दूसरी विभक्ति का विधान, प्राकृत के स्वरों और व्यञ्जनों की स्थिति, प्राकृत शब्दों के स्वरान्तत्वकी व्यवस्था, द्विवचन का अभाव, स्वर- मात्रा परिगणन के प्राकृत पिङ्गल सूत्र के सिद्धांत और अपवाद इत्यादि व्याकरण नियमों का स्पष्टीकरण 'आवश्यक कतिपय संकेत' उपशीर्षक से किया है।
इसके आगे एक उपशीर्षक 'प्रकीर्णक विषय' दिया गया है। इसमें आगमों में वल्लभीपुरीय एवं माधुरीय वाचना भेद और दृष्टिवाद अङ्ग के विच्छेद की चर्चा की गयी है । यहीं पर प्राकृत भाषा की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है और कुमारिल भट्ट के कटाक्ष का सटीक जवाब दिया गया है। यहीं पर आगे संस्कृत व्याकरण एवं प्राकृत व्याकरण के आचार्यों एवं व्याकरणों का संकेत किया गया है।
आगम-ग्रंथों में कहीं पर सूत्रों की टीका या चूर्णि का न पाया जाना और कहीं पर छन्दों में पढनें में असंगति पाया जाना - इन दो विषयों का संकेत करते हुए संप्रति प्राप्त (45 आगमों के नाम, उनकी मूल श्लोक संख्या, उनपर पृथक-पृथक आचार्यों द्वारा निर्मित बृहद्वृत्ति, लघुवृत्ति, निर्युक्ति और भाष्यादिक, और उनका श्लोकसंख्याप्रमाण बताया गया हैं। इनमें 11 अंग, 12 उपांग, और दश पयन्ना के साथ छः छेद ग्रंथ, चार मूल सूत्र और दो चूलिका ग्रंथों का निर्देश किया गया है।) इस प्रकार उपाध्याय श्री मोहन सूत्र विजयजी के द्वारा हिन्दी में लिखित प्रस्तावना पूर्ण होती हैं।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org