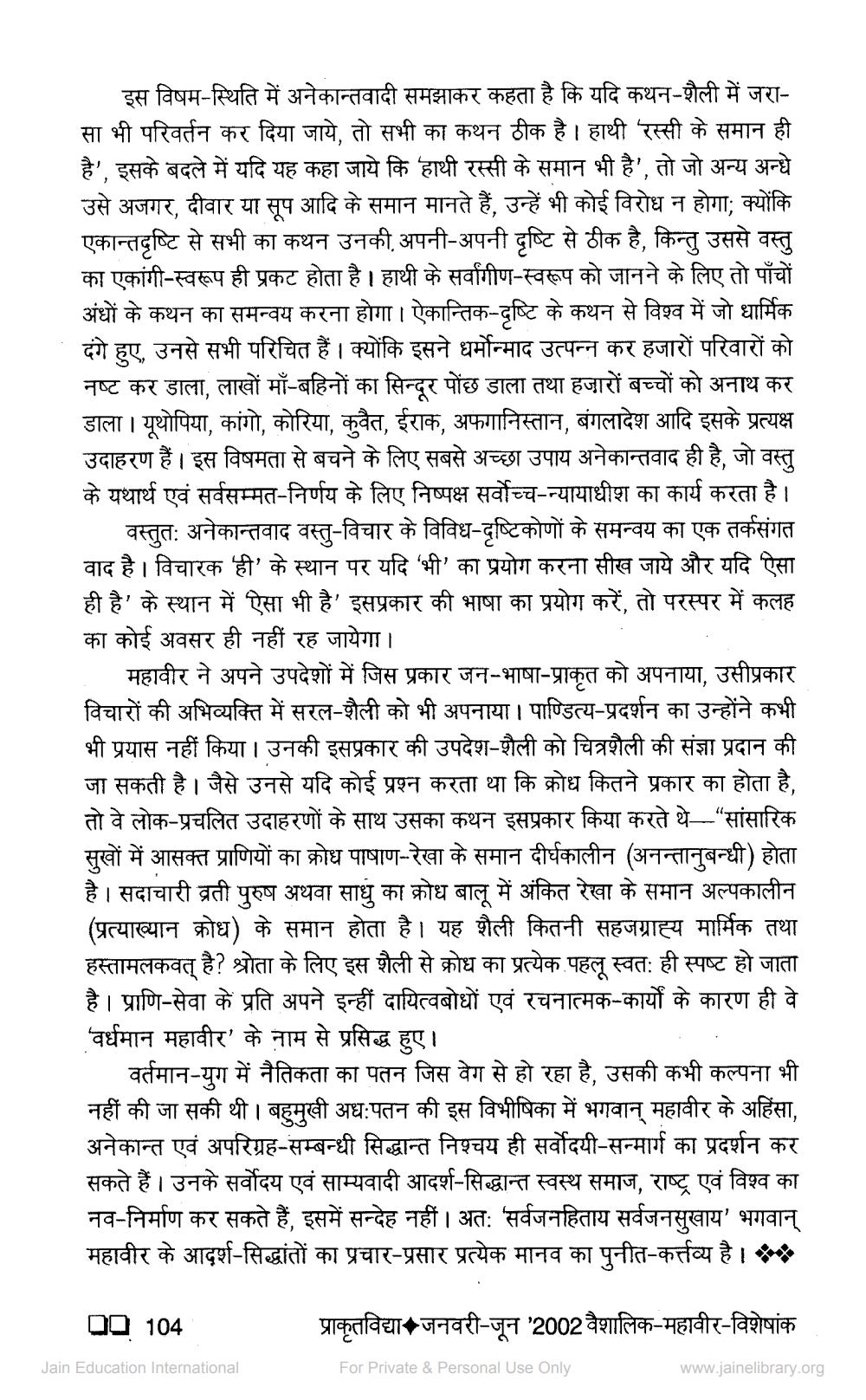________________
इस विषम-स्थिति में अनेकान्तवादी समझाकर कहता है कि यदि कथन-शैली में जरासा भी परिवर्तन कर दिया जाये, तो सभी का कथन ठीक है। हाथी 'रस्सी के समान ही है', इसके बदले में यदि यह कहा जाये कि हाथी रस्सी के समान भी है', तो जो अन्य अन्धे उसे अजगर, दीवार या सूप आदि के समान मानते हैं, उन्हें भी कोई विरोध न होगा; क्योंकि एकान्तदृष्टि से सभी का कथन उनकी अपनी-अपनी दृष्टि से ठीक है, किन्तु उससे वस्तु का एकांगी-स्वरूप ही प्रकट होता है। हाथी के सर्वांगीण-स्वरूप को जानने के लिए तो पाँचों अंधों के कथन का समन्वय करना होगा। ऐकान्तिक-दृष्टि के कथन से विश्व में जो धार्मिक दंगे हुए, उनसे सभी परिचित हैं। क्योंकि इसने धर्मोन्माद उत्पन्न कर हजारों परिवारों को नष्ट कर डाला, लाखों माँ-बहिनों का सिन्दूर पोंछ डाला तथा हजारों बच्चों को अनाथ कर डाला। यूथोपिया, कांगो, कोरिया, कुवैत, ईराक, अफगानिस्तान, बंगलादेश आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इस विषमता से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय अनेकान्तवाद ही है, जो वस्तु के यथार्थ एवं सर्वसम्मत-निर्णय के लिए निष्पक्ष सर्वोच्च-न्यायाधीश का कार्य करता है। ___ वस्तुत: अनेकान्तवाद वस्तु-विचार के विविध-दृष्टिकोणों के समन्वय का एक तर्कसंगत वाद है। विचारक 'ही' के स्थान पर यदि 'भी' का प्रयोग करना सीख जाये और यदि एसा ही है' के स्थान में एसा भी है' इसप्रकार की भाषा का प्रयोग करें, तो परस्पर में कलह का कोई अवसर ही नहीं रह जायेगा।
महावीर ने अपने उपदेशों में जिस प्रकार जन-भाषा-प्राकृत को अपनाया, उसीप्रकार विचारों की अभिव्यक्ति में सरल-शैली को भी अपनाया। पाण्डित्य-प्रदर्शन का उन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया। उनकी इसप्रकार की उपदेश-शैली को चित्रशैली की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। जैसे उनसे यदि कोई प्रश्न करता था कि क्रोध कितने प्रकार का होता है, तो वे लोक-प्रचलित उदाहरणों के साथ उसका कथन इसप्रकार किया करते थे—“सांसारिक सुखों में आसक्त प्राणियों का क्रोध पाषाण-रेखा के समान दीर्घकालीन (अनन्तानुबन्धी) होता है। सदाचारी व्रती पुरुष अथवा साधु का क्रोध बालू में अंकित रेखा के समान अल्पकालीन (प्रत्याख्यान क्रोध) के समान होता है। यह शैली कितनी सहजग्राह्य मार्मिक तथा हस्तामलकवत् है? श्रोता के लिए इस शैली से क्रोध का प्रत्येक पहलू स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है। प्राणि-सेवा के प्रति अपने इन्हीं दायित्वबोधों एवं रचनात्मक-कार्यों के कारण ही वे ‘वर्धमान महावीर' के नाम से प्रसिद्ध हुए। ___वर्तमान-युग में नैतिकता का पतन जिस वेग से हो रहा है, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकी थी। बहुमुखी अध:पतन की इस विभीषिका में भगवान् महावीर के अहिंसा, अनेकान्त एवं अपरिग्रह-सम्बन्धी सिद्धान्त निश्चय ही सर्वोदयी-सन्मार्ग का प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके सर्वोदय एवं साम्यवादी आदर्श-सिद्धान्त स्वस्थ समाज, राष्ट्र एवं विश्व का नव-निर्माण कर सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं। अत: 'सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय' भगवान् महावीर के आदर्श-सिद्धांतों का प्रचार-प्रसार प्रत्येक मानव का पुनीत-कर्तव्य है।
00 104
प्राकृतविद्या जनवरी-जून '2002 वैशालिक-महावीर-विशेषांक For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org
Jain Education International