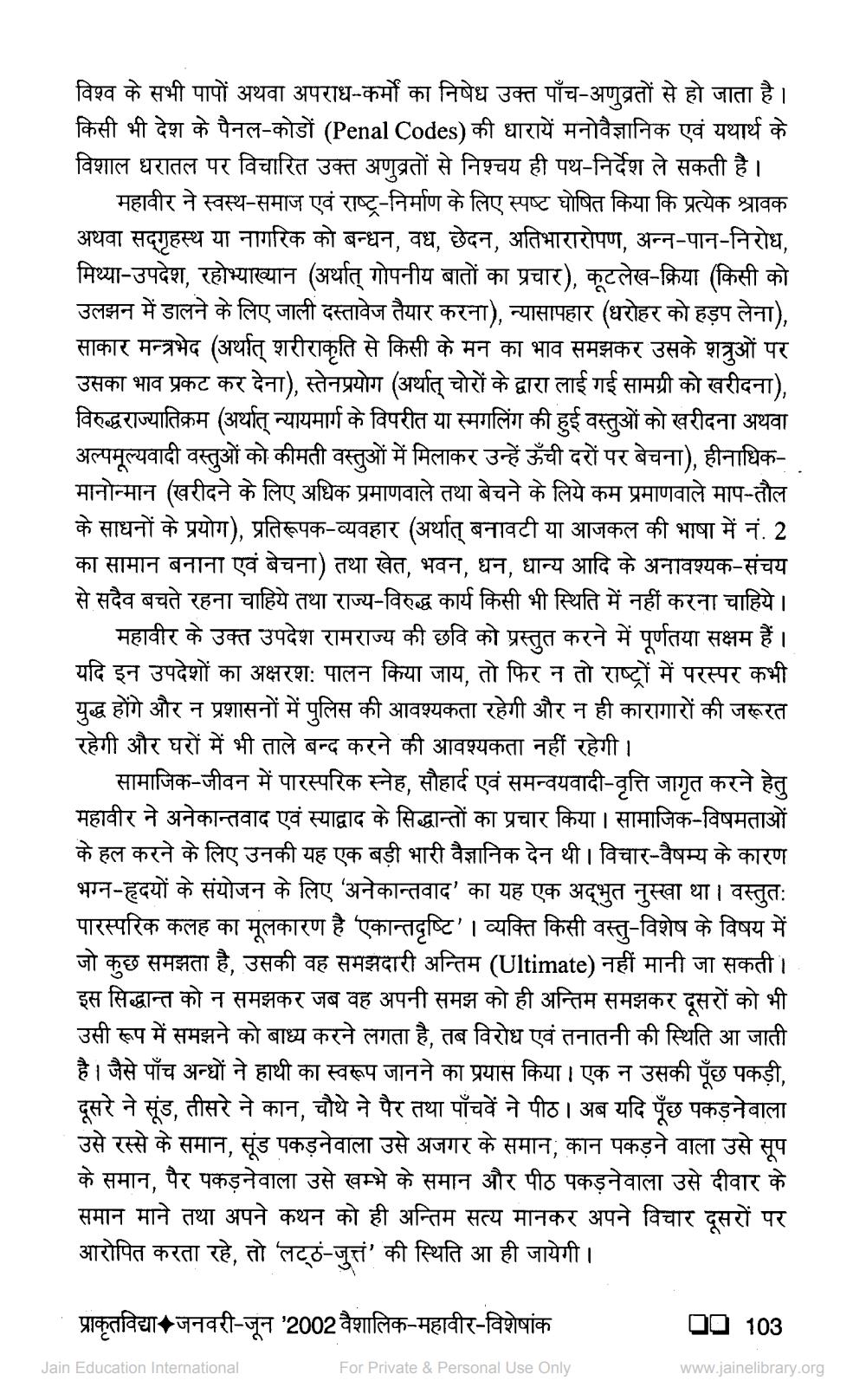________________
विश्व के सभी पापों अथवा अपराध-कर्मों का निषेध उक्त पाँच-अणुव्रतों से हो जाता है। किसी भी देश के पैनल-कोडों (Penal Codes) की धारायें मनोवैज्ञानिक एवं यथार्थ के विशाल धरातल पर विचारित उक्त अणुव्रतों से निश्चय ही पथ-निर्देश ले सकती है। ___महावीर ने स्वस्थ-समाज एवं राष्ट्र-निर्माण के लिए स्पष्ट घोषित किया कि प्रत्येक श्रावक अथवा सद्गृहस्थ या नागरिक को बन्धन, वध, छेदन, अतिभारारोपण, अन्न-पान-निरोध, मिथ्या-उपदेश, रहोभ्याख्यान (अर्थात् गोपनीय बातों का प्रचार), कूटलेख-क्रिया (किसी को उलझन में डालने के लिए जाली दस्तावेज तैयार करना), न्यासापहार (धरोहर को हड़प लेना), साकार मन्त्रभेद (अर्थात् शरीराकृति से किसी के मन का भाव समझकर उसके शत्रुओं पर उसका भाव प्रकट कर देना), स्तेनप्रयोग (अर्थात् चोरों के द्वारा लाई गई सामग्री को खरीदना), विरुद्धराज्यातिक्रम (अर्थात् न्यायमार्ग के विपरीत या स्मगलिंग की हुई वस्तुओं को खरीदना अथवा अल्पमूल्यवादी वस्तुओं को कीमती वस्तुओं में मिलाकर उन्हें ऊँची दरों पर बेचना), हीनाधिकमानोन्मान (खरीदने के लिए अधिक प्रमाणवाले तथा बेचने के लिये कम प्रमाणवाले माप-तौल के साधनों के प्रयोग), प्रतिरूपक-व्यवहार (अर्थात् बनावटी या आजकल की भाषा में नं. 2 का सामान बनाना एवं बेचना) तथा खेत, भवन, धन, धान्य आदि के अनावश्यक-संचय से सदैव बचते रहना चाहिये तथा राज्य-विरुद्ध कार्य किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिये।
महावीर के उक्त उपदेश रामराज्य की छवि को प्रस्तुत करने में पूर्णतया सक्षम हैं। यदि इन उपदेशों का अक्षरश: पालन किया जाय, तो फिर न तो राष्ट्रों में परस्पर कभी युद्ध होंगे और न प्रशासनों में पुलिस की आवश्यकता रहेगी और न ही कारागारों की जरूरत रहेगी और घरों में भी ताले बन्द करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
सामाजिक-जीवन में पारस्परिक स्नेह, सौहार्द एवं समन्वयवादी-वृत्ति जागृत करने हेतु महावीर ने अनेकान्तवाद एवं स्याद्वाद के सिद्धान्तों का प्रचार किया। सामाजिक-विषमताओं के हल करने के लिए उनकी यह एक बड़ी भारी वैज्ञानिक देन थी। विचार-वैषम्य के कारण भग्न-हृदयों के संयोजन के लिए 'अनेकान्तवाद' का यह एक अद्भुत नुस्खा था। वस्तुत: पारस्परिक कलह का मूलकारण है 'एकान्तदृष्टि' । व्यक्ति किसी वस्तु-विशेष के विषय में जो कुछ समझता है, उसकी वह समझदारी अन्तिम (Ultimate) नहीं मानी जा सकती। इस सिद्धान्त को न समझकर जब वह अपनी समझ को ही अन्तिम समझकर दूसरों को भी उसी रूप में समझने को बाध्य करने लगता है, तब विरोध एवं तनातनी की स्थिति आ जाती है। जैसे पाँच अन्धों ने हाथी का स्वरूप जानने का प्रयास किया। एक न उसकी पूँछ पकड़ी, दूसरे ने सूंड, तीसरे ने कान, चौथे ने पैर तथा पाँचवें ने पीठ। अब यदि पूँछ पकड़नेवाला उसे रस्से के समान, सूंड पकड़नेवाला उसे अजगर के समान, कान पकड़ने वाला उसे सूप के समान, पैर पकड़नेवाला उसे खम्भे के समान और पीठ पकड़नेवाला उसे दीवार के समान माने तथा अपने कथन को ही अन्तिम सत्य मानकर अपने विचार दूसरों पर आरोपित करता रहे, तो लट्ठ-जुत्तं' की स्थिति आ ही जायेगी।
प्राकृतविद्या-जनवरी-जून '2002 वैशालिक-महावीर-विशेषांक
00 103
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org