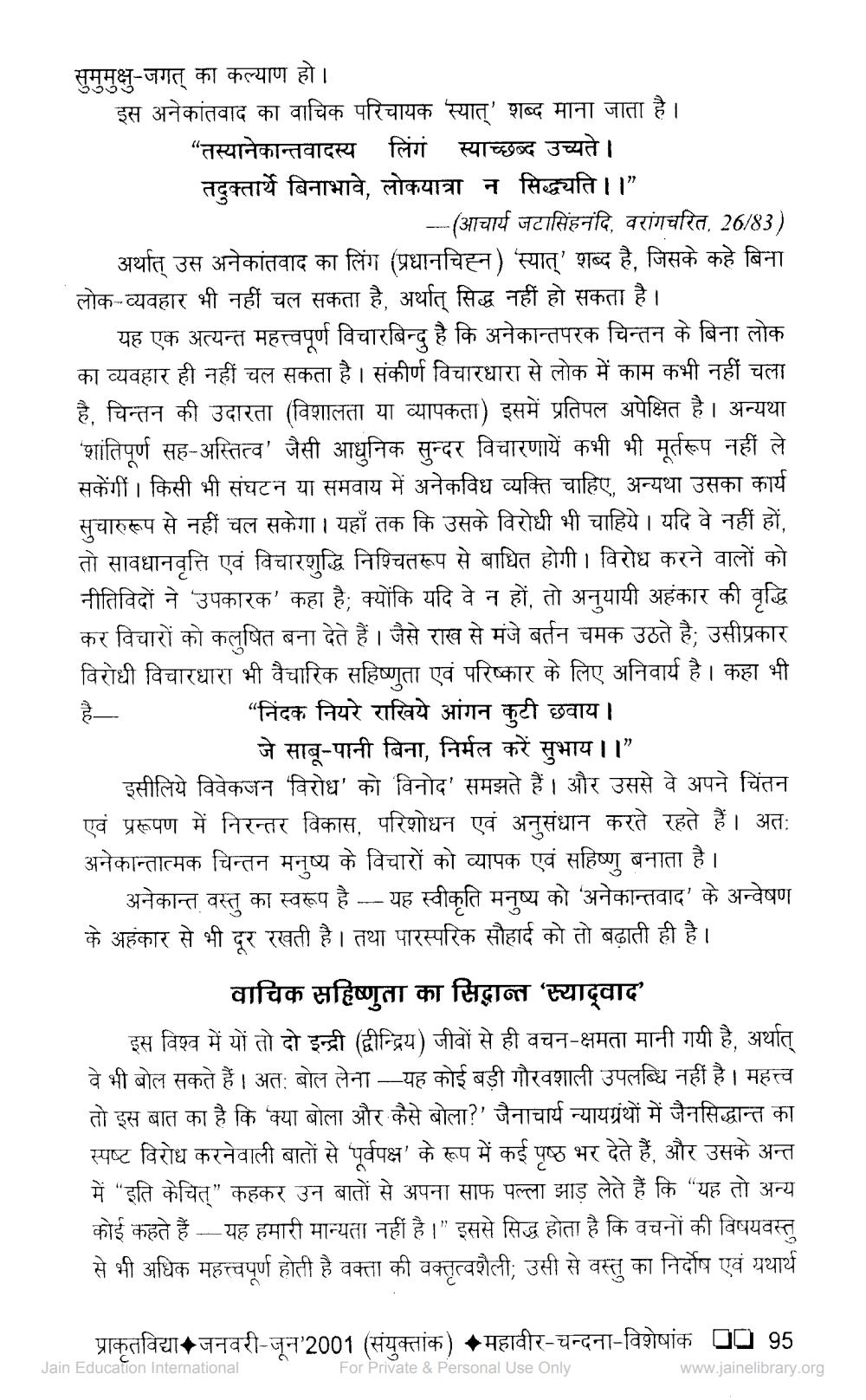________________
सुमुमुक्षु-जगत् का कल्याण हो। इस अनेकांतवाद का वाचिक परिचायक स्यात्' शब्द माना जाता है।
"तस्यानेकान्तवादस्य लिंगं स्याच्छब्द उच्यते। तदुक्तार्थे बिनाभावे, लोकयात्रा न सिद्ध्यति ।।"
--(आचार्य जटासिंहनंदि, वरांगचरित, 26/83) अर्थात् उस अनेकांतवाद का लिंग (प्रधानचिह्न) 'स्यात्' शब्द है, जिसके कहे बिना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता है, अर्थात् सिद्ध नहीं हो सकता है।
यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचारबिन्दु है कि अनेकान्तपरक चिन्तन के बिना लोक का व्यवहार ही नहीं चल सकता है। संकीर्ण विचारधारा से लोक में काम कभी नहीं चला है, चिन्तन की उदारता (विशालता या व्यापकता) इसमें प्रतिपल अपेक्षित है। अन्यथा 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व' जैसी आधुनिक सुन्दर विचारणायें कभी भी मूर्तरूप नहीं ले सकेंगीं। किसी भी संघटन या समवाय में अनेकविध व्यक्ति चाहिए, अन्यथा उसका कार्य सुचारुरूप से नहीं चल सकेगा। यहाँ तक कि उसके विरोधी भी चाहिये। यदि वे नहीं हों, तो सावधानवृत्ति एवं विचारशुद्धि निश्चितरूप से बाधित होगी। विरोध करने वालों को नीतिविदों ने 'उपकारक' कहा है; क्योंकि यदि वे न हों, तो अनुयायी अहंकार की वृद्धि कर विचारों को कलषित बना देते हैं। जैसे राख से मंजे बर्तन चमक उठते है; उसीप्रकार विरोधी विचारधारा भी वैचारिक सहिष्णुता एवं परिष्कार के लिए अनिवार्य है। कहा भी है- “निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय।
जे साबू-पानी बिना, निर्मल करें सुभाय ।।" इसीलिये विवेकजन 'विरोध' को विनोद' समझते हैं। और उससे वे अपने चिंतन एवं प्ररूपण में निरन्तर विकास, परिशोधन एवं अनुसंधान करते रहते हैं। अत: अनेकान्तात्मक चिन्तन मनुष्य के विचारों को व्यापक एवं सहिष्णु बनाता है।
अनेकान्त वस्तु का स्वरूप है ---- यह स्वीकृति मनुष्य को ‘अनेकान्तवाद' के अन्वेषण के अहंकार से भी दूर रखती है। तथा पारस्परिक सौहार्द को तो बढ़ाती ही है।
वाचिक सहिष्णुता का सिद्धान्त 'स्याद्वाद' इस विश्व में यों तो दो इन्द्री (द्वीन्द्रिय) जीवों से ही वचन-क्षमता मानी गयी है, अर्थात् वे भी बोल सकते हैं। अत: बोल लेना —यह कोई बड़ी गौरवशाली उपलब्धि नहीं है। महत्त्व तो इस बात का है कि क्या बोला और कैसे बोला?' जैनाचार्य न्यायग्रंथों में जैनसिद्धान्त का स्पष्ट विरोध करनेवाली बातों से 'पूर्वपक्ष' के रूप में कई पृष्ठ भर देते हैं, और उसके अन्त में “इति केचित्” कहकर उन बातों से अपना साफ पल्ला झाड़ लेते हैं कि “यह तो अन्य कोई कहते हैं .... यह हमारी मान्यता नहीं है।" इससे सिद्ध होता है कि वचनों की विषयवस्तु से भी अधिक महत्त्वपूर्ण होती है वक्ता की वक्तृत्वशैली; उसी से वस्तु का निर्दोष एवं यथार्थ
प्राकृतविद्या जनवरी-जून 2001 (संयुक्तांक) +महावीर-चन्दना-विशेषांक 95 Jain Education International For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org