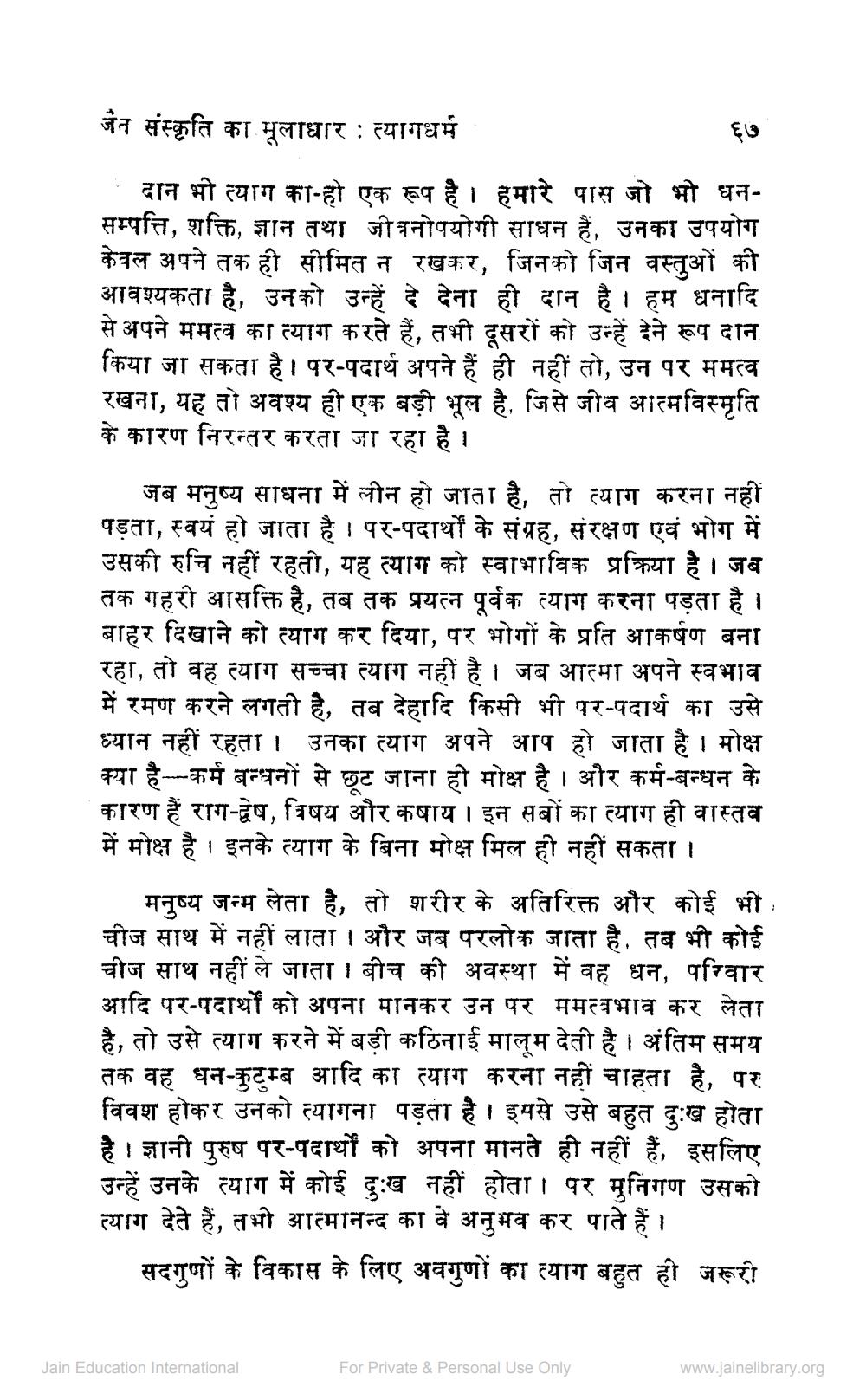________________
जैन संस्कृति का मूलाधार : त्यागधर्म
६७
- दान भी त्याग का-हो एक रूप है। हमारे पास जो भो धनसम्पत्ति, शक्ति, ज्ञान तथा जीवनोपयोगी साधन हैं, उनका उपयोग केवल अपने तक ही सीमित न रखकर, जिनको जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनको उन्हें दे देना ही दान है। हम धनादि से अपने ममत्व का त्याग करते हैं, तभी दूसरों को उन्हें देने रूप दान किया जा सकता है। पर-पदार्थ अपने हैं ही नहीं तो, उन पर ममत्व रखना, यह तो अवश्य ही एक बड़ी भूल है, जिसे जीव आत्मविस्मृति के कारण निरन्तर करता जा रहा है ।
जब मनुष्य साधना में लीन हो जाता है, तो त्याग करना नहीं पड़ता, स्वयं हो जाता है। पर-पदार्थों के संग्रह, संरक्षण एवं भोग में उसकी रुचि नहीं रहती, यह त्याग को स्वाभाविक प्रक्रिया है । जब तक गहरी आसक्ति है, तब तक प्रयत्न पूर्वक त्याग करना पड़ता है। बाहर दिखाने को त्याग कर दिया, पर भोगों के प्रति आकर्षण बना रहा, तो वह त्याग सच्चा त्याग नहीं है। जब आत्मा अपने स्वभाव में रमण करने लगती है, तब देहादि किसी भी पर-पदार्थ का उसे ध्यान नहीं रहता। उनका त्याग अपने आप हो जाता है। मोक्ष क्या है-कर्म बन्धनों से छूट जाना हो मोक्ष है। और कर्म-बन्धन के कारण हैं राग-द्वेष, विषय और कषाय । इन सबों का त्याग ही वास्तव में मोक्ष है । इनके त्याग के बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता।
मनुष्य जन्म लेता है, तो शरीर के अतिरिक्त और कोई भी चीज साथ में नहीं लाता । और जब परलोक जाता है, तब भी कोई चीज साथ नहीं ले जाता । बीच की अवस्था में वह धन, परिवार आदि पर-पदार्थों को अपना मानकर उन पर ममत्वभाव कर लेता है, तो उसे त्याग करने में बड़ी कठिनाई मालूम देती है। अंतिम समय तक वह धन-कूटम्ब आदि का त्याग करना नहीं चाहता है, पर विवश होकर उनको त्यागना पड़ता है। इससे उसे बहुत दुःख होता है । ज्ञानी पुरुष पर-पदार्थों को अपना मानते ही नहीं हैं, इसलिए उन्हें उनके त्याग में कोई दुःख नहीं होता। पर मुनिगण उसको त्याग देते हैं, तभी आत्मानन्द का वे अनुभव कर पाते हैं।
सदगुणों के विकास के लिए अवगुणों का त्याग बहुत ही जरूरी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org