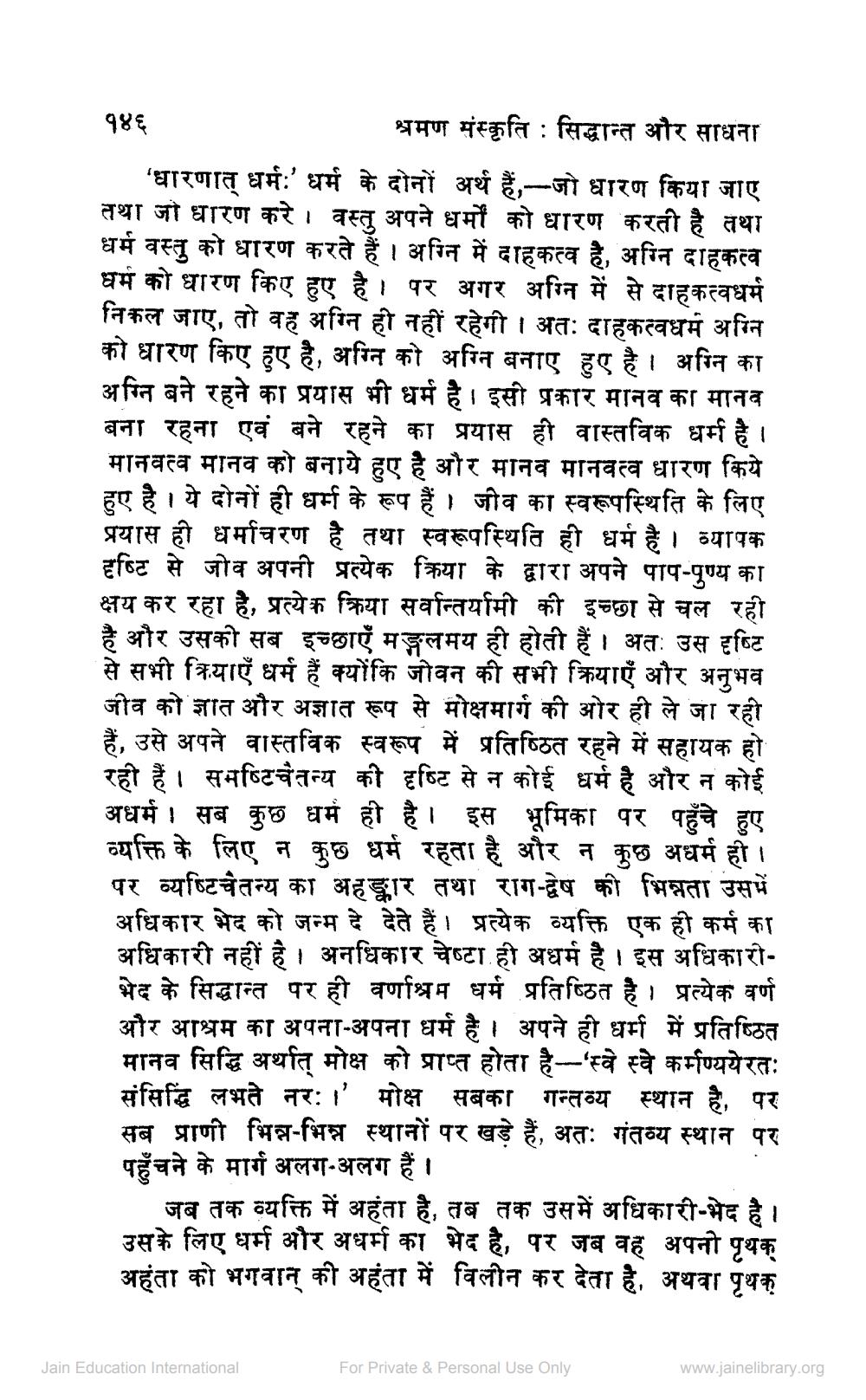________________
श्रमण संस्कृति : सिद्धान्त और साधना
1
'धारणात् धर्मः' धर्म के दोनों अर्थ हैं, जो धारण किया जाए तथा जो धारण करे । वस्तु अपने धर्मों को धारण करती है तथा धर्म वस्तु को धारण करते हैं । अग्नि में दाहकत्व है, अग्नि दाहकत्व धर्म को धारण किए हुए है । पर अगर अग्नि में से दाहकत्वधर्म निकल जाए, तो वह अग्नि ही नहीं रहेगी । अतः दाहकत्वधर्म अग्नि को धारण किए हुए है, अग्नि को अग्नि बनाए हुए है। अग्नि का अग्नि बने रहने का प्रयास भी धर्म है। इसी प्रकार मानव का मानव बना रहना एवं बने रहने का प्रयास ही वास्तविक धर्म है । मानवत्व मानव को बनाये हुए है और मानव मानवत्व धारण किये हुए है । ये दोनों ही धर्म के रूप हैं । जीव का स्वरूपस्थिति के लिए प्रयास ही धर्माचरण है तथा स्वरूपस्थिति ही धर्म है । व्यापक tfse से जोव अपनी प्रत्येक क्रिया के द्वारा अपने पाप-पुण्य का क्षय कर रहा है, प्रत्येक क्रिया सर्वान्तर्यामी की इच्छा से चल रही है और उसकी सब इच्छाएँ मङ्गलमय ही होती हैं । अतः उस दृष्टि से सभी क्रियाएँ धर्म हैं क्योंकि जीवन की सभी क्रियाएँ और अनुभव जीव को ज्ञात और अज्ञात रूप से मोक्षमार्ग की ओर ही ले जा रही हैं, उसे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने में सहायक हो रही हैं । समष्टिचैतन्य की दृष्टि से न कोई धर्म है और न कोई अधर्म । सब कुछ धर्म ही है । इस भूमिका पर पहुँचे हुए व्यक्ति के लिए न कुछ धर्म रहता है और न कुछ अधर्म ही । पर व्यष्टिचैतन्य का अहङ्कार तथा राग-द्वेष की भिन्नता उसमें अधिकार भेद को जन्म दे देते हैं । प्रत्येक व्यक्ति एक ही कर्म का अधिकारी नहीं है । अनधिकार चेष्टा ही अधर्म है । इस अधिकारीभेद के सिद्धान्त पर ही वर्णाश्रम धर्म प्रतिष्ठित है । प्रत्येक वर्ण और आश्रम का अपना-अपना धर्म है । अपने ही धर्म में प्रतिष्ठित मानव सिद्धि अर्थात् मोक्ष को प्राप्त होता है - 'स्वे स्वे कर्मण्यये रतः संसिद्धिं लभते नरः ।' मोक्ष सबका गन्तव्य स्थान है, पर सब प्राणी भिन्न-भिन्न स्थानों पर खड़े हैं, अतः गंतव्य स्थान पर पहुँचने के मार्ग अलग-अलग हैं ।
--
१४६
taar व्यक्ति में अहंता है, तब तक उसमें अधिकारी-भेद है । उसके लिए धर्म और अधर्म का भेद है, पर जब वह अपनी पृथक् अहंता को भगवान् की अहंता में विलीन कर देता है, अथवा पृथक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org