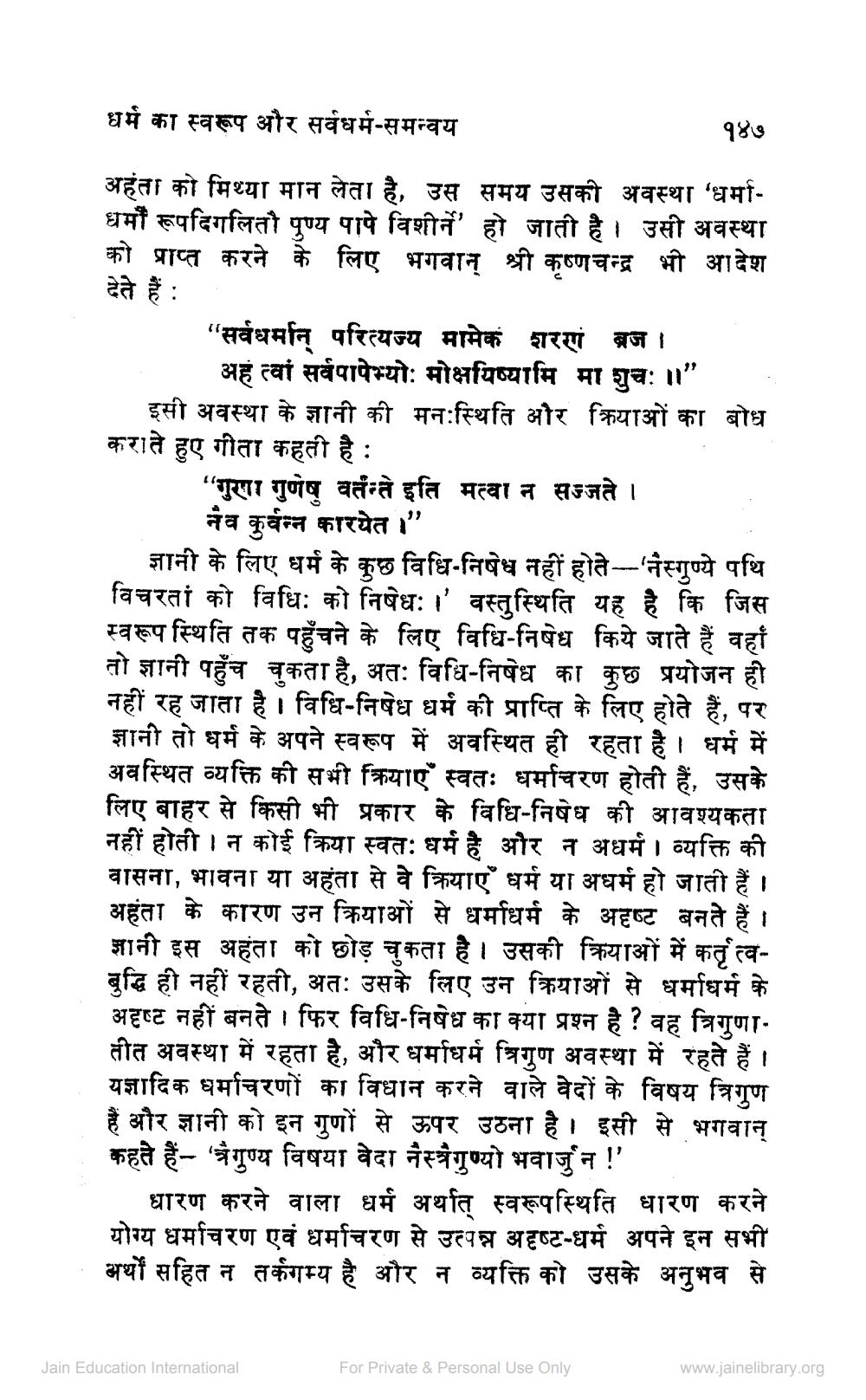________________
धर्म का स्वरूप और सर्वधर्म समन्वय
१४७
अहंता को मिथ्या मान लेता है, उस समय उसकी अवस्था 'धर्मा - धर्मो रूपदिगलितौ पुण्य पापे विशीर्ने' हो जाती है । उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान् श्री कृष्णचन्द्र भी आदेश देते हैं
"सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वां सर्वपापेभ्योः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥" इसी अवस्था के ज्ञानी की मनःस्थिति और क्रियाओं का बोध कराते हुए गीता कहती है :
"गुरणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते । नैव कुर्वन्न कारयेत ।"
ज्ञानी के लिए धर्म के कुछ विधि-निषेध नहीं होते - 'नंस्गुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ।' वस्तुस्थिति यह है कि जिस स्वरूप स्थिति तक पहुँचने के लिए विधि-निषेध किये जाते हैं वहाँ तो ज्ञानी पहुँच चुकता है, अतः विधि-निषेध का कुछ प्रयोजन ही नहीं रह जाता है । विधि-निषेध धर्म की प्राप्ति के लिए होते हैं, पर ज्ञानी तो धर्म के अपने स्वरूप में अवस्थित ही रहता है । धर्म में अवस्थित व्यक्ति की सभी क्रियाएँ स्वतः धर्माचरण होती हैं, उसके लिए बाहर से किसी भी प्रकार के विधि-निषेध की आवश्यकता नहीं होती । न कोई क्रिया स्वतः धर्म है और न अधर्मं । व्यक्ति की वासना, भावना या अहंता से वे क्रियाएँ धर्म या अधर्म हो जाती हैं । अहंता के कारण उन क्रियाओं से धर्माधर्म के अदृष्ट बनते हैं । ज्ञानी इस अहंता को छोड़ चुकता है । उसकी क्रियाओं में कर्तृत्वबुद्धि ही नहीं रहती, अतः उसके लिए उन क्रियाओं से धर्माधर्म के अदृष्ट नहीं बनते । फिर विधि-निषेध का क्या प्रश्न है ? वह त्रिगुणातीत अवस्था में रहता है, और धर्माधर्म त्रिगुण अवस्था में रहते हैं । यज्ञादिक धर्माचरणों का विधान करने वाले वेदों के विषय त्रिगुण हैं और ज्ञानी को इन गुणों से ऊपर उठना है । इसी से भगवान् कहते हैं- 'त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन !'
धारण करने वाला धर्म अर्थात् स्वरूपस्थिति धारण करने योग्य धर्माचरण एवं धर्माचरण से उत्पन्न अदृष्ट-धर्म अपने इन सभी अर्थों सहित न तर्कगम्य है और न व्यक्ति को उसके अनुभव से
Jain Education International
A
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org