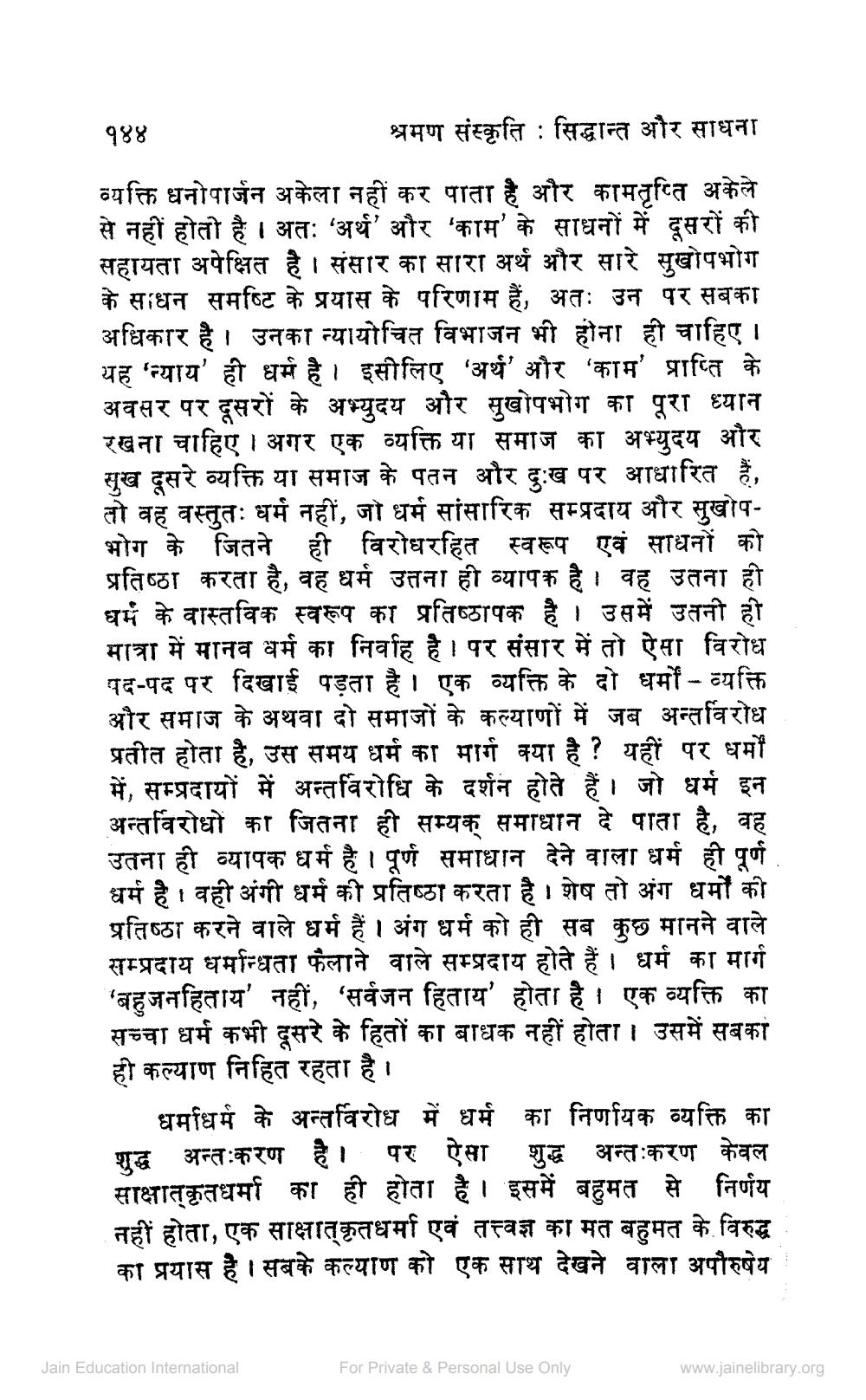________________
१४४
श्रमण संस्कृति : सिद्धान्त और साधना
व्यक्ति धनोपार्जन अकेला नहीं कर पाता है और कामतृप्ति अकेले से नहीं होती है । अत: 'अर्थ' और 'काम' के साधनों में दूसरों की सहायता अपेक्षित है। संसार का सारा अर्थ और सारे सूखोपभोग के साधन समष्टि के प्रयास के परिणाम हैं, अतः उन पर सबका अधिकार है। उनका न्यायोचित विभाजन भी होना ही चाहिए । यह 'न्याय' ही धर्म है। इसीलिए 'अर्थ' और 'काम' प्राप्ति के अवसर पर दूसरों के अभ्युदय और सुखोपभोग का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर एक व्यक्ति या समाज का अभ्युदय और सुख दूसरे व्यक्ति या समाज के पतन और दुःख पर आधारित हैं, तो वह वस्तुतः धर्म नहीं, जो धर्म सांसारिक सम्प्रदाय और सुखोपभोग के जितने ही विरोधरहित स्वरूप एवं साधनों को प्रतिष्ठा करता है, वह धर्म उतना ही व्यापक है। वह उतना ही धर्म के वास्तविक स्वरूप का प्रतिष्ठापक है। उसमें उतनी ही मात्रा में मानव धर्म का निर्वाह है। पर संसार में तो ऐसा विरोध पद-पद पर दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति के दो धर्मों - व्यक्ति और समाज के अथवा दो समाजों के कल्याणों में जब अन्तविरोध प्रतीत होता है, उस समय धर्म का मार्ग क्या है ? यहीं पर धर्मों में, सम्प्रदायों में अन्तविरोधि के दर्शन होते हैं। जो धर्म इन अन्तर्विरोधो का जितना ही सम्यक् समाधान दे पाता है, वह उतना ही व्यापक धर्म है । पूर्ण समाधान देने वाला धर्म ही पूर्ण धर्म है। वही अंगी धर्म की प्रतिष्ठा करता है। शेष तो अंग धमों की प्रतिष्ठा करने वाले धर्म हैं । अंग धर्म को ही सब कुछ मानने वाले सम्प्रदाय धर्मान्धता फैलाने वाले सम्प्रदाय होते हैं। धर्म का मार्ग 'बहुजनहिताय' नहीं, 'सर्वजन हिताय' होता है। एक व्यक्ति का सच्चा धर्म कभी दूसरे के हितों का बाधक नहीं होता। उसमें सबका ही कल्याण निहित रहता है।
धर्माधर्म के अन्तविरोध में धर्म का निर्णायक व्यक्ति का शुद्ध अन्तःकरण है। पर ऐसा शुद्ध अन्तःकरण केवल साक्षात्कृतधर्मा का ही होता है। इसमें बहुमत से निर्णय नहीं होता, एक साक्षात्कृतधर्मा एवं तत्त्वज्ञ का मत बहुमत के विरुद्ध का प्रयास है। सबके कल्याण को एक साथ देखने वाला अपौरुषेय
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org