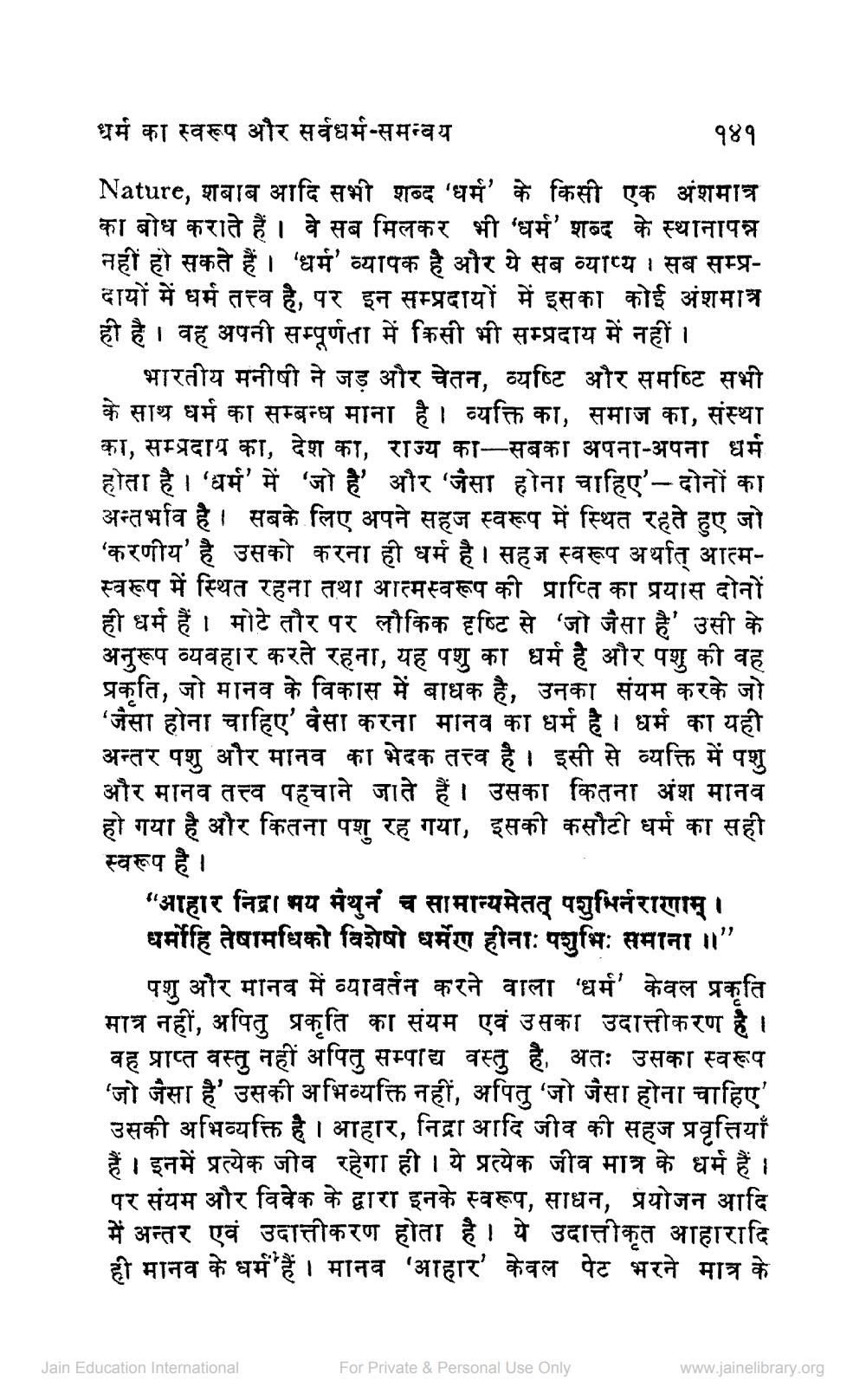________________
धर्म का स्वरूप और सर्वधर्म-समन्वय
१४१
Nature, शबाब आदि सभी शब्द 'धर्म' के किसी एक अंशमात्र का बोध कराते हैं। वे सब मिलकर भी 'धर्म' शब्द के स्थानापन्न नहीं हो सकते हैं। 'धर्म' व्यापक है और ये सब व्याप्य । सब सम्प्रदायों में धर्म तत्त्व है, पर इन सम्प्रदायों में इसका कोई अंशमात्र ही है। वह अपनी सम्पूर्णता में किसी भी सम्प्रदाय में नहीं। __भारतीय मनीषी ने जड़ और चेतन, व्यष्टि और समष्टि सभी के साथ धर्म का सम्बन्ध माना है। व्यक्ति का, समाज का, संस्था का, सम्प्रदाय का, देश का, राज्य का-सबका अपना-अपना धर्म होता है । 'धर्म' में 'जो है' और 'जैसा होना चाहिए'-दोनों का अन्तर्भाव है। सबके लिए अपने सहज स्वरूप में स्थित रहते हुए जो 'करणीय' है उसको करना ही धर्म है। सहज स्वरूप अर्थात् आत्मस्वरूप में स्थित रहना तथा आत्मस्वरूप की प्राप्ति का प्रयास दोनों ही धर्म हैं। मोटे तौर पर लौकिक दृष्टि से 'जो जैसा है' उसी के अनुरूप व्यवहार करते रहना, यह पशु का धर्म है और पशु की वह प्रकृति, जो मानव के विकास में बाधक है, उनका संयम करके जो 'जैसा होना चाहिए' वैसा करना मानव का धर्म है। धर्म का यही अन्तर पशु और मानव का भेदक तत्त्व है। इसी से व्यक्ति में पशु और मानव तत्त्व पहचाने जाते हैं। उसका कितना अंश मानव हो गया है और कितना पशु रह गया, इसको कसौटी धर्म का सही स्वरूप है।
"आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् । धर्मोहि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना ॥"
पशु और मानव में व्यावर्तन करने वाला 'धर्म' केवल प्रकृति मात्र नहीं, अपितु प्रकृति का संयम एवं उसका उदात्तीकरण है। वह प्राप्त वस्तु नहीं अपितु सम्पाद्य वस्तु है, अतः उसका स्वरूप 'जो जैसा है' उसकी अभिव्यक्ति नहीं, अपितु 'जो जैसा होना चाहिए' उसकी अभिव्यक्ति है । आहार, निद्रा आदि जीव की सहज प्रवृत्तियाँ हैं। इनमें प्रत्येक जीव रहेगा ही। ये प्रत्येक जीव मात्र के धर्म हैं। पर संयम और विवेक के द्वारा इनके स्वरूप, साधन, प्रयोजन आदि में अन्तर एवं उदात्तीकरण होता है। ये उदात्तीकत आहारादि ही मानव के धर्म हैं । मानव 'आहार' केवल पेट भरने मात्र के
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org