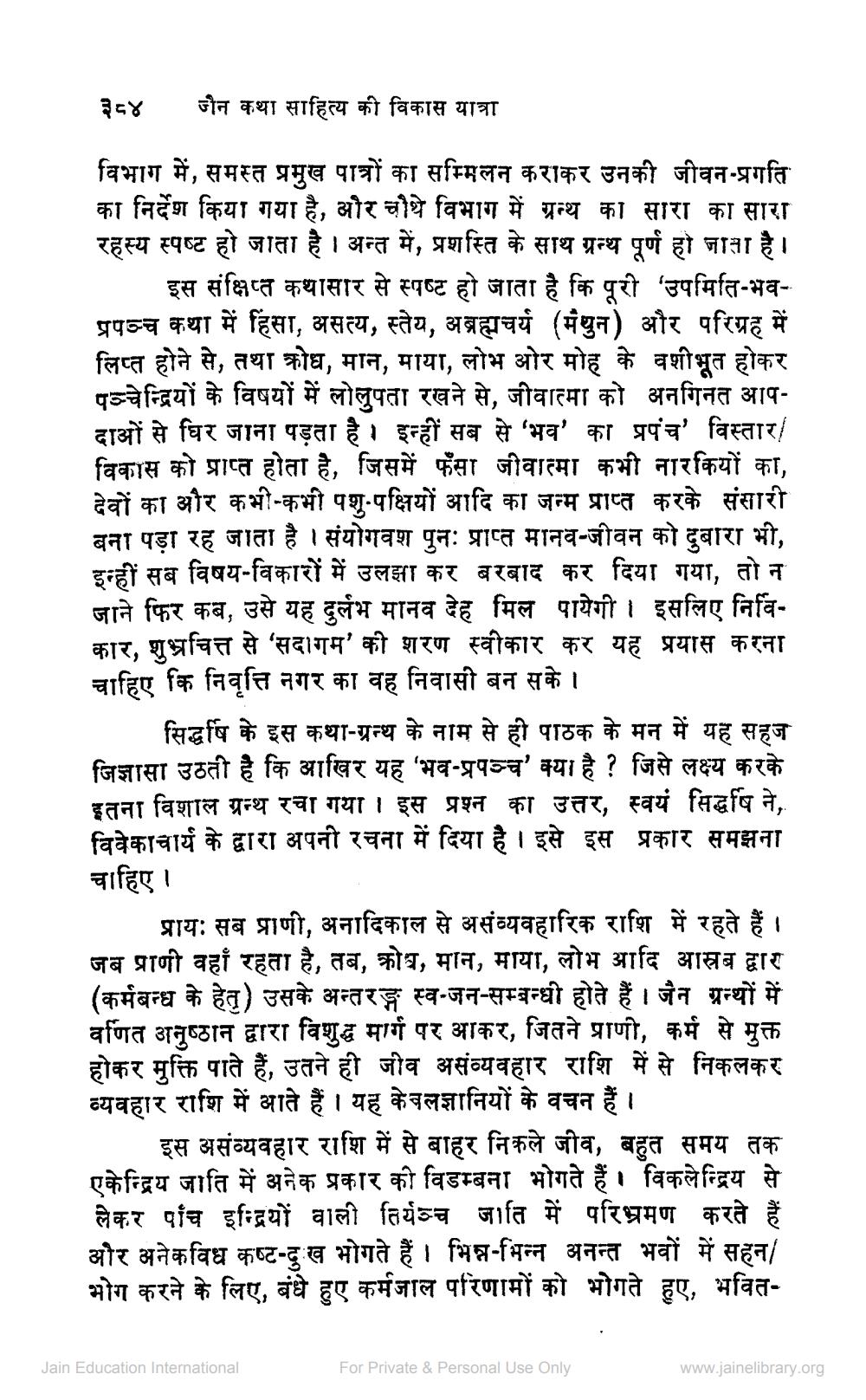________________
३-४ जैन कथा साहित्य की विकास यात्रा
विभाग में, समस्त प्रमुख पात्रों का सम्मिलन कराकर उनकी जीवन - प्रगति का निर्देश किया गया है, और चौथे विभाग में ग्रन्थ का सारा का सारा रहस्य स्पष्ट हो जाता है । अन्त में, प्रशस्ति के साथ ग्रन्थ पूर्ण हो जाता है। इस संक्षिप्त कथासार से स्पष्ट हो जाता है कि पूरी 'उपमिति भवप्रपञ्च कथा में हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य (मैथुन) और परिग्रह में लिप्त होने से, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ ओर मोह के वशीभूत होकर पञ्चेन्द्रियों के विषयों में लोलुपता रखने से, जीवात्मा को अनगिनत आपदाओं से घिर जाना पड़ता है । इन्हीं सब से 'भव' का प्रपंच' विस्तार / विकास को प्राप्त होता है, जिसमें फँसा जीवात्मा कभी नारकियों का, देवों का और कभी-कभी पशु-पक्षियों आदि का जन्म प्राप्त करके संसारी बना पड़ा रह जाता है । संयोगवश पुनः प्राप्त मानव जीवन को दुबारा भी, इन्हीं सब विषय विकारों में उलझा कर बरबाद कर दिया गया, तो न जाने फिर कब उसे यह दुर्लभ मानव देह मिल पायेगी । इसलिए निर्विकार, शुभ्रचित्त से 'सदागम' की शरण स्वीकार कर यह प्रयास करना चाहिए कि निवृत्ति नगर का वह निवासी बन सके ।
सिद्धर्षि के इस कथा - ग्रन्थ के नाम से ही पाठक के मन में यह सहज जिज्ञासा उठती है कि आखिर यह 'भव - प्रपञ्च' क्या है ? जिसे लक्ष्य करके इतना विशाल ग्रन्थ रचा गया। इस प्रश्न का उत्तर, स्वयं सिद्धषि ने, विवेकाचार्य के द्वारा अपनी रचना में दिया है । इसे इस प्रकार समझना
चाहिए ।
प्रायः सब प्राणी, अनादिकाल से असंव्यवहारिक राशि में रहते हैं । जब प्राणी वहाँ रहता है, तब, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आस्रव द्वारा ( कर्मबन्ध के हेतु ) उसके अन्तरङ्ग स्व-जन- सम्बन्धी होते हैं । जैन ग्रन्थों में वर्णित अनुष्ठान द्वारा विशुद्ध मार्ग पर आकर, जितने प्राणी, कर्म से मुक्त होकर मुक्ति पाते हैं, उतने ही जीव असंव्यवहार राशि में से निकलकर व्यवहार राशि में आते हैं । यह केवलज्ञानियों के वचन हैं ।
इस असंव्यवहार राशि में से बाहर निकले जीव, बहुत समय तक एकेन्द्रिय जाति में अनेक प्रकार की विडम्बना भोगते हैं । विकलेन्द्रिय से लेकर पाँच इन्द्रियों वाली तिर्यञ्च जाति में परिभ्रमण करते हैं और अनेकविध कष्ट-दुःख भोगते हैं । भिन्न-भिन्न अनन्त भवों में सहन / भोग करने के लिए, बंधे हुए कर्मजाल परिणामों को भोगते हुए, भवित
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org