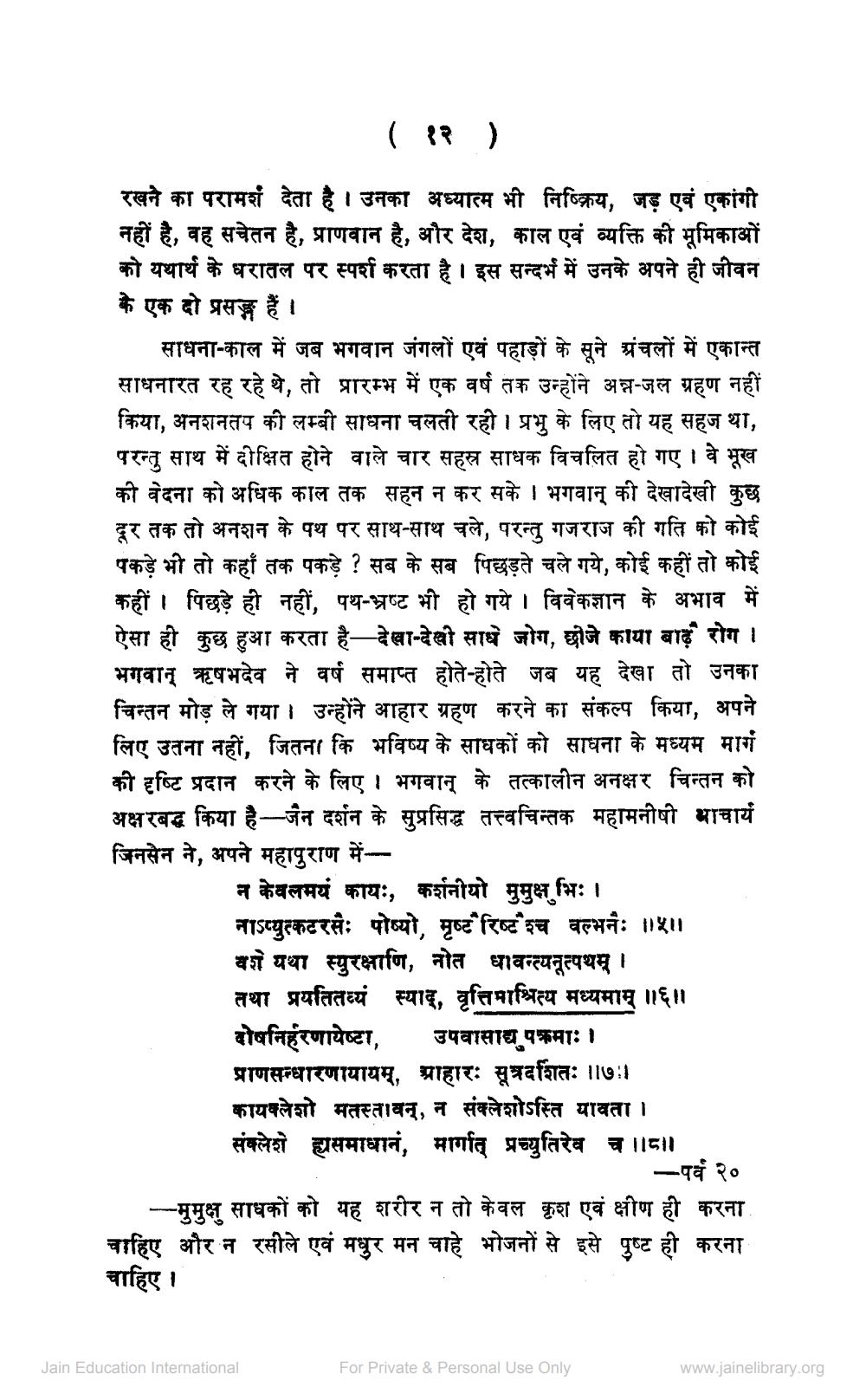________________
रखने का परामर्श देता है । उनका अध्यात्म भी निष्क्रिय, जड़ एवं एकांगी नहीं है, वह सचेतन है, प्राणवान है, और देश, काल एवं व्यक्ति की भूमिकाओं को यथार्थ के धरातल पर स्पर्श करता है। इस सन्दर्भ में उनके अपने ही जीवन के एक दो प्रसङ्ग हैं।
साधना-काल में जब भगवान जंगलों एवं पहाड़ों के सूने अंचलों में एकान्त साधनारत रह रहे थे, तो प्रारम्भ में एक वर्ष तक उन्होंने अन्न-जल ग्रहण नहीं किया, अनशनतप की लम्बी साधना चलती रही। प्रभु के लिए तो यह सहज था, परन्तु साथ में दीक्षित होने वाले चार सहस्र साधक विचलित हो गए। वे भूख की वेदना को अधिक काल तक सहन न कर सके । भगवान् की देखादेखी कुछ दूर तक तो अनशन के पथ पर साथ-साथ चले, परन्तु गजराज की गति को कोई पकड़े भी तो कहाँ तक पकड़े ? सब के सब पिछड़ते चले गये, कोई कहीं तो कोई कहीं। पिछड़े ही नहीं, पथ-भ्रष्ट भी हो गये । विवेकज्ञान के अभाव में ऐसा ही कुछ हुआ करता है—देखा-देखी साधे जोग, छोजे काया बाढ़ रोग । भगवान् ऋषभदेव ने वर्ष समाप्त होते-होते जब यह देखा तो उनका चिन्तन मोड़ ले गया। उन्होंने आहार ग्रहण करने का संकल्प किया, अपने लिए उतना नहीं, जितना कि भविष्य के साधकों को साधना के मध्यम मार्ग की दृष्टि प्रदान करने के लिए । भगवान् के तत्कालीन अनक्षर चिन्तन को अक्षरबद्ध किया है-जैन दर्शन के सुप्रसिद्ध तत्त्वचिन्तक महामनीषी भाचार्य जिनसेन ने, अपने महापुराण में
न केवलमयं कायः, कर्शनीयो मुमुक्ष भिः । नाऽप्युत्कटरसः पोष्यो, मृष्ट रिष्ट श्च वल्भनः ॥५॥ वशे यथा स्युरक्षाणि, नोत धावन्त्यनूत्पथम् । तथा प्रयतितव्यं स्याद्, वृत्तिमाश्रित्य मध्यमाम् ॥६॥ दोषनिहरणायेष्टा, उपवासाधु पक्रमाः। प्राणसन्धारणायायम्, प्राहारः सूत्रदर्शितः ।।७।। कायक्लेशो मतस्तावन्, न संक्लेशोऽस्ति यावता। संक्लेशे यसमाधानं, मार्गात् प्रच्युतिरेव च ।।८॥
-पर्व २० -~~-मुमुक्षु साधकों को यह शरीर न तो केवल कृश एवं क्षीण ही करना चाहिए और न रसीले एवं मधुर मन चाहे भोजनों से इसे पुष्ट ही करना चाहिए।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org