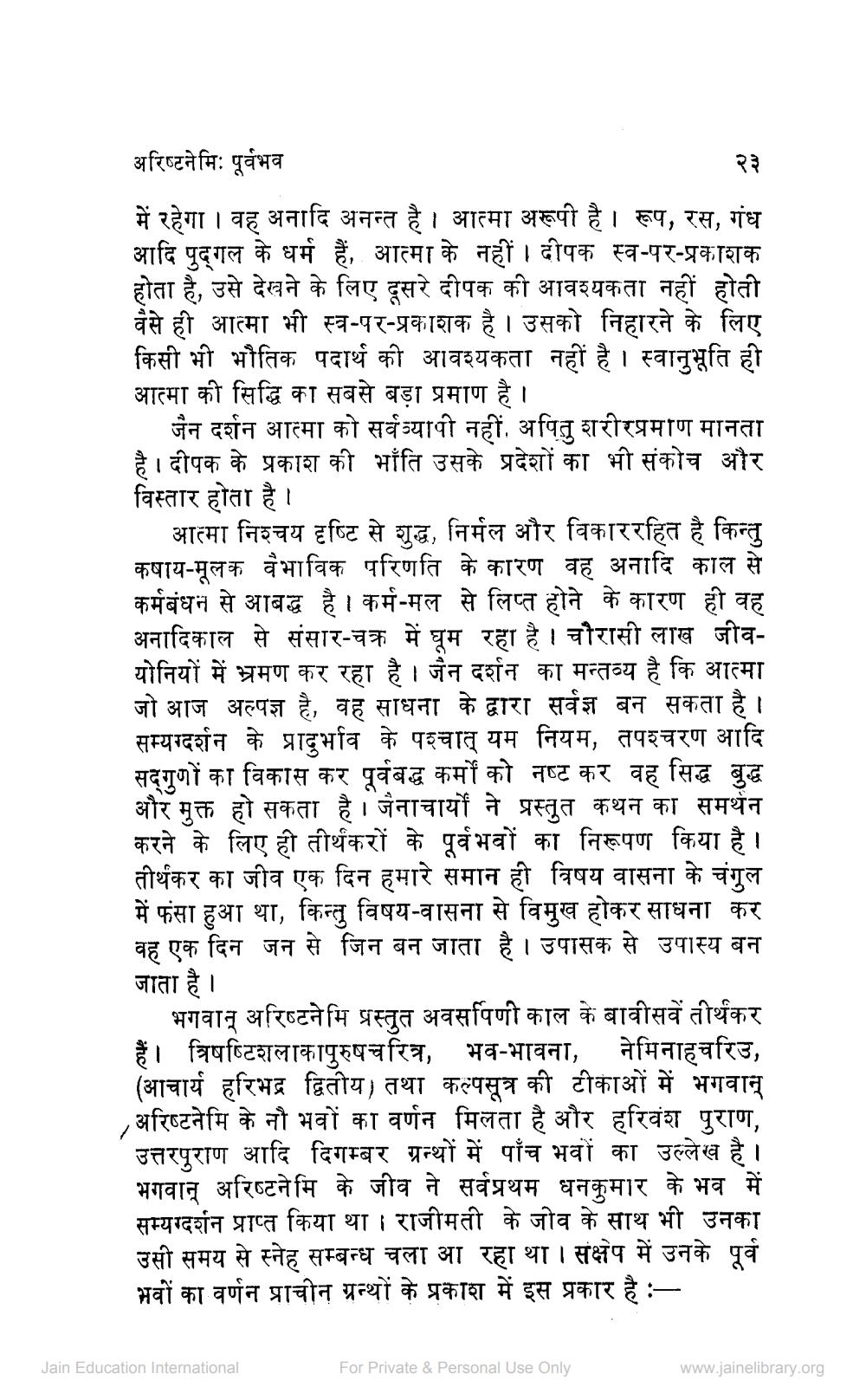________________
अरिष्टनेमिः पूर्वभव में रहेगा। वह अनादि अनन्त है। आत्मा अरूपी है। रूप, रस, गंध आदि पुद्गल के धर्म हैं, आत्मा के नहीं । दीपक स्व-पर-प्रकाशक होता है, उसे देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती वैसे ही आत्मा भी स्व-पर-प्रकाशक है । उसको निहारने के लिए किसी भी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। स्वानुभूति ही आत्मा की सिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है।
जैन दर्शन आत्मा को सर्वव्यापी नहीं, अपितु शरीरप्रमाण मानता है । दीपक के प्रकाश की भाँति उसके प्रदेशों का भी संकोच और विस्तार होता है। __ आत्मा निश्चय दृष्टि से शुद्ध, निर्मल और विकाररहित है किन्तु कषाय-मूलक वैभाविक परिणति के कारण वह अनादि काल से कर्मबंधन से आबद्ध है। कर्म-मल से लिप्त होने के कारण ही वह अनादिकाल से संसार-चक्र में घूम रहा है। चौरासी लाख जीवयोनियों में भ्रमण कर रहा है। जैन दर्शन का मन्तव्य है कि आत्मा जो आज अल्पज्ञ है, वह साधना के द्वारा सर्वज्ञ बन सकता है। सम्यग्दर्शन के प्रादुर्भाव के पश्चात् यम नियम, तपश्चरण आदि सद्गुणों का विकास कर पूर्वबद्ध कर्मों को नष्ट कर वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है। जैनाचार्यों ने प्रस्तुत कथन का समर्थन करने के लिए ही तीर्थंकरों के पूर्व भवों का निरूपण किया है। तीर्थकर का जीव एक दिन हमारे समान ही विषय वासना के चंगुल में फंसा हुआ था, किन्तु विषय-वासना से विमुख होकर साधना कर वह एक दिन जन से जिन बन जाता है । उपासक से उपास्य बन जाता है। ___ भगवान् अरिष्टनेमि प्रस्तुत अवसर्पिणी काल के बावीसवें तीर्थंकर हैं। त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, भव-भावना, नेमिनाहचरिउ, (आचार्य हरिभद्र द्वितीय) तथा कल्पसूत्र की टीकाओं में भगवान् , अरिष्टनेमि के नौ भवों का वर्णन मिलता है और हरिवंश पुराण, उत्तरपूराण आदि दिगम्बर ग्रन्थों में पाँच भवों का उल्लेख है। भगवान् अरिष्टनेमि के जीव ने सर्वप्रथम धनकूमार के भव में सम्यग्दर्शन प्राप्त किया था। राजीमती के जीव के साथ भी उनका उसी समय से स्नेह सम्बन्ध चला आ रहा था। संक्षेप में उनके पूर्व भवों का वर्णन प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाश में इस प्रकार है :
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org