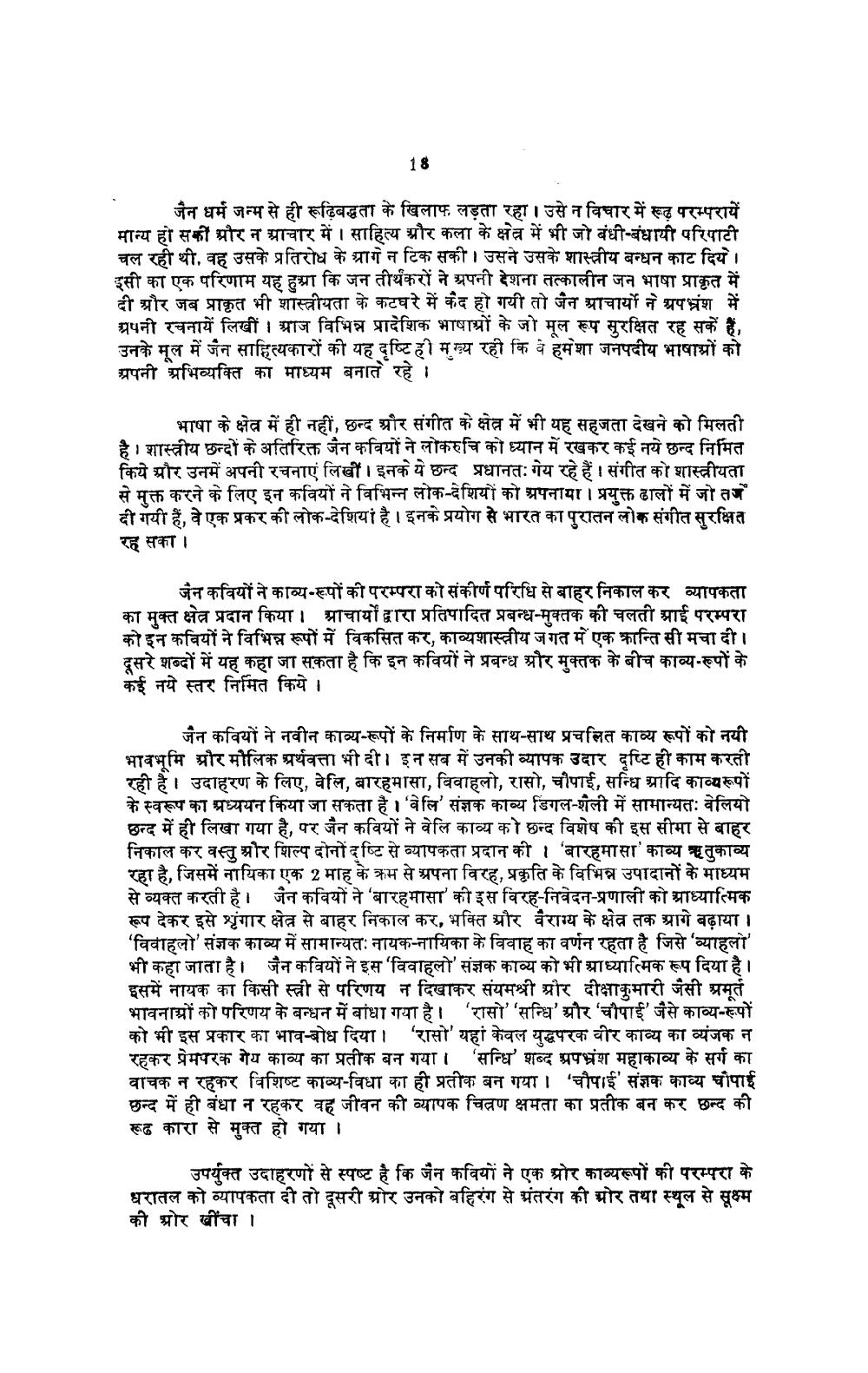________________
18
जैन धर्म जन्म से ही रूढ़िबद्धता के खिलाफ लड़ता रहा। उसे न विचार में रूढ़ परम्परायें मान्य हो सकीं और न आचार में। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी जो बंधी-बंधायी परिपाटी चल रही थी, वह उसके प्रतिरोध के आगे न टिक सकी। उसने उसके शास्त्रीय बन्धन काट दिये । इसी का एक परिणाम यह हुआ कि जन तीर्थंकरों ने अपनी देशना तत्कालीन जन भाषा प्राकृत में दी और जब प्राकृत भी शास्त्रीयता के कटघरे में कैद हो गयी तो जैन आचार्यो ने श्रपभ्रंश में अपनी रचनायें लिखीं । आज विभिन्न प्रादेशिक भाषात्रों के जो मूल रूप सुरक्षित रह सकें हैं, उनके मूल में जैन साहित्यकारों की यह दृष्टि ही मुख्य रही कि वे हमेशा जनपदीय भाषाओं को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते रहे ।
भाषा के क्षेत्र में ही नहीं, छन्द और संगीत के क्षेत्र में भी यह सहजता देखने को मिलती है । शास्त्रीय छन्दों के अतिरिक्त जैन कवियों ने लोकरुचि को ध्यान में रखकर कई नये छन्द निर्मित किये और उनमें अपनी रचनाएं लिखीं। इनके ये छन्द प्रधानतः गेय रहे हैं। संगीत को शास्त्रीयता करने के लिए इन कवियों ने विभिन्न लोक- देशियों को अपनाया । प्रयुक्त ढालों में जो त हैं, वे एक प्रकर की लोक-देशियां है। इनके प्रयोग से भारत का पुरातन लोक संगीत सुरक्षित रह सका ।
मुक्त
जैन कवियों ने काव्य रूपों की परम्परा को संकीर्ण परिधि से बाहर निकाल कर व्यापकता का मुक्त क्षेत्र प्रदान किया। प्राचार्यों द्वारा प्रतिपादित प्रबन्ध-मुक्तक की चलती आई परम्परा इन कवियों ने विभिन्न रूपों में विकसित कर, काव्यशास्त्रीय जगत में एक क्रान्ति सी मचा दी । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इन कवियों ने प्रबन्ध और मुक्तक के बीच काव्य रूपों के कई नये स्तर निर्मित किये ।
जैन कवियों ने नवीन काव्य रूपों के निर्माण के साथ-साथ प्रचलित काव्य रूपों को नयी भावभूमि और मौलिक प्रर्थवत्ता भी दी। इन सब में उनकी व्यापक उदार दृष्टि ही काम करती रही है । उदाहरण के लिए, वेलि, बारहमासा, विवाहलो, रासो, चौपाई, सन्धि आदि काव्यरूपों के स्वरूप का अध्ययन किया जा सकता है। 'वेलि' संज्ञक काव्य डिंगल शैली में सामान्यतः वेलियो छन्द में ही लिखा गया है, पर जैन कवियों ने वेलि काव्य को छन्द विशेष की इस सीमा से बाहर निकाल कर वस्तु और शिल्प दोनों दृष्टि से व्यापकता प्रदान की । 'बारहमासा' काव्य ऋतुकाव्य रहा है, जिसमें नायिका एक 2 माह के क्रम से अपना विरह, प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम
व्यक्त करती है। जैन कवियों ने 'बारहमासा' की इस विरह-निवेदन प्रणाली को आध्यात्मिक रूप देकर इसे शृंगार क्षेत्र से बाहर निकाल कर, भक्ति और वैराग्य के क्षेत्र तक आगे बढ़ाया । 'विवाहलो' संज्ञक काव्य में सामान्यतः नायक-नायिका के विवाह का वर्णन रहता है जिसे 'व्याहलो' भी कहा जाता है । जैन कवियों ने इस 'विवाहलो' संज्ञक काव्य को भी आध्यात्मिक रूप दिया है । इसमें नायक का किसी स्त्री से परिणय न दिखाकर संयमश्री श्रीर दीक्षाकुमारी जैसी मू भावनाओं को परिणय के बन्धन में बांधा गया है। 'रासो' 'सन्धि' और 'चौपाई' जैसे काव्य रूपों को भी इस प्रकार का भाव-बोध दिया । 'रासो' यहां केवल युद्धपरक वीर काव्य का व्यंजक न रहकर प्रेमपरक गेय काव्य का प्रतीक बन गया । 'सन्धि' शब्द अपभ्रंश महाकाव्य के सर्ग का वाचक न रहकर विशिष्ट काव्य-विधा का ही प्रतीक बन गया। 'चौपाई' संज्ञक काव्य चौपाई छन्द में ही बंधा न रहकर वह जीवन की व्यापक चित्रण क्षमता का प्रतीक बन कर छन्द की रूढ कारा से मुक्त हो गया ।
उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि जैन कवियों ने एक ओर काव्यरूपों की परम्परा के धरातल को व्यापकता दी तो दूसरी ओर उनको बहिरंग से अंतरंग की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर खींचा।