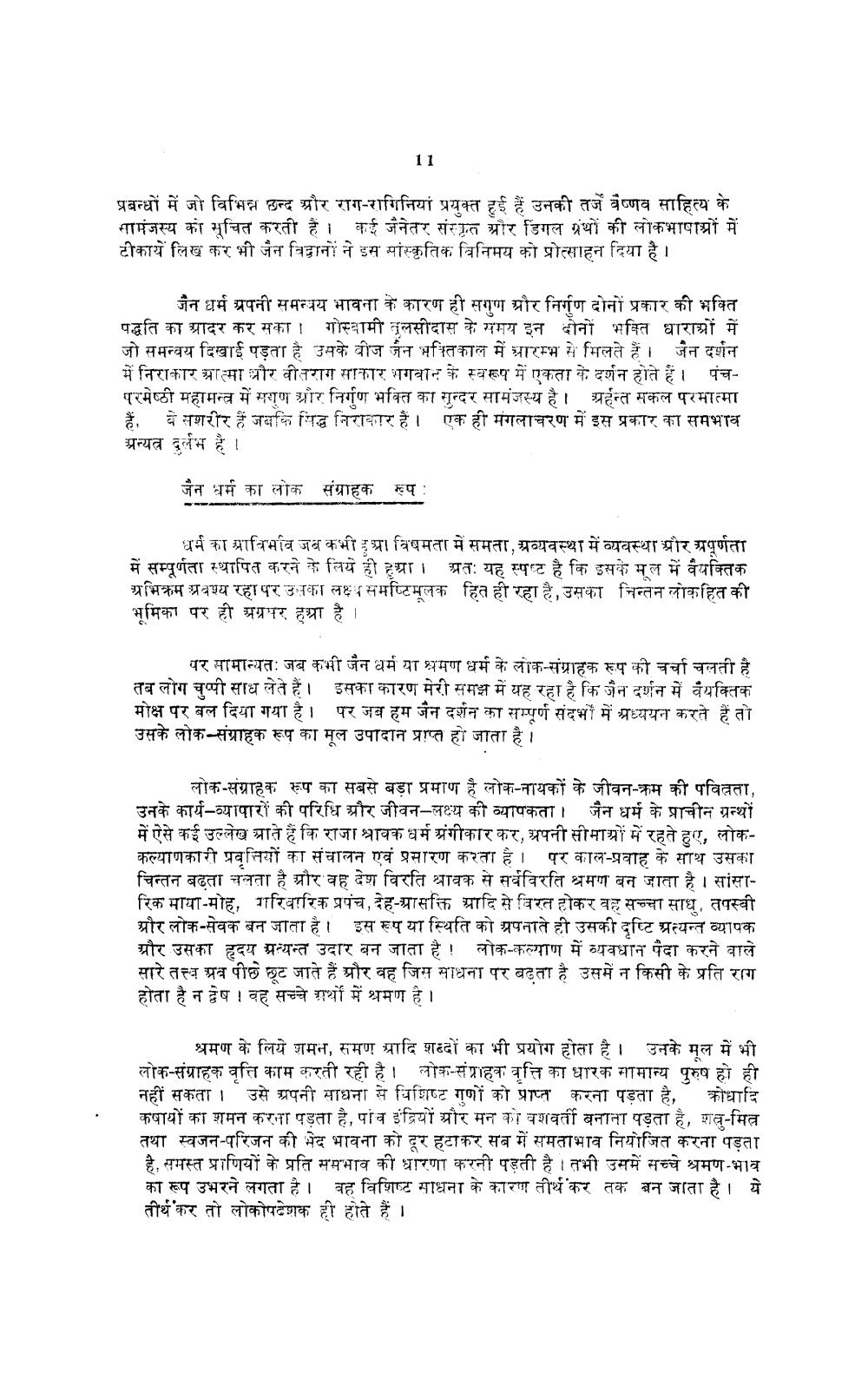________________
11
प्रबन्धों में जो विभिन्न छन्द और राग-रागिनियां प्रयक्त हुई हैं उनकी तर्जे वैष्णव साहित्य के सामंजस्य को भूचित करती हैं। कई जैनेतर संस्कृत और डिंगल ग्रंथों की लोकभाषाओं में टीकायें लिख कर भी जैन विद्वानों ने इस सांस्कृतिक विनिमय को प्रोत्साहन दिया है।
जैन धर्म अपनी समन्वय भावना के कारण ही सगुण और निर्गण दोनों प्रकार की भक्ति पद्धति का आदर कर सका। गोस्वामी तुलसीदास के समय इन दोनों भक्ति धाराओं में जो समन्वय दिखाई पड़ता है उसके बीज जैन भक्तिकाल में प्रारम्भ से मिलते हैं। जैन दर्शन में निराकार प्रात्मा और वीतराग साकार भगवान के स्वरूप में एकता के दर्शन होते हैं। पंचपरमेष्ठी महामन्त्र में मगुण और निर्गुण भक्ति का सुन्दर सामंजस्य है। अर्हन्त मकल परमात्मा हैं, के सशरीर हैं जबकि गिद्ध निराकार हैं। एक ही मंगलाचरण में इस प्रकार का समभाव अन्यत्र दुर्लभ है।
जैन धर्म का लोक संग्राहक रूप :
धर्म का प्राविभव जब कभी या विषमता में समता, अव्यवस्था में व्यवस्था और अपूर्णता में सम्पूर्णता स्थापित करने के लिये ही हया। अतः यह स्पष्ट है कि इसके मल में वैयक्तिक अभिक्रम अवश्य रहा पर उसका लक्ष्य समष्टिमूलक हित ही रहा है, उसका चिन्तन लोकहित की भमिका पर ही अग्रपर हया है।
पर सामान्यत: जब कभी जैन धर्म या श्रमण धर्म के लोक-संग्राहक रूप की चर्चा चलती है तब लोग चप्पी साध लेते हैं। इसका कारण मेरी समझ में यह रहा है कि जैन दर्शन में वैयक्तिक मोक्ष पर बल दिया गया है। पर जब हम जैन दर्शन का सम्पूर्ण संदों में अध्ययन करते हैं तो उसके लोक-संग्राहक रूप का मूल उपादान प्राप्त हो जाता है।
लोक-संग्राहक रूप का सबसे बड़ा प्रमाण है लोक-नायकों के जीवन-क्रम की पवित्रता, उनके कार्य-व्यापारों की परिधि और जीवन-लक्ष्य की व्यापकता। जैन धर्म के प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे कई उल्लेख आते हैं कि राजा श्रावक धर्म अंगीकार कर, अपनी सीमायों में रहते हए, लोककल्याणकारी प्रवृत्तियों का संचालन एवं प्रसारण करता है। पर काल-प्रवाह के साथ उसका चिन्तन बढ़ता चलता है और वह देश विरति श्रावक से सर्वविरति श्रमण बन जाता है। सांसारिक माया-मोह, गरिवारिक प्रपंच, देह-यासक्ति आदि से विरत होकर वह सच्चा साध, तपस्वी और लोक-सेवक बन जाता है। इस रूप या स्थिति को अपनाते ही उसकी दष्टि अत्यन्त व्यापक और उसका हृदय अत्यन्त उदार बन जाता है। लोक-कल्याण में व्यवधान पैदा करने वाले सारे तत्त्व अब पीछे छूट जाते हैं और वह जिस साधना पर बढ़ता है उसमें न किसी के प्रति राग होता है न द्वेष । वह सच्चे अर्थों में श्रमण है।
श्रमण के लिये शमन, समण आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। उनके मूल में भी लोक-संग्राहक वृत्ति काम करती रही है। लोक-संग्राहत वृत्ति का धारक मामान्य पुरुष हो ही नहीं सकता। उसे अपनी साधना से विशिष्ट गुणों को प्राप्त करना पड़ता है, कोधादि कषायों का शमन करना पड़ता है, पांव इंद्रियों और मन को वशवर्ती बनाना पड़ता है, शत्रु-मित्र तथा स्वजन-परिजन की भेद भावना को दूर हटाकर सब में समताभाव नियोजित करना पड़ता है,समस्त प्राणियों के प्रति समभाव की धारणा करनी पड़ती है। तभी उसमें सच्चे श्रमण-भाव का रूप उभरने लगता है। वह विशिष्ट माधना के कारण तीर्थकर तक बन जाता है। ये तीर्थ कर तो लोकोपदेशक ही होते हैं।