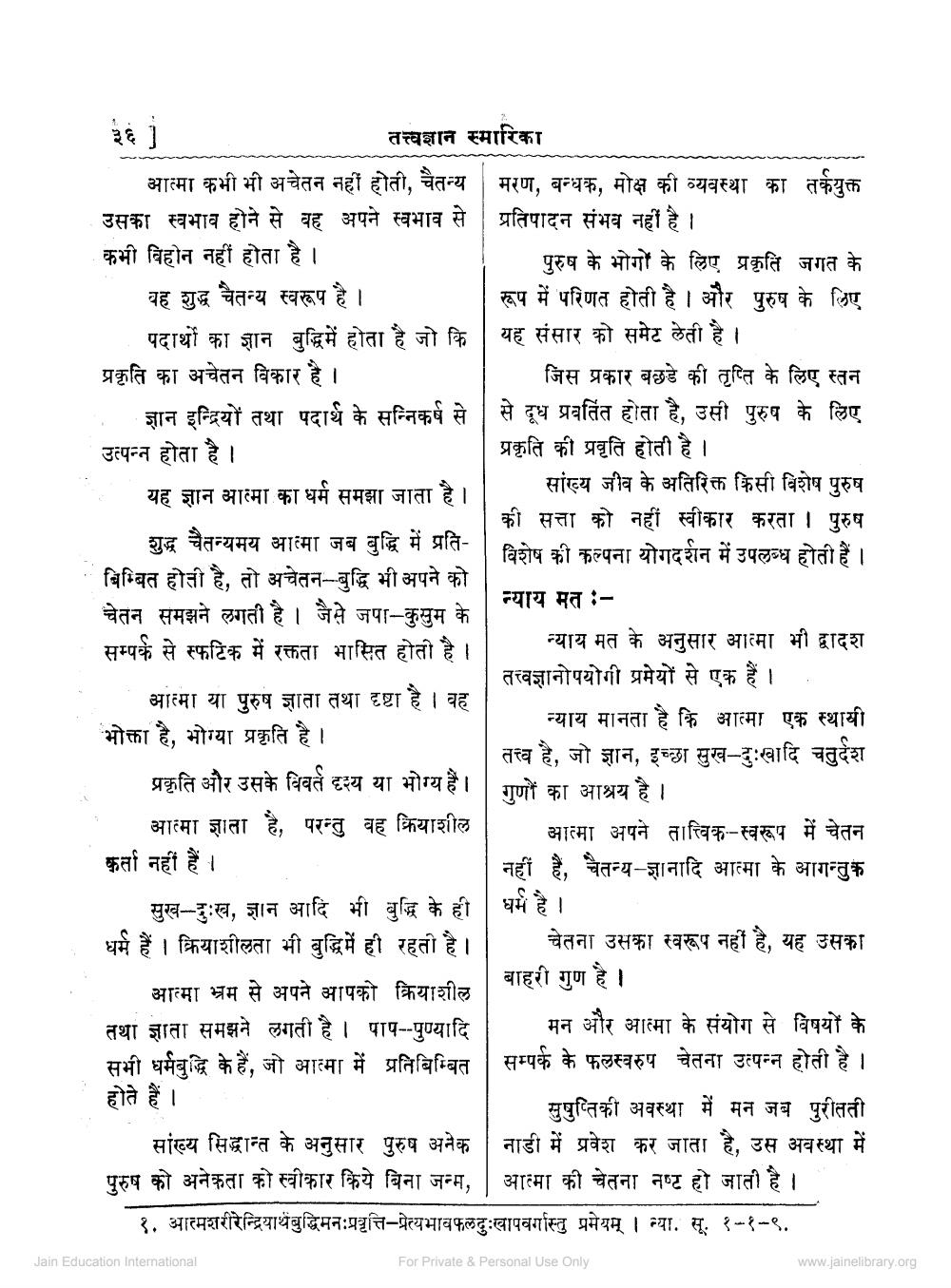________________
तत्त्वज्ञान स्मारिका आत्मा कभी भी अचेतन नहीं होती, चैतन्य मरण, बन्धक, मोक्ष की व्यवस्था का तर्कयुक्त उसका स्वभाव होने से वह अपने स्वभाव से प्रतिपादन संभव नहीं है। कभी विहोन नहीं होता है।
पुरुष के भोगों के लिए प्रकृति जगत के वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। | रूप में परिणत होती है । और पुरुष के लिए
पदार्थो का ज्ञान बुद्धिमें होता है जो कि | यह संसार को समेट लेती है । प्रकृति का अचेतन विकार है ।
जिस प्रकार बछडे की तृप्ति के लिए स्तन ज्ञान इन्द्रियों तथा पदार्थ के सन्निकर्ष से | से दूध प्रवर्तित होता है, उसी पुरुष के लिए उत्पन्न होता है।
प्रकृति की प्रवृति होती है। यह ज्ञान आत्मा का धर्म समझा जाता है ।
सांख्य जीव के अतिरिक्त किसी विशेष पुरुष
की सत्ता को नहीं स्वीकार करता । पुरुष शुद्ध चैतन्यमय आत्मा जब बुद्धि में प्रति- ।
विशेष की कल्पना योगदर्शन में उपलब्ध होती हैं । बिम्बित होती है, तो अचेतन-बुद्धि भी अपने को
न्याय मत :चेतन समझने लगती है। जैसे जपा-कुसुम के सम्पर्क से स्फटिक में रक्तता भासित होती है ।
न्याय मत के अनुसार आत्मा भी द्वादश
तत्त्वज्ञानोपयोगी प्रमेयों से एक हैं। आत्मा या पुरुष ज्ञाता तथा दृष्टा है । वह भोक्ता है, भोग्या प्रकृति है।
न्याय मानता है कि आत्मा एक स्थायी
| तत्त्व है, जो ज्ञान, इच्छा सुख-दुःखादि चतुर्दश प्रकृति और उसके विवर्त दृश्य या भोग्य है।
गुणों का आश्रय है। आत्मा ज्ञाता है, परन्तु वह क्रियाशील
आत्मा अपने तात्त्विक-स्वरूप में चेतन कर्ता नहीं हैं।
नहीं हैं, चैतन्य-ज्ञानादि आत्मा के आगन्तुक सुख-दुःख, ज्ञान आदि भी बुद्धि के ही | धर्म है। धर्म हैं । क्रियाशीलता भी बुद्धि में ही रहती है। चेतना उसका स्वरूप नहीं है, यह उसका आत्मा भ्रम से अपने आपको क्रियाशील |
बाहरी गुण है। तथा ज्ञाता समझने लगती है। पाप--पुण्यादि | मन और आत्मा के संयोग से विषयों के सभी धर्मबुद्धि के हैं, जो आत्मा में प्रतिबिम्बित | सम्पर्क के फलस्वरुप चेतना उत्पन्न होती है। होते हैं।
सुषुप्तिकी अवस्था में मन जब पुरीतती सांख्य सिद्धान्त के अनुसार पुरुष अनेक | नाडी में प्रवेश कर जाता है, उस अवस्था में पुरुष को अनेकता को स्वीकार किये बिना जन्म, | आत्मा की चेतना नष्ट हो जाती है।
१. आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्ति-प्रेत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् । न्या. सू. १-१-९.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org