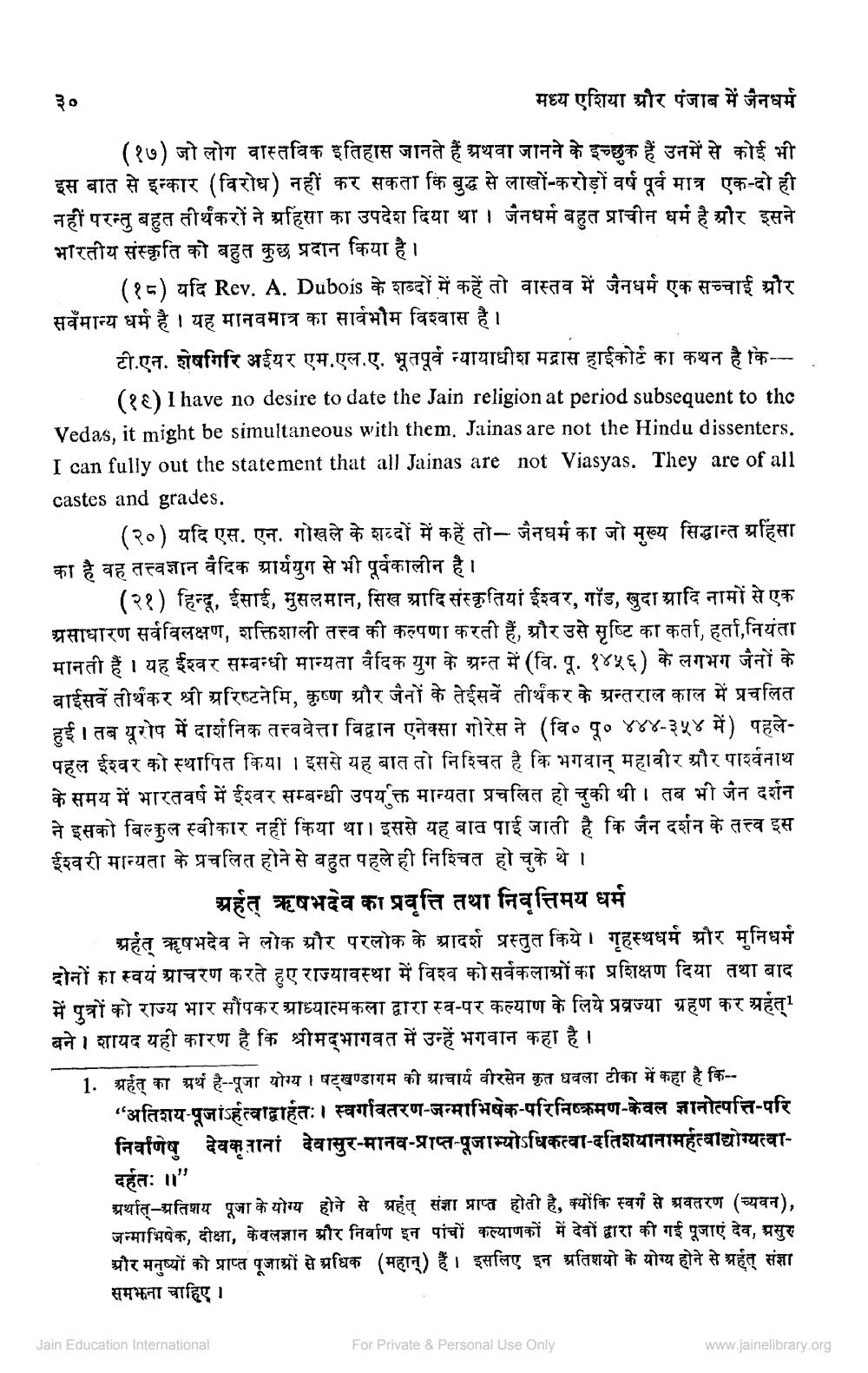________________
मध्य एशिया और पंजाब में जैनधर्म
( १७ ) जो लोग वास्तविक इतिहास जानते हैं अथवा जानने के इच्छुक हैं उनमें से कोई भी इस बात से इन्कार (विरोध) नहीं कर सकता कि बुद्ध से लाखों-करोड़ों वर्ष पूर्व मात्र एक-दो हो नहीं परन्तु बहुत तीर्थंकरों ने अहिंसा का उपदेश दिया था। जैनधर्म बहुत प्राचीन धर्म है और इसने भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ प्रदान किया है ।
३०
(१८) यदि Rev. A. Dubois के शब्दों में कहें तो वास्तव में जैनधर्म एक सच्चाई और समान्य धर्म है । यह मानवमात्र का सार्वभौम विश्वास है ।
टी. एन. शेषगिरि अईयर एम. एल. ए. भूतपूर्व न्यायाधीश मद्रास हाईकोर्ट का कथन है कि---
(१६) I have no desire to date the Jain religion at period subsequent to the Vedas, it might be simultaneous with them. Jainas are not the Hindu dissenters. I can fully out the statement that all Jainas are not Viasyas. They are of all castes and grades.
(२०) यदि एस. एन. गोखले के शब्दों में कहें तो - जैनधर्म का जो मुख्य सिद्धान्त अहिंसा का है वह तत्त्वज्ञान वैदिक प्रार्ययुग से भी पूर्वकालीन है ।
(२१) हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, सिख आदि संस्कृतियां ईश्वर, गॉड, ख़ुदा आदि नामों से एक असाधारण सर्वविलक्षण, शक्तिशाली तत्व की कल्पणा करती हैं, और उसे सृष्टि का कर्ता, हर्ता, नियंता मानती हैं । यह ईश्वर सम्बन्धी मान्यता वैदिक युग के अन्त में (वि. पू. १४५६ ) के लगभग जैनों के बाईसवें तीर्थंकर श्री अरिष्टनेमि, कृष्ण और जैनों के तेईसवें तीर्थंकर के अन्तराल काल में प्रचलित हुई। तब यूरोप में दार्शनिक तत्त्ववेत्ता विद्वान एनेक्सा गोरेस ने ( वि० पू० ४४४ - ३५४ में ) पहले - पहल ईश्वर को स्थापित किया । इससे यह बात तो निश्चित है कि भगवान् महावीर और पार्श्वनाथ के समय में भारतवर्ष में ईश्वर सम्बन्धी उपर्युक्त मान्यता प्रचलित हो चुकी थी । तब भी जैन दर्शन ने इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया था। इससे यह बात पाई जाती है कि जैन दर्शन के तत्त्व इस ईश्वरी मान्यता के प्रचलित होने से बहुत पहले ही निश्चित हो चुके थे ।
अर्हत् ऋषभदेव का प्रवृत्ति तथा निवृत्तिमय धर्म
अर्हत् ऋषभदेव ने लोक और परलोक के आदर्श प्रस्तुत किये। गृहस्थधर्म और मुनिधर्म दोनों का स्वयं प्राचरण करते हुए राज्यावस्था में विश्व को सर्वकलाओं का प्रशिक्षण दिया तथा बाद में पुत्रों को राज्य भार सौंपकर श्राध्यात्मकला द्वारा स्व-पर कल्याण के लिये प्रव्रज्या ग्रहण कर प्रर्हत् बने । शायद यही कारण है कि श्रीमद्भागवत में उन्हें भगवान कहा है ।
1. अर्हत् का अर्थ है--पूजा योग्य । षट्खण्डागम की प्राचार्य वीरसेन कृत धवला टीका में कहा है कि-"अतिशय पूजार्हत्वाद्वार्हितः । स्वर्गावतरण- जन्माभिषेक परिनिष्क्रमण- केवल ज्ञानोत्पत्ति-परि निर्वाणेषु देवकृतानां देवासुर- मानव-प्राप्त-पूजाभ्योऽधिकत्वादतिशयानामर्हत्वाद्योग्यत्वादर्हतः ॥ "
अर्थात्-प्रतिशय पूजा के योग्य होने से अर्हत् संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि स्वर्ग से अवतरण ( च्यवन), जन्माभिषेक, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण इन पांचों कल्याणकों में देवों द्वारा की गई पूजाएं देव, असुर और मनुष्यों को प्राप्त पूजाओं से अधिक ( महान् ) हैं । इसलिए इन अतिशयो के योग्य होने से अर्हत् संज्ञा समझना चाहिए ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org