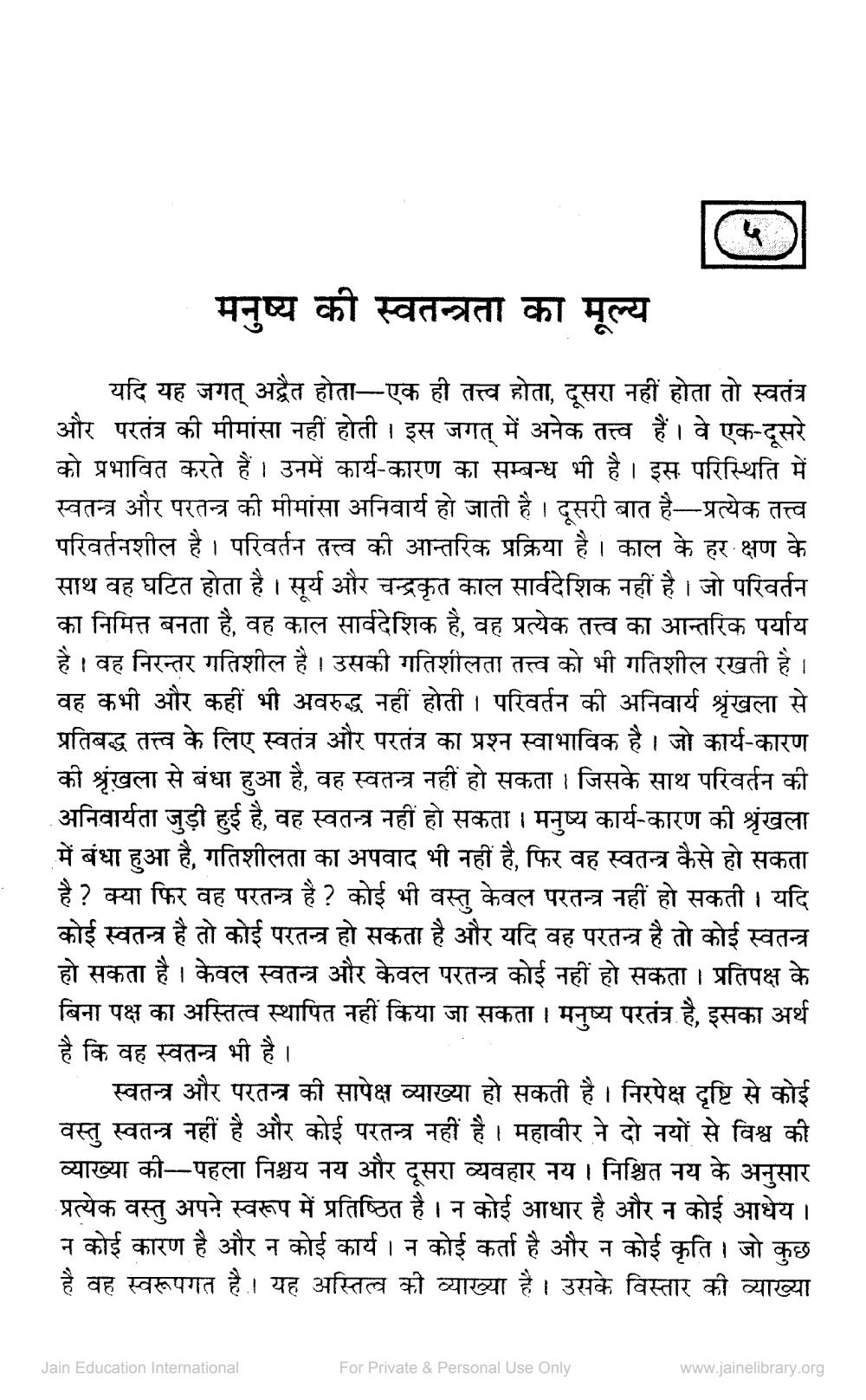________________
मनुष्य की स्वतन्त्रता का मूल्य
1
|
यदि यह जगत् अद्वैत होता - एक ही तत्त्व होता, दूसरा नहीं होता तो स्वतंत्र और परतंत्र की मीमांसा नहीं होती। इस जगत् में अनेक तत्त्व हैं । वे एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं । उनमें कार्य-कारण का सम्बन्ध भी है । इस परिस्थिति में स्वतन्त्र और परतन्त्र की मीमांसा अनिवार्य हो जाती है। दूसरी बात है - प्रत्येक तत्त्व परिवर्तनशील है । परिवर्तन तत्त्व की आन्तरिक प्रक्रिया है। काल के हर क्षण के साथ वह घटित होता है । सूर्य और चन्द्रकृत काल सार्वदेशिक नहीं है । जो परिवर्तन का निमित्त बनता है, वह काल सार्वदेशिक है, वह प्रत्येक तत्त्व का आन्तरिक पर्याय है । वह निरन्तर गतिशील है । उसकी गतिशीलता तत्त्व को भी गतिशील रखती है। वह कभी और कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती । परिवर्तन की अनिवार्य श्रृंखला से प्रतिबद्ध तत्त्व के लिए स्वतंत्र और परतंत्र का प्रश्न स्वाभाविक है। जो कार्य-कारण की श्रृंखला से बंधा हुआ है, वह स्वतन्त्र नहीं हो सकता । जिसके साथ परिवर्तन की अनिवार्यता जुड़ी हुई है, वह स्वतन्त्र नहीं हो सकता। मनुष्य कार्य-कारण की श्रृंखला में बंधा हुआ है, गतिशीलता का अपवाद भी नहीं है, फिर वह स्वतन्त्र कैसे हो सकता है ? क्या फिर वह परतन्त्र हैं ? कोई भी वस्तु केवल परतन्त्र नहीं हो सकती । यदि कोई स्वतन्त्र है तो कोई परतन्त्र हो सकता है और यदि वह परतन्त्र है तो कोई स्वतन्त्र हो सकता है । केवल स्वतन्त्र और केवल परतन्त्र कोई नहीं हो सकता । प्रतिपक्ष के बिना पक्ष का अस्तित्व स्थापित नहीं किया जा सकता। मनुष्य परतंत्र है, इसका अर्थ है कि वह स्वतन्त्र भी है ।
स्वतन्त्र और परतन्त्र की सापेक्ष व्याख्या हो सकती है । निरपेक्ष दृष्टि से कोई वस्तु स्वतन्त्र नहीं है और कोई परतन्त्र नहीं है । महावीर ने दो नयों से विश्व की व्याख्या की — पहला निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय । निश्चित नय के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है । न कोई आधार है और न कोई आधेय । न कोई कारण है और न कोई कार्य । न कोई कर्ता है और न कोई कृति । जो कुछ है वह स्वरूपगत है । यह अस्तित्व की व्याख्या है। उसके विस्तार की व्याख्या
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org