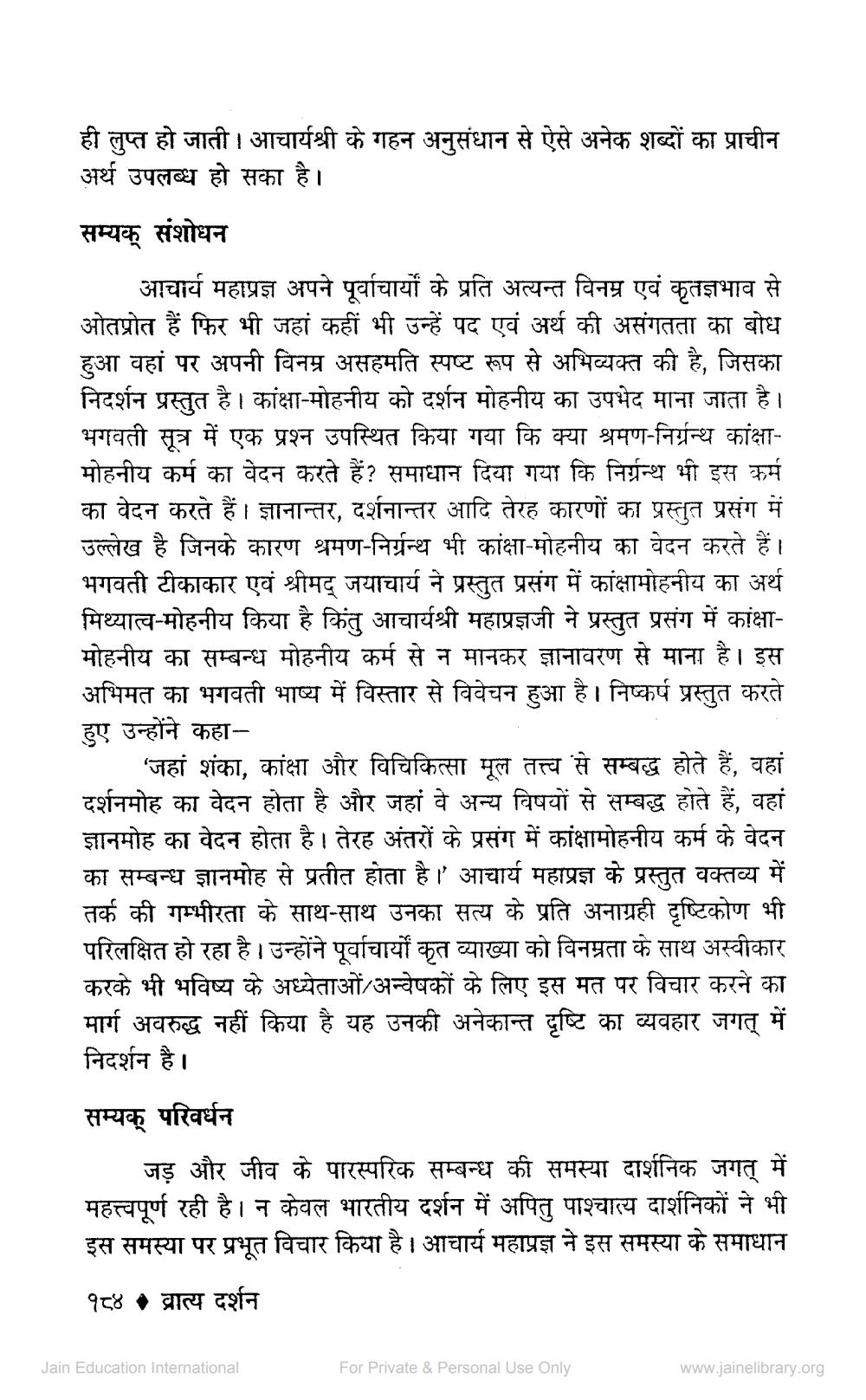________________
लुप्त हो जाती । आचार्यश्री के गहन अनुसंधान से ऐसे अनेक शब्दों का प्राचीन अर्थ उपलब्ध हो सका है
I
सम्यक् संशोधन
आचार्य महाप्रज्ञ अपने पूर्वाचार्यों के प्रति अत्यन्त विनम्र एवं कृतज्ञभाव से ओतप्रोत हैं फिर भी जहां कहीं भी उन्हें पद एवं अर्थ की असंगतता का बोध हुआ वहां पर अपनी विनम्र असहमति स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त की है, जिसका निदर्शन प्रस्तुत है । कांक्षा - मोहनीय को दर्शन मोहनीय का उपभेद माना जाता है। भगवती सूत्र में एक प्रश्न उपस्थित किया गया कि क्या श्रमण-निर्ग्रन्थ कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं? समाधान दिया गया कि निर्ग्रन्थ भी इस कर्म का वेदन करते हैं। ज्ञानान्तर, दर्शनान्तर आदि तेरह कारणों का प्रस्तुत प्रसंग में उल्लेख है जिनके कारण श्रमण-निर्ग्रन्थ भी कांक्षा - मोहनीय का वेदन करते हैं 1 भगवती टीकाकार एवं श्रीमद् जयाचार्य ने प्रस्तुत प्रसंग में कांक्षामोहनीय का अर्थ मिथ्यात्व - मोहनीय किया है किंतु आचार्यश्री महाप्रज्ञजी ने प्रस्तुत प्रसंग में कांक्षामोहनीय का सम्बन्ध मोहनीय कर्म से न मानकर ज्ञानावरण से माना है । इस अभिमत का भगवती भाष्य में विस्तार से विवेचन हुआ है । निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा
'जहां शंका, कांक्षा और विचिकित्सा मूल तत्त्व से सम्बद्ध होते हैं, वहां दर्शनमोह का वेदन होता है और जहां वे अन्य विषयों से सम्बद्ध होते हैं, वहां ज्ञानमोह का वेदन होता है। तेरह अंतरों के प्रसंग में कांक्षामोहनीय कर्म के वेदन का सम्बन्ध ज्ञानमोह से प्रतीत होता है।' आचार्य महाप्रज्ञ के प्रस्तुत वक्तव्य में तर्क की गम्भीरता के साथ-साथ उनका सत्य के प्रति अनाग्रही दृष्टिकोण भी परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने पूर्वाचार्यों कृत व्याख्या को विनम्रता के साथ अस्वीकार करके भी भविष्य के अध्येताओं/ अन्वेषकों के लिए इस मत पर विचार करने का मार्ग अवरुद्ध नहीं किया है यह उनकी अनेकान्त दृष्टि का व्यवहार जगत् में निदर्शन है ।
सम्यक् परिवर्धन
जड़ और जीव के पारस्परिक सम्बन्ध की समस्या दार्शनिक जगत् में महत्त्वपूर्ण रही है । न केवल भारतीय दर्शन में अपितु पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी इस समस्या पर प्रभूत विचार किया है। आचार्य महाप्रज्ञ ने इस समस्या के समाधान
१८४ • व्रात्य दर्शन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org