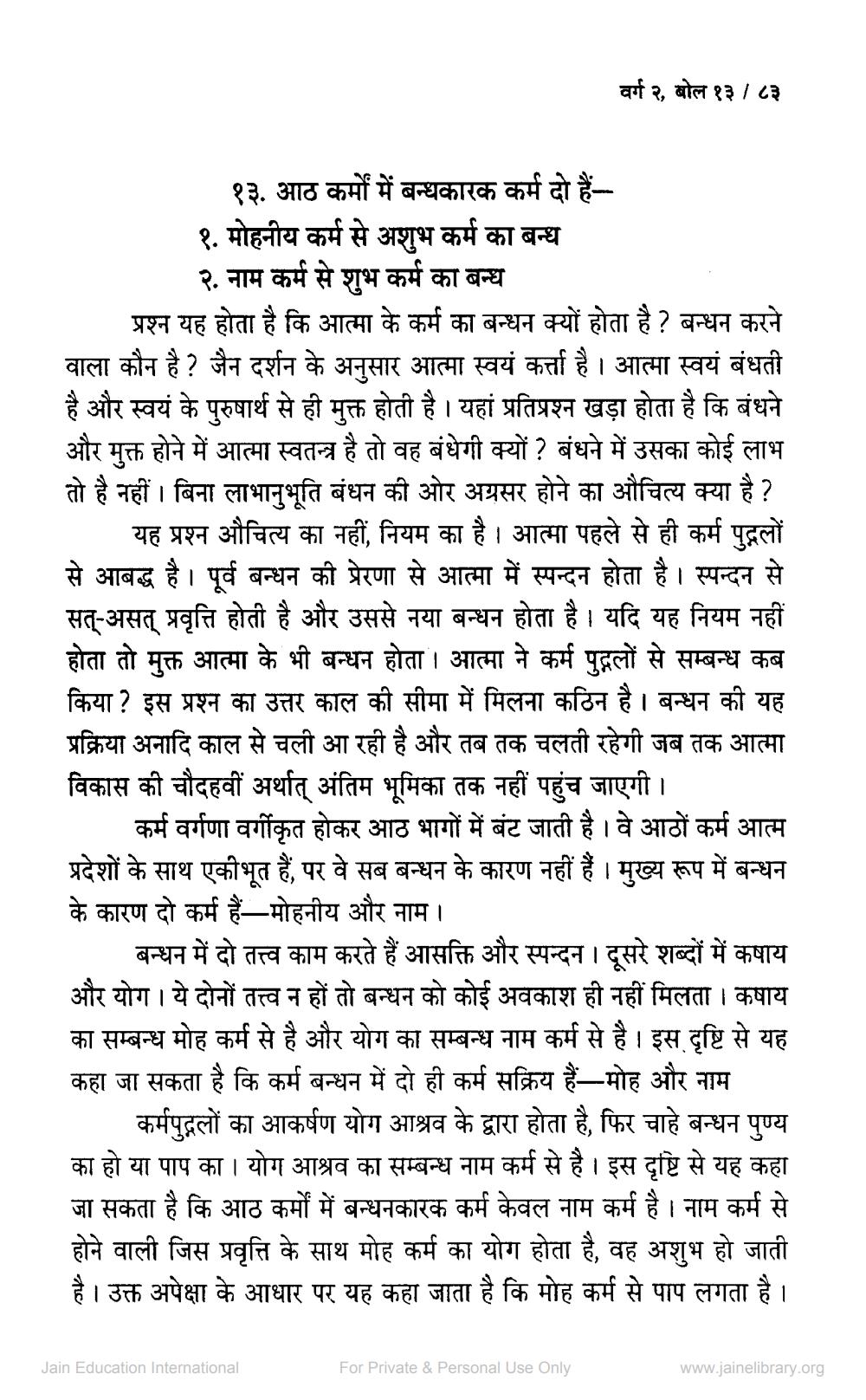________________
१३. आठ कर्मों में बन्धकारक कर्म दो हैं
१. मोहनीय कर्म से अशुभ कर्म का बन्ध २. नाम कर्म से शुभ कर्म का बन्ध
प्रश्न यह होता है कि आत्मा के कर्म का बन्धन क्यों होता है ? बन्धन करने वाला कौन है ? जैन दर्शन के अनुसार आत्मा स्वयं कर्ता है । आत्मा स्वयं बंधती है और स्वयं के पुरुषार्थ से ही मुक्त होती है। यहां प्रतिप्रश्न खड़ा होता है कि बंधने और मुक्त होने में आत्मा स्वतन्त्र है तो वह बंधेगी क्यों ? बंधने में उसका कोई लाभ तो है नहीं । बिना लाभानुभूति बंधन की ओर अग्रसर होने का औचित्य क्या है ? यह प्रश्न औचित्य का नहीं, नियम का है। आत्मा पहले से ही कर्म पुद्गलों से आबद्ध है। पूर्व बन्धन की प्रेरणा से आत्मा में स्पन्दन होता है । स्पन्दन से सत्-असत् प्रवृत्ति होती है और उससे नया बन्धन होता है । यदि यह नियम नहीं होता तो मुक्त आत्मा के भी बन्धन होता । आत्मा ने कर्म पुद्गलों से सम्बन्ध कब किया ? इस प्रश्न का उत्तर काल की सीमा में मिलना कठिन है । बन्धन की यह प्रक्रिया अनादि काल से चली आ रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक आत्मा विकास की चौदहवीं अर्थात् अंतिम भूमिका तक नहीं पहुंच जाएगी।
I
कर्म वर्गणा वर्गीकृत होकर आठ भागों में बंट जाती है । वे आठों कर्म आत्म प्रदेशों के साथ एकीभूत हैं, पर वे सब बन्धन के कारण नहीं हैं । मुख्य रूप में बन्धन के कारण दो कर्म हैं— मोहनीय और नाम ।
वर्ग २, बोल १३ / ८३
बन्धन में दो तत्त्व काम करते हैं आसक्ति और स्पन्दन । दूसरे शब्दों में कषाय और योग । ये दोनों तत्त्व न हों तो बन्धन को कोई अवकाश ही नहीं मिलता । कषाय का सम्बन्ध मोह कर्म से है और योग का सम्बन्ध नाम कर्म से है । इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि कर्म बन्धन में दो ही कर्म सक्रिय हैं— मोह और नाम
कर्मपुद्गलों का आकर्षण योग आश्रव के द्वारा होता है, फिर चाहे बन्धन पुण्य का हो या पाप का । योग आश्रव का सम्बन्ध नाम कर्म से । इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि आठ कर्मों में बन्धनकारक कर्म केवल नाम कर्म है । नाम कर्म से होने वाली जिस प्रवृत्ति के साथ मोह कर्म का योग होता है, वह अशुभ हो जाती है । उक्त अपेक्षा के आधार पर यह कहा जाता है कि मोह कर्म से पाप लगता है
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
1
www.jainelibrary.org