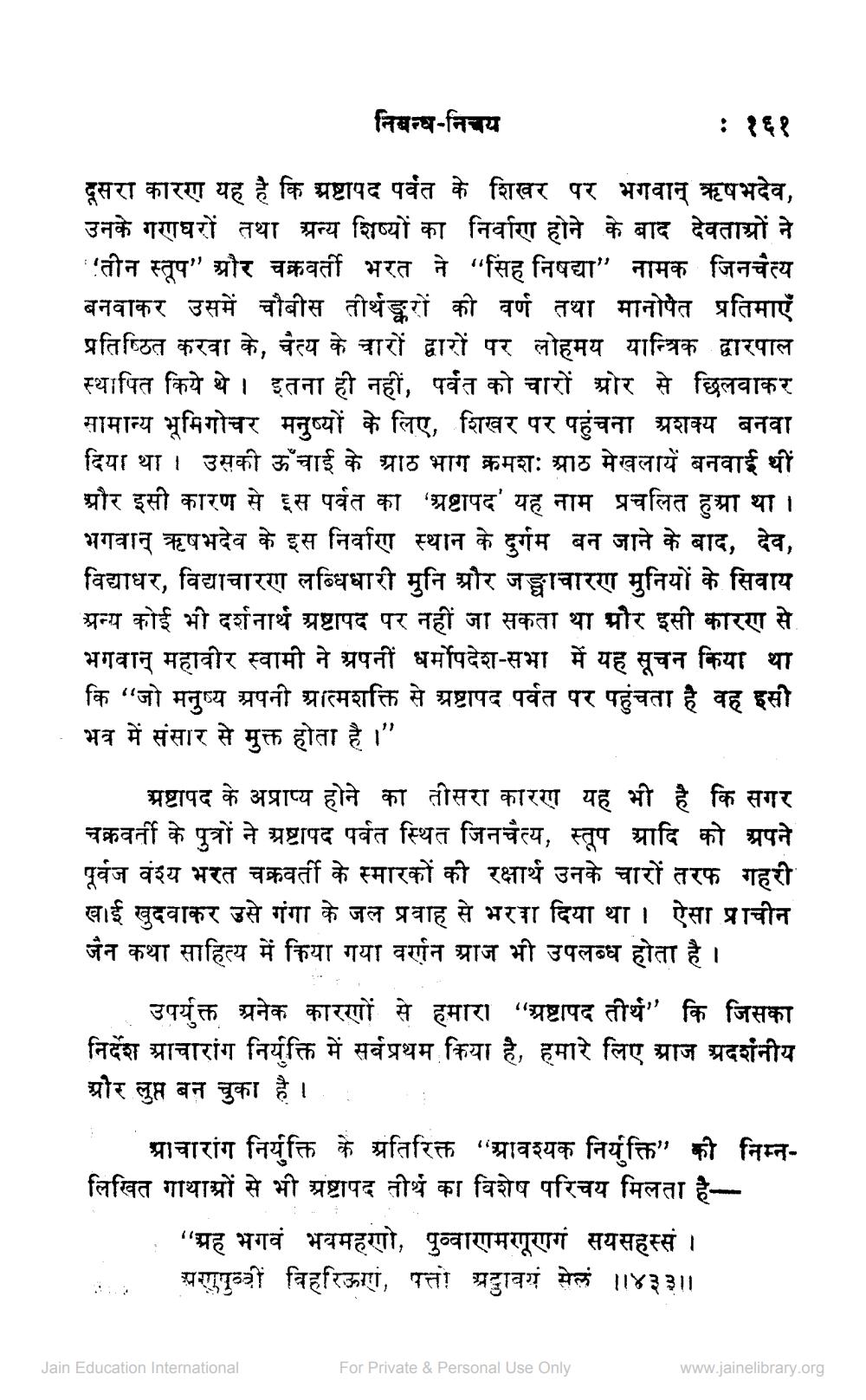________________
निबन्ध-निचय
दूसरा कारण यह है कि अष्टापद पर्वत के शिखर पर भगवान् ऋषभदेव, उनके गणघरों तथा अन्य शिष्यों का निर्वाण होने के बाद देवताओं ने 'तीन स्तूप" और चक्रवर्ती भरत ने "सिंह निषद्या" नामक जिनचैत्य बनवाकर उसमें चौबीस तीर्थङ्करों को वर्ण तथा मानोपेत प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करवा के, चैत्य के चारों द्वारों पर लोहमय यान्त्रिक द्वारपाल स्थापित किये थे। इतना ही नहीं, पर्वत को चारों ओर से छिलवाकर सामान्य भूमिगोचर मनुष्यों के लिए, शिखर पर पहुंचना अशक्य बनवा दिया था। उसकी ऊँचाई के अाठ भाग क्रमशः आठ मेखलायें बनवाई थीं और इसी कारण से इस पर्वत का 'अष्टापद' यह नाम प्रचलित हुआ था। भगवान् ऋषभदेव के इस निर्वाण स्थान के दुर्गम बन जाने के बाद, देव, विद्याधर, विद्याचारण लब्धिधारी मुनि और जङ्घाचारण मुनियों के सिवाय अन्य कोई भी दर्शनार्थ अष्टापद पर नहीं जा सकता था और इसी कारण से भगवान् महावीर स्वामी ने अपनी धर्मोपदेश-सभा में यह सूचन किया था कि "जो मनुष्य अपनी प्रात्मशक्ति से अष्टापद पर्वत पर पहुंचता है वह इसी . भव में संसार से मुक्त होता है ।" ।
अष्टापद के अप्राप्य होने का तीसरा कारण यह भी है कि सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने अष्टापद पर्वत स्थित जिनचैत्य, स्तूप आदि को अपने पूर्वज वंश्य भरत चक्रवर्ती के स्मारकों की रक्षार्थ उनके चारों तरफ गहरी खाई खुदवाकर उसे गंगा के जल प्रवाह से भरवा दिया था। ऐसा प्राचीन जैन कथा साहित्य में किया गया वर्णन आज भी उपलब्ध होता है।
उपर्युक्त अनेक कारणों से हमारा “अष्टापद तीर्थ" कि जिसका निर्देश प्राचारांग नियुक्ति में सर्वप्रथम किया है, हमारे लिए आज प्रदर्शनीय और लुप्त बन चुका है।
प्राचारांग नियुक्ति के अतिरिक्त "आवश्यक नियुक्ति" को निम्नलिखित गाथाओं से भी अष्टापद तीर्थ का विशेष परिचय मिलता है
. "ग्रह भगवं भवमहणो, पुवारणमणूणगं सयसहस्सं । .. अणुपुब्बी विहरिजागं, पत्तो अद्यावयं सेलं ॥४३३।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org