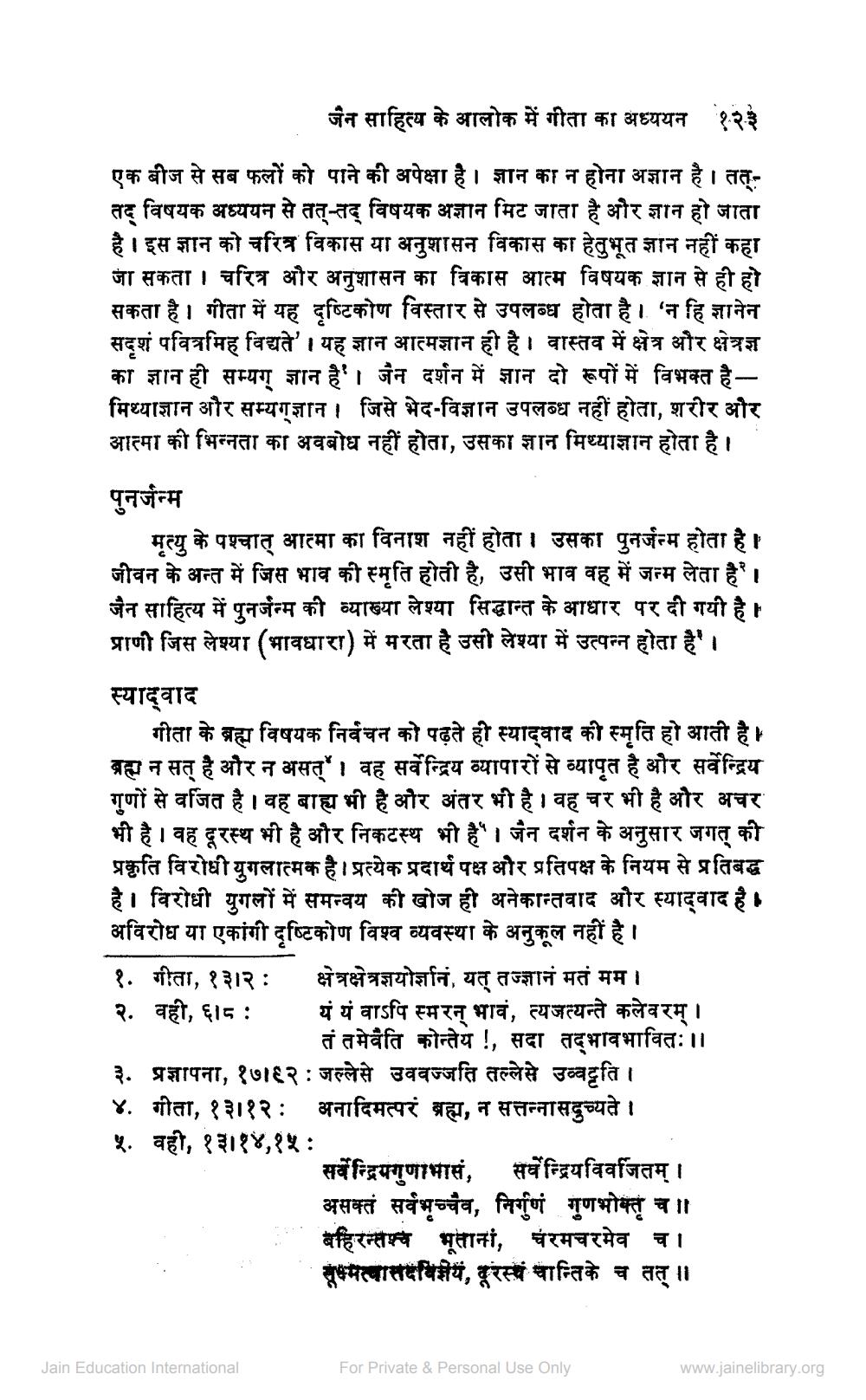________________
जैन साहित्य के आलोक में गीता का अध्ययन
एक बीज से सब फलों को पाने की अपेक्षा है। ज्ञान का न होना अज्ञान है । तत्तद् विषयक अध्ययन से तत्-तद् विषयक अज्ञान मिट जाता है और ज्ञान हो जाता है । इस ज्ञान को चरित्र विकास या अनुशासन विकास का हेतुभूत ज्ञान नहीं कहा जा सकता । चरित्र और अनुशासन का विकास आत्म विषयक ज्ञान से ही हो सकता है। गीता में यह दृष्टिकोण विस्तार से उपलब्ध होता है । 'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते' । यह ज्ञान आत्मज्ञान ही है । वास्तव में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सम्यग् ज्ञान है' । जैन दर्शन में ज्ञान दो रूपों में विभक्त हैमिथ्याज्ञान और सम्यग्ज्ञान। जिसे भेद - विज्ञान उपलब्ध नहीं होता, शरीर और आत्मा की भिन्नता का अवबोध नहीं होता, उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान होता है ।
पुनर्जन्म
मृत्यु के पश्चात् आत्मा का विनाश नहीं होता । उसका पुनर्जन्म होता है । जीवन के अन्त में जिस भाव की स्मृति होती है, उसी भाव वह में जन्म लेता है । जैन साहित्य में पुनर्जन्म की व्याख्या लेश्या सिद्धान्त के आधार पर दी गयी है । प्राणी जिस लेश्या (भावधारा) में मरता है उसी लेश्या में उत्पन्न होता है ' ।
स्याद्वाद
गीता के ब्रह्मविषयक निर्वचन को पढ़ते ही स्याद्वाद की स्मृति हो आती है । ब्रह्म न सत् है और न असत् । वह सर्वेन्द्रिय व्यापारों से व्यापृत है और सर्वेन्द्रिय वर्जित है । वह बाह्य भी है और अंतर भी है । वह चर भी है और अचर भी है । वह दूरस्थ भी है और निकटस्थ भी हैं । जैन दर्शन के अनुसार जगत् की प्रकृति विरोधी युगलात्मक है। प्रत्येक प्रदार्थ पक्ष और प्रतिपक्ष के नियम से प्रतिबद्ध है । विरोधी युगलों में समन्वय की खोज ही अनेकान्तवाद और स्याद्वाद है अविरोध या एकांगी दृष्टिकोण विश्व व्यवस्था के अनुकूल नहीं है ।
१. गीता, १३।२ : २ . वही, ६८ :
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् तज्ज्ञानं मतं मम ।
यं यं वाऽपि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥
३. प्रज्ञापना, १७।९२ : जल्ले से उववज्जति तल्लेसे उव्वदृति । ४. गीता, १३।१२: अनादिमत्परं ब्रह्म, न सत्तन्नासदुच्यते । ५. वही, १३।१४, १५ :
Jain Education International
सर्वेन्द्रियगुणाभासं,
सर्वेन्द्रियविवजितम् ।
असक्तं सर्वभृच्चैव, निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ बहिरन्तश्च भूतानां चरमचरमेव च । सूक्ष्मत्वादविज्ञेय, दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org