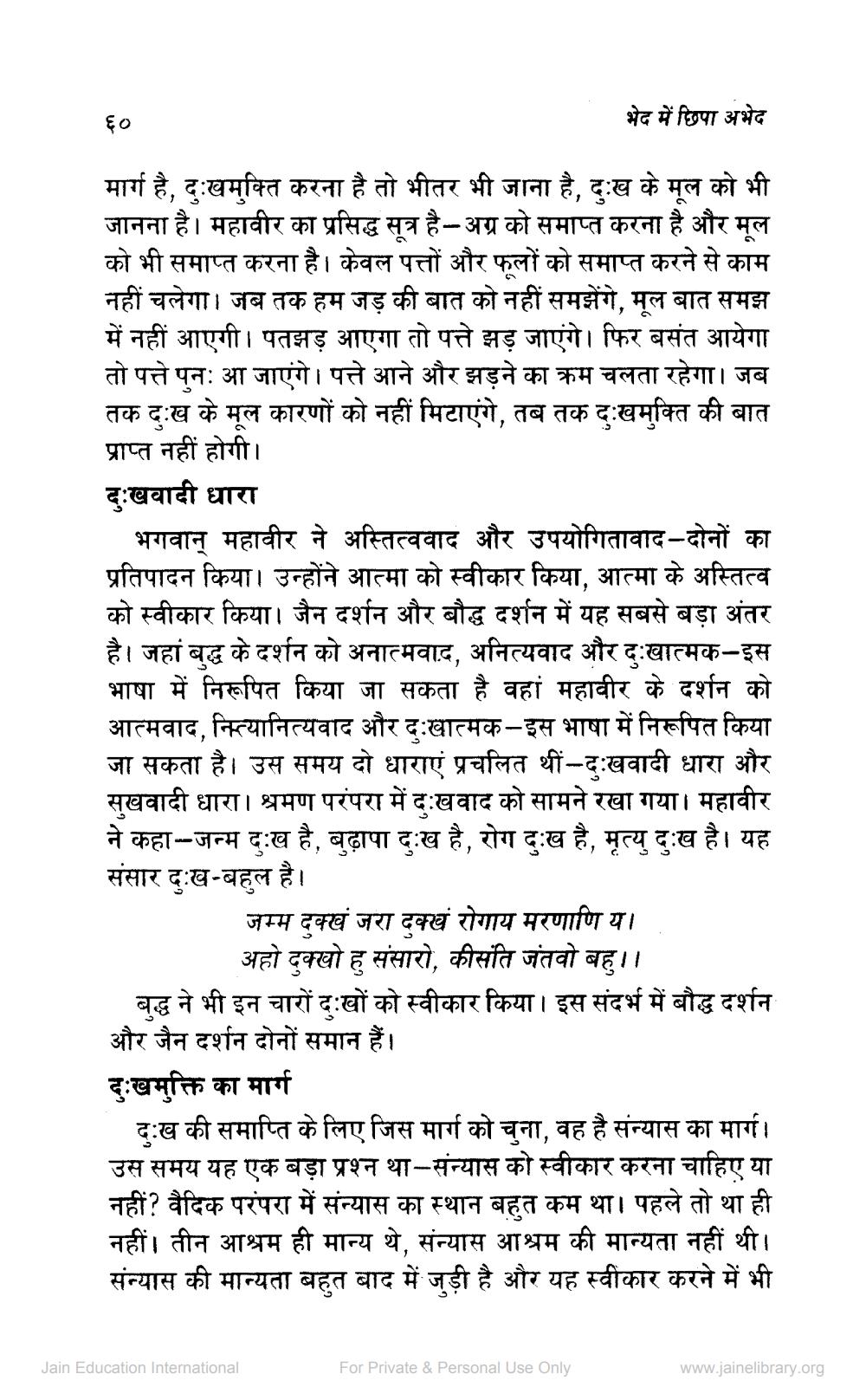________________
भेद में छिपा अभेद
मार्ग है, दुःखमुक्ति करना है तो भीतर भी जाना है, दुःख के मूल को भी जानना है। महावीर का प्रसिद्ध सूत्र है - अग्र को समाप्त करना है और मूल को भी समाप्त करना है। केवल पत्तों और फूलों को समाप्त करने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम जड़ की बात को नहीं समझेंगे, मूल बात समझ में नहीं आएगी। पतझड़ आएगा तो पत्ते झड़ जाएंगे। फिर बसंत आयेगा तो पत्ते पुनः आ जाएंगे। पत्ते आने और झड़ने का क्रम चलता रहेगा। जब तक दुःख के मूल कारणों को नहीं मिटाएंगे, तब तक दुःखमुक्ति की बात प्राप्त नहीं होगी।
६०
दुःखवादी धारा
भगवान् महावीर ने अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद - दोनों का प्रतिपादन किया। उन्होंने आत्मा को स्वीकार किया, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में यह सबसे बड़ा अंतर है। जहां बुद्ध के दर्शन को अनात्मवाद, अनित्यवाद और दुःखात्मक - इस भाषा में निरूपित किया जा सकता है वहां महावीर के दर्शन को आत्मवाद, नित्यानित्यवाद और दुःखात्मक - इस भाषा में निरूपित किया जा सकता है। उस समय दो धाराएं प्रचलित थीं- दुःखवादी धारा और सुखवादी धारा । श्रमण परंपरा में दुःखवाद को सामने रखा गया। महावीर ने कहा- जन्म दुःख है, बुढ़ापा दुःख है, रोग दुःख है, मृत्यु दुःख है। यह संसार दुःख-बहुल है।
जम्म दुक्खं जरा दुक्खं रोगाय मरणाणि य ।
अहो दुक्खो हु संसारो, कीसंति जंतवो बहु । ।
बुद्ध ने भी इन चारों दुःखों को स्वीकार किया। इस संदर्भ में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों समान हैं।
दुःखमुक्ति का मार्ग
दुःख की समाप्ति के लिए जिस मार्ग को चुना, वह है संन्यास का मार्ग । उस समय यह एक बड़ा प्रश्न था - संन्यास को स्वीकार करना चाहिए या नहीं? वैदिक परंपरा में संन्यास का स्थान बहुत कम था। पहले तो था ही नहीं। तीन आश्रम ही मान्य थे, संन्यास आश्रम की मान्यता नहीं थी । संन्यास की मान्यता बहुत बाद में जुड़ी है और यह स्वीकार करने में भी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org