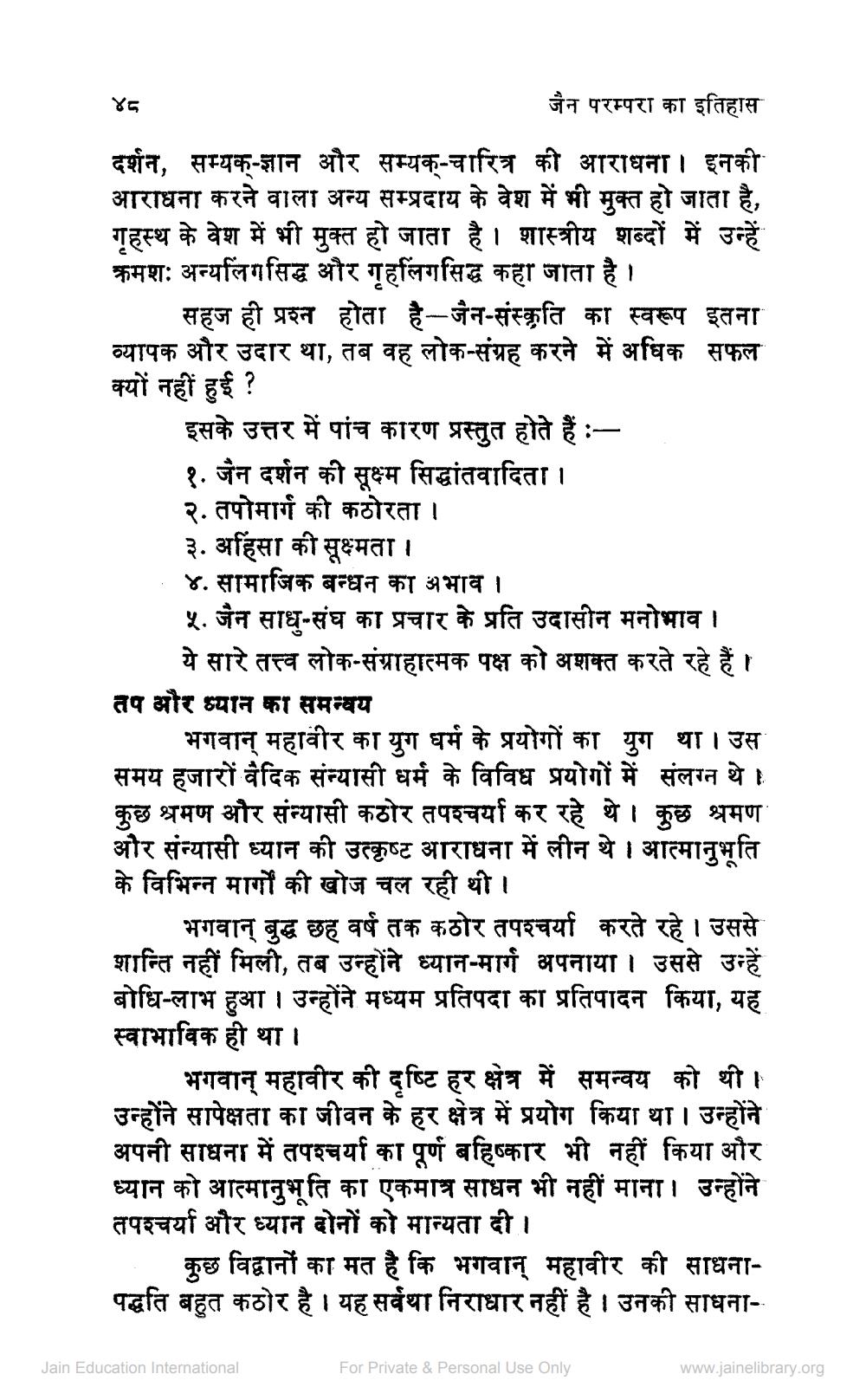________________
जैन परम्परा का इतिहास
दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र की आराधना। इनकी आराधना करने वाला अन्य सम्प्रदाय के वेश में भी मुक्त हो जाता है, गृहस्थ के वेश में भी मुक्त हो जाता है। शास्त्रीय शब्दों में उन्हें क्रमशः अयलिंगसिद्ध और गृहलिंगसिद्ध कहा जाता है।
सहज ही प्रश्न होता है-जैन-संस्कृति का स्वरूप इतना व्यापक और उदार था, तब वह लोक-संग्रह करने में अधिक सफल क्यों नहीं हुई ?
इसके उत्तर में पांच कारण प्रस्तुत होते हैं :१. जैन दर्शन की सूक्ष्म सिद्धांतवादिता । २. तपोमार्ग की कठोरता। ३. अहिंसा की सूक्ष्मता। ४. सामाजिक बन्धन का अभाव । ५. जैन साधु-संघ का प्रचार के प्रति उदासीन मनोभाव ।
ये सारे तत्त्व लोक-संग्राहात्मक पक्ष को अशक्त करते रहे हैं। तप और ध्यान का समन्वय
भगवान महावीर का युग धर्म के प्रयोगों का युग था। उस समय हजारों वैदिक संन्यासी धर्म के विविध प्रयोगों में संलग्न थे। कुछ श्रमण और संन्यासी कठोर तपश्चर्या कर रहे थे। कुछ श्रमण और संन्यासी ध्यान की उत्कृष्ट आराधना में लीन थे । आत्मानुभूति के विभिन्न मार्गों की खोज चल रही थी।
भगवान् बुद्ध छह वर्ष तक कठोर तपश्चर्या करते रहे । उससे शान्ति नहीं मिली, तब उन्होंने ध्यान-मार्ग अपनाया। उससे उन्हें बोधि-लाभ हुआ। उन्होंने मध्यम प्रतिपदा का प्रतिपादन किया, यह स्वाभाविक ही था।
भगवान् महावीर की दृष्टि हर क्षेत्र में समन्वय को थी। उन्होंने सापेक्षता का जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया था। उन्होंने अपनी साधना में तपश्चर्या का पूर्ण बहिष्कार भी नहीं किया और ध्यान को आत्मानुभूति का एकमात्र साधन भी नहीं माना। उन्होंने तपश्चर्या और ध्यान दोनों को मान्यता दी।
कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान् महावीर की साधनापद्धति बहुत कठोर है । यह सर्वथा निराधार नहीं है। उनकी साधना
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org