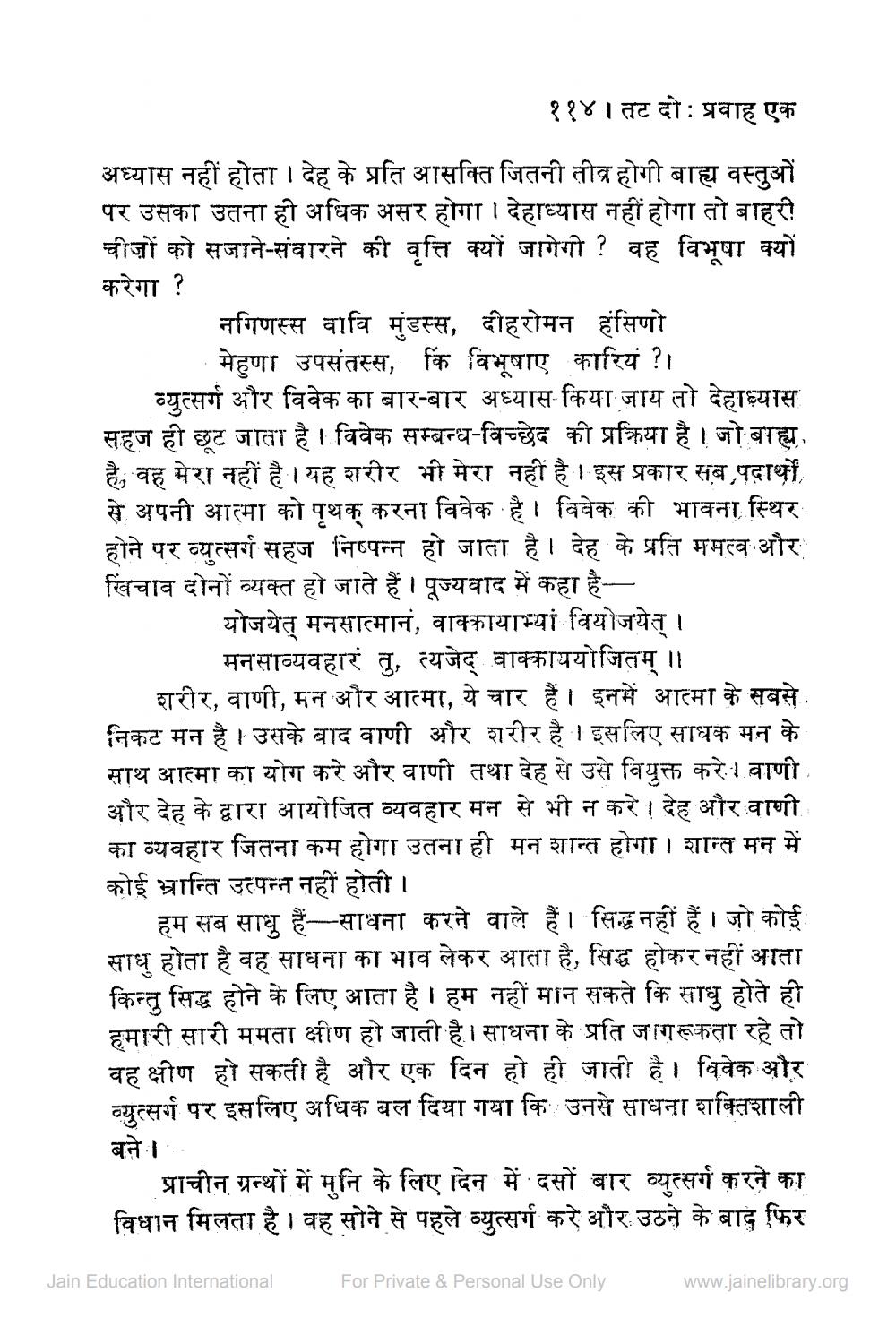________________
११४ । तट दो : प्रवाह एक
अध्यास नहीं होता । देह के प्रति आसक्ति जितनी तीव्र होगी बाह्य वस्तुओं पर उसका उतना ही अधिक असर होगा। देहाध्यास नहीं होगा तो बाहरी चीजों को सजाने-संवारने की वृत्ति क्यों जागेगी ? वह विभूषा क्यों करेगा ?
नगिणस्स वावि मुंडस्स, दीहरोमन हंसिणो
मेहुणा उपसंतस्स, किं विभूषाए कारियं ?। व्युत्सर्ग और विवेक का बार-बार अध्यास किया जाय तो देहाध्यास सहज ही छूट जाता है। विवेक सम्बन्ध-विच्छेद की प्रक्रिया है। जो बाह्य है, वह मेरा नहीं है । यह शरीर भी मेरा नहीं है । इस प्रकार सब,पदार्थों से अपनी आत्मा को पृथक करना विवेक है। विवेक की भावना स्थिर होने पर व्युत्सर्ग सहज निष्पन्न हो जाता है। देह के प्रति ममत्व और खिंचाव दोनों व्यक्त हो जाते हैं । पूज्यवाद में कहा है
योजयेत् मनसात्मानं, वाक्कायाभ्यां वियोजयेत् ।
मनसाव्यवहारं तु, त्यजेद् वाक्काययोजितम् ।। शरीर, वाणी, मन और आत्मा, ये चार हैं। इनमें आत्मा के सबसे निकट मन है। उसके बाद वाणी और शरीर है । इसलिए साधक मन के साथ आत्मा का योग करे और वाणी तथा देह से उसे वियुक्त करे। वाणी और देह के द्वारा आयोजित व्यवहार मन से भी न करे। देह और वाणी का व्यवहार जितना कम होगा उतना ही मन शान्त होगा। शान्त मन में कोई भ्रान्ति उत्पन्न नहीं होती।
हम सब साधु हैं-साधना करने वाले हैं। सिद्ध नहीं हैं । जो कोई साधु होता है वह साधना का भाव लेकर आता है, सिद्ध होकर नहीं आता किन्तु सिद्ध होने के लिए आता है। हम नहीं मान सकते कि साधु होते ही हमारी सारी ममता क्षीण हो जाती है। साधना के प्रति जागरूकता रहे तो वह क्षीण हो सकती है और एक दिन हो ही जाती है। विवेक और व्युत्सर्ग पर इसलिए अधिक बल दिया गया कि उनसे साधना शक्तिशाली बने।
प्राचीन ग्रन्थों में मुनि के लिए दिन में दसों बार व्युत्सर्ग करने का विधान मिलता है । वह सोने से पहले व्युत्सर्ग करे और उठने के बाद फिर
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org