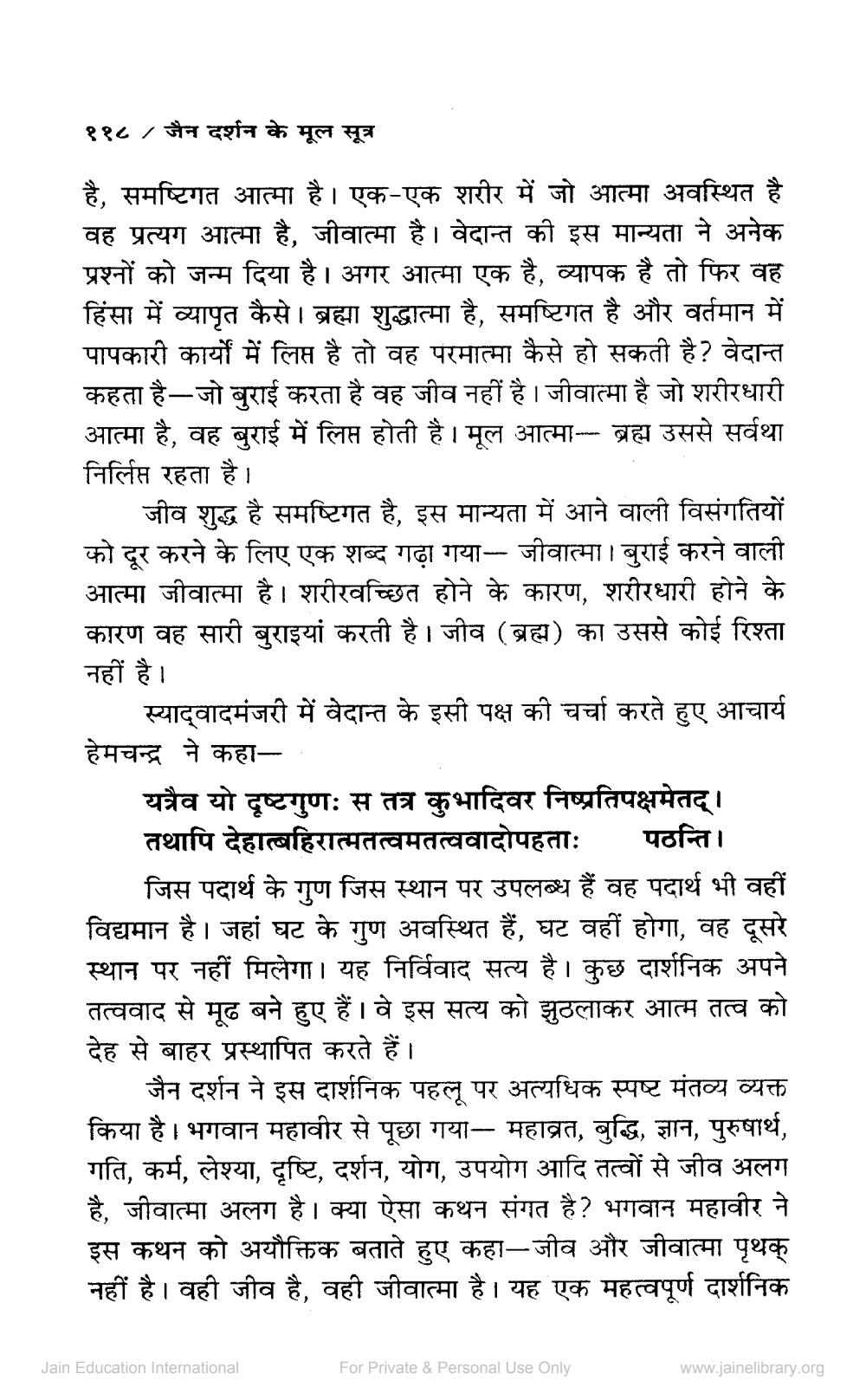________________
११८ / जैन दर्शन के मूल सूत्र
है, समष्टिगत आत्मा है। एक-एक शरीर में जो आत्मा अवस्थित है वह प्रत्यग आत्मा है, जीवात्मा है। वेदान्त की इस मान्यता ने अनेक प्रश्नों को जन्म दिया है। अगर आत्मा एक है, व्यापक है तो फिर वह हिंसा में व्याप्त कैसे। ब्रह्मा शुद्धात्मा है, समष्टिगत है और वर्तमान में पापकारी कार्यों में लिप्त है तो वह परमात्मा कैसे हो सकती है? वेदान्त कहता है-जो बुराई करता है वह जीव नहीं है । जीवात्मा है जो शरीरधारी आत्मा है, वह बुराई में लिप्त होती है। मूल आत्मा--- ब्रह्म उससे सर्वथा निर्लिप्त रहता है।
जीव शुद्ध है समष्टिगत है, इस मान्यता में आने वाली विसंगतियों को दूर करने के लिए एक शब्द गढ़ा गया- जीवात्मा। बुराई करने वाली आत्मा जीवात्मा है। शरीरवच्छित होने के कारण, शरीरधारी होने के कारण वह सारी बुराइयां करती है। जीव (ब्रह्म) का उससे कोई रिश्ता नहीं है।
स्याद्वादमंजरी में वेदान्त के इसी पक्ष की चर्चा करते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा
यत्रैव यो दृष्टगुणः स तत्र कुभादिवर निष्प्रतिपक्षमेतद्। तथापि देहात्बहिरात्मतत्वमतत्ववादोपहताः पठन्ति ।
जिस पदार्थ के गुण जिस स्थान पर उपलब्ध हैं वह पदार्थ भी वहीं विद्यमान है। जहां घट के गुण अवस्थित हैं, घट वहीं होगा, वह दूसरे स्थान पर नहीं मिलेगा। यह निर्विवाद सत्य है। कुछ दार्शनिक अपने तत्ववाद से मूढ बने हुए हैं। वे इस सत्य को झुठलाकर आत्म तत्व को देह से बाहर प्रस्थापित करते हैं।
जैन दर्शन ने इस दार्शनिक पहलू पर अत्यधिक स्पष्ट मंतव्य व्यक्त किया है। भगवान महावीर से पूछा गया- महाव्रत, बुद्धि, ज्ञान, पुरुषार्थ, गति, कर्म, लेश्या, दृष्टि, दर्शन, योग, उपयोग आदि तत्वों से जीव अलग है, जीवात्मा अलग है। क्या ऐसा कथन संगत है? भगवान महावीर ने इस कथन को अयौक्तिक बताते हुए कहा- जीव और जीवात्मा पृथक् नहीं है। वही जीव है, वही जीवात्मा है। यह एक महत्वपूर्ण दार्शनिक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org