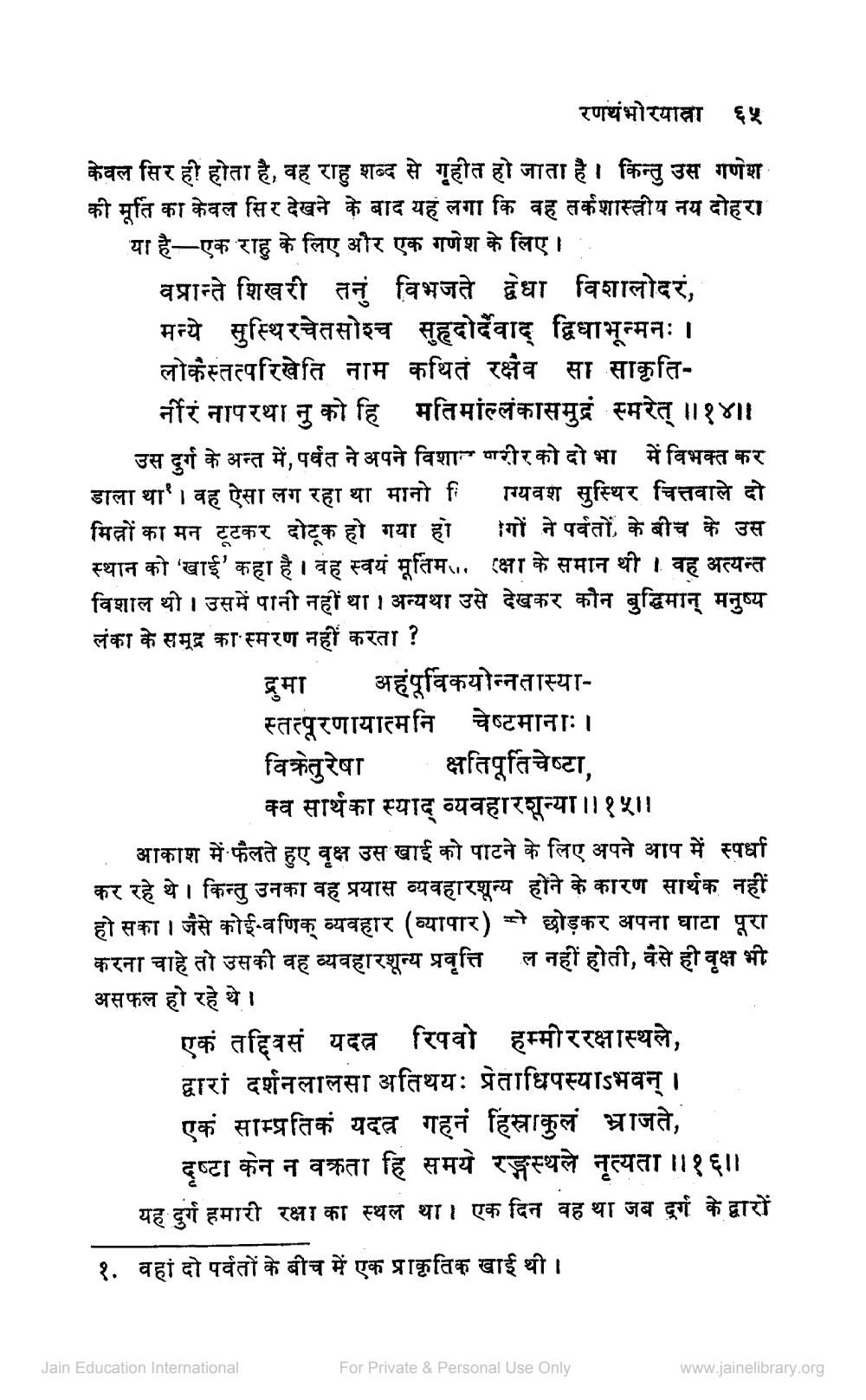________________
रणथंभोरयाता ६५
केवल सिर ही होता है, वह राहु शब्द से गृहीत हो जाता है । किन्तु उस गणेश की मूर्ति का केवल सिर देखने के बाद यह लगा कि वह तर्कशास्त्रीय नय दोहरा या है— एक राहु के लिए और एक गणेश के लिए ।
वप्रान्ते शिखरी तनुं विभजते द्वेधा विशालोदरं, मन्ये सुस्थिरचेतसोश्च सुहृदोर्देवाद् द्विधाभून्मनः । लोकैस्तत्परिखेति नाम कथितं रक्षैव सा साकृतिनीरं नापरथा नु कोहि मतिमल्लिकासमुद्रं स्मरेत् ॥ १४॥
में विभक्त कर
उस दुर्ग के अन्त में, पर्वत ने अपने विशाल पारीर को दो भा था । वह ऐसा लग रहा था मानो ग्यवश सुस्थिर चित्तवाले दो मित्रों का मन टूटकर दोटूक हो गया हो गों ने पर्वतों के बीच के उस स्थान को 'खाई' कहा है । वह स्वयं मूर्तिमा रक्षा के समान थी । वह अत्यन्त विशाल थी । उसमें पानी नहीं था । अन्यथा उसे देखकर कौन बुद्धिमान् मनुष्य लंका के समुद्र का स्मरण नहीं करता ?
द्रुमा
अहंपूर्विकयोन्नतास्या
स्तत्पूरणायात्मनि चेष्टमानाः । विक्रेतुरेषा क्षतिपूर्तिचेष्टा,
क्व सार्थका स्याद् व्यवहारशून्या ।। १५ ।।
आकाश में फैलते हुए वृक्ष उस खाई को पाटने के लिए अपने आप में स्पर्धा कर रहे थे । किन्तु उनका वह प्रयास व्यवहारशून्य होने के कारण सार्थक नहीं हो सका । जैसे कोई वणिक् व्यवहार (व्यापार) को छोड़कर अपना घाटा पूरा करना चाहे तो उसकी वह व्यवहारशून्य प्रवृत्ति ल नहीं होती, वैसे ही वृक्ष भी असफल हो रहे थे ।
एकं तद्दिवसं यदत्र रिपवो हम्मीररक्षास्थले, द्वारां दर्शनलालसा अतिथयः प्रेताधिपस्याऽभवन् । एकं साम्प्रतिकं यदत्र गहनं हिंस्राकुलं भ्राजते, दृष्टा केन न वक्रता हि समये रङ्गस्थले नृत्यता ॥ १६ ॥ यह दुर्ग हमारी रक्षा का स्थल था । एक दिन वह था जब दुर्ग के द्वारों
९. वहां दो पर्वतों के बीच में एक प्राकृतिक खाई थी ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org