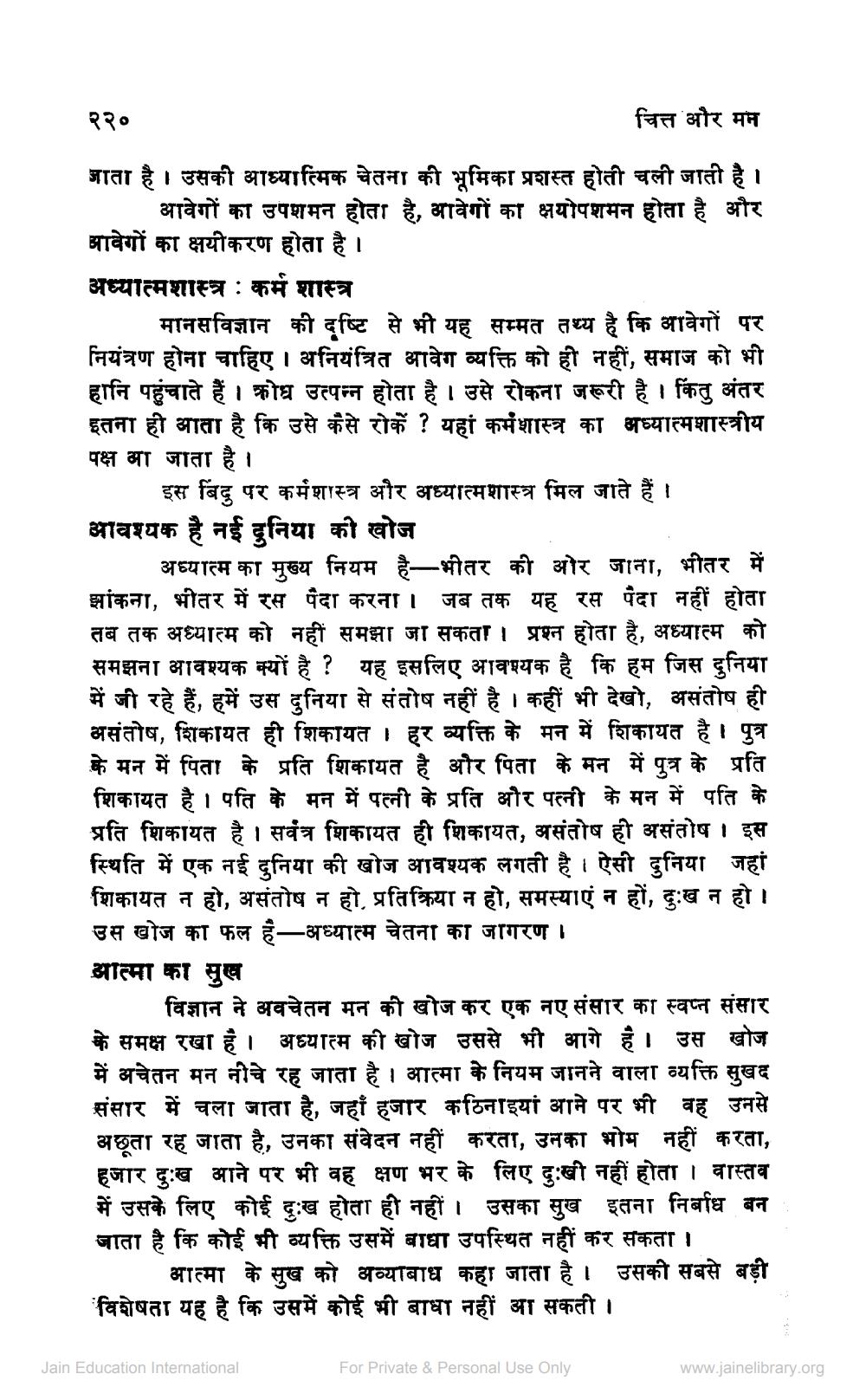________________
२२०
चित्त और मन
जाता है | उसकी आध्यात्मिक चेतना की भूमिका प्रशस्त होती चली जाती है । आवेगों का उपशमन होता है, आवेगों का क्षयोपशमन होता है और आवेगों का क्षयीकरण होता है ।
अध्यात्मशास्त्र : कर्म शास्त्र
मानसविज्ञान की दृष्टि से भी यह सम्मत तथ्य है कि आवेगों पर नियंत्रण होना चाहिए । अनियंत्रित आवेग व्यक्ति को ही नहीं, समाज को भी हानि पहुंचाते हैं । क्रोध उत्पन्न होता है । उसे रोकना जरूरी है । किंतु अंतर इतना ही आता है कि उसे कैसे रोकें ? यहां कर्मशास्त्र का अध्यात्मशास्त्रीय पक्ष आ जाता है ।
इस बिंदु पर कर्मशास्त्र और अध्यात्मशास्त्र मिल जाते हैं ।
आवश्यक है नई दुनिया की खोज
अध्यात्म का मुख्य नियम है—भीतर की ओर जाना, भीतर में झांकना, भीतर में रस पैदा करना । जब तक यह रस पैदा नहीं होता तब तक अध्यात्म को नहीं समझा जा सकता । प्रश्न होता है, अध्यात्म को समझना आवश्यक क्यों है ? यह इसलिए आवश्यक है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमें उस दुनिया से संतोष नहीं है । कहीं भी देखो, असंतोष ही असंतोष, शिकायत ही शिकायत । हर व्यक्ति के मन में शिकायत है । पुत्र के मन में पिता के प्रति शिकायत है और पिता के मन में पुत्र के प्रति शिकायत है | पति के मन में पत्नी के प्रति और पत्नी के मन में पति के प्रति शिकायत है । सर्वत्र शिकायत ही शिकायत, असंतोष ही असंतोष । इस स्थिति में एक नई दुनिया की खोज आवश्यक लगती है। ऐसी दुनिया जहां शिकायत न हो, असंतोष न हो, प्रतिक्रिया न हो, समस्याएं न हों, दुःख न हो । उस खोज का फल है - अध्यात्म चेतना का जागरण ।
आत्मा का सुख
विज्ञान ने अवचेतन मन की खोज कर एक नए संसार का स्वप्न संसार के समक्ष रखा है । अध्यात्म की खोज उससे भी आगे है । उस खोज में अचेतन मन नीचे रह जाता है । आत्मा के नियम जानने वाला व्यक्ति सुखद कठिनाइयां आने पर भी वह उनसे करता, उनका भोम नहीं करता,
संसार में चला जाता है, जहाँ हजार अछूता रह जाता है, उनका संवेदन नहीं हजार दु:ख आने पर भी वह क्षण भर के में उसके लिए कोई दुःख होता ही नहीं । जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसमें बाधा उपस्थित नहीं कर सकता । आत्मा के सुख को अव्याबाध कहा जाता है । उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें कोई भी बाधा नहीं आ सकती ।
लिए दुःखी नहीं होता । वास्तव उसका सुख इतना निर्बाध बन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org