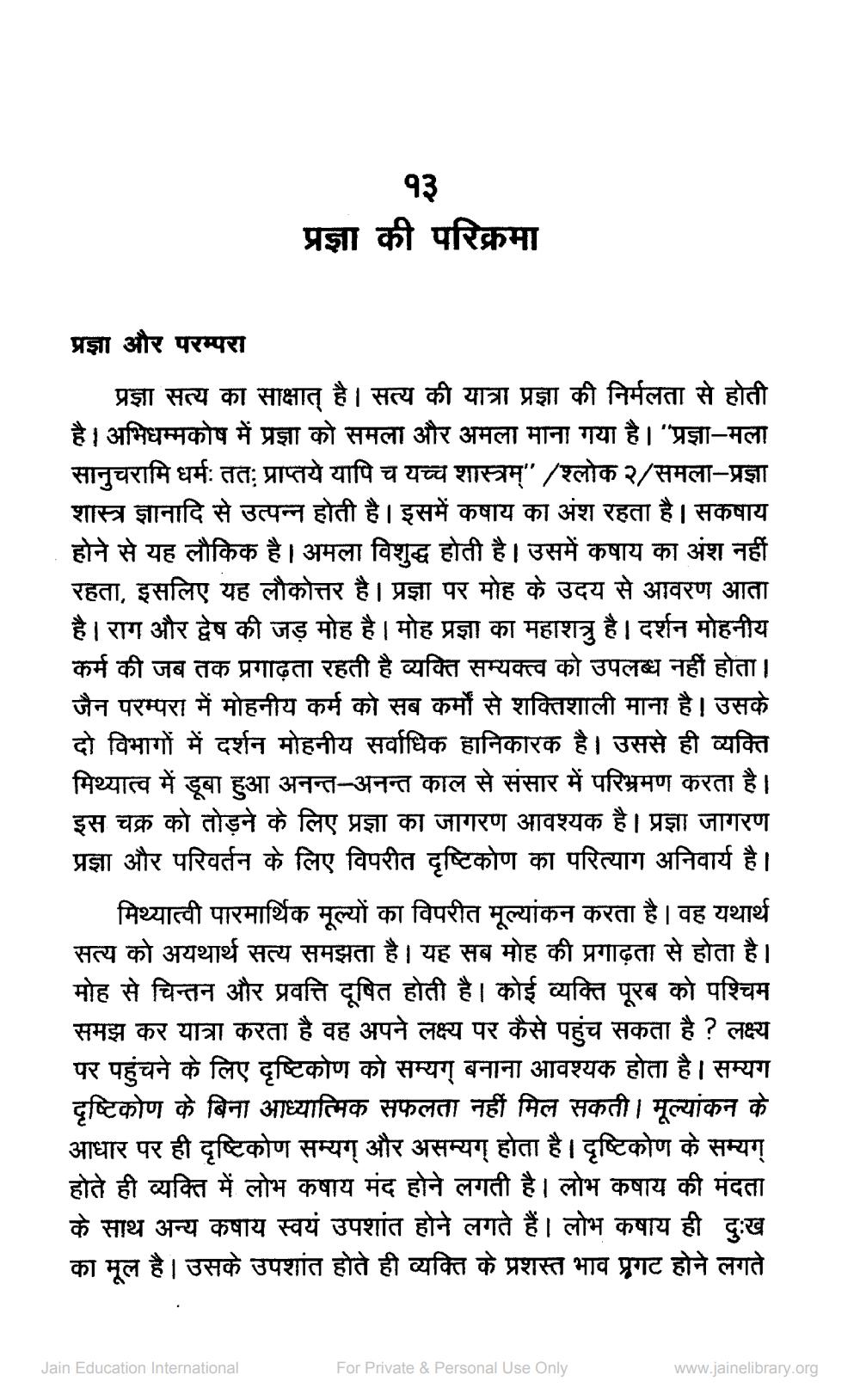________________
१३ प्रज्ञा की परिक्रमा
प्रज्ञा और परम्परा
प्रज्ञा सत्य का साक्षात् है । सत्य की यात्रा प्रज्ञा की निर्मलता से होती है। अभिधम्मकोष में प्रज्ञा को समला और अमला माना गया है। "प्रज्ञा - मला सानुचरामि धर्मः ततः प्राप्तये यापि च यच्च शास्त्रम्" / श्लोक २ / समला- प्रज्ञा शास्त्र ज्ञानादि से उत्पन्न होती है। इसमें कषाय का अंश रहता है । सकषाय होने से यह लौकिक है। अमला विशुद्ध होती है। उसमें कषाय का अंश नहीं रहता, इसलिए यह लौकोत्तर है। प्रज्ञा पर मोह के उदय से आवरण आता है। राग और द्वेष की जड़ मोह है। मोह प्रज्ञा का महाशत्रु है। दर्शन मोहनीय कर्म की जब तक प्रगाढ़ता रहती है व्यक्ति सम्यक्त्व को उपलब्ध नहीं होता । जैन परम्परा में मोहनीय कर्म को सब कर्मों से शक्तिशाली माना है। उसके दो विभागों में दर्शन मोहनीय सर्वाधिक हानिकारक है। उससे ही व्यक्ति मिथ्यात्व में डूबा हुआ अनन्त - अनन्त काल से संसार में परिभ्रमण करता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए प्रज्ञा का जागरण आवश्यक है। प्रज्ञा जागरण प्रज्ञा और परिवर्तन के लिए विपरीत दृष्टिकोण का परित्याग अनिवार्य है ।
मिथ्यात्वी पारमार्थिक मूल्यों का विपरीत मूल्यांकन करता है । वह यथार्थ सत्य को अयथार्थ सत्य समझता है। यह सब मोह की प्रगाढ़ता से होता है। मोह से चिन्तन और प्रवत्ति दूषित होती है । कोई व्यक्ति पूरब को पश्चिम समझ कर यात्रा करता है वह अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंच सकता है ? लक्ष्य पर पहुंचने के लिए दृष्टिकोण को सम्यग् बनाना आवश्यक होता है। सम्यग दृष्टिकोण के बिना आध्यात्मिक सफलता नहीं मिल सकती। मूल्यांकन के आधार पर ही दृष्टिकोण सम्यग् और असम्यग् होता है । दृष्टिकोण के सम्यग् होते ही व्यक्ति में लोभ कषाय मंद होने लगती है। लोभ कषाय की मंदता के साथ अन्य कषाय स्वयं उपशांत होने लगते हैं। लोभ कषाय ही दुःख का मूल है। उसके उपशांत होते ही व्यक्ति के प्रशस्त भाव प्रगट होने लगते
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org