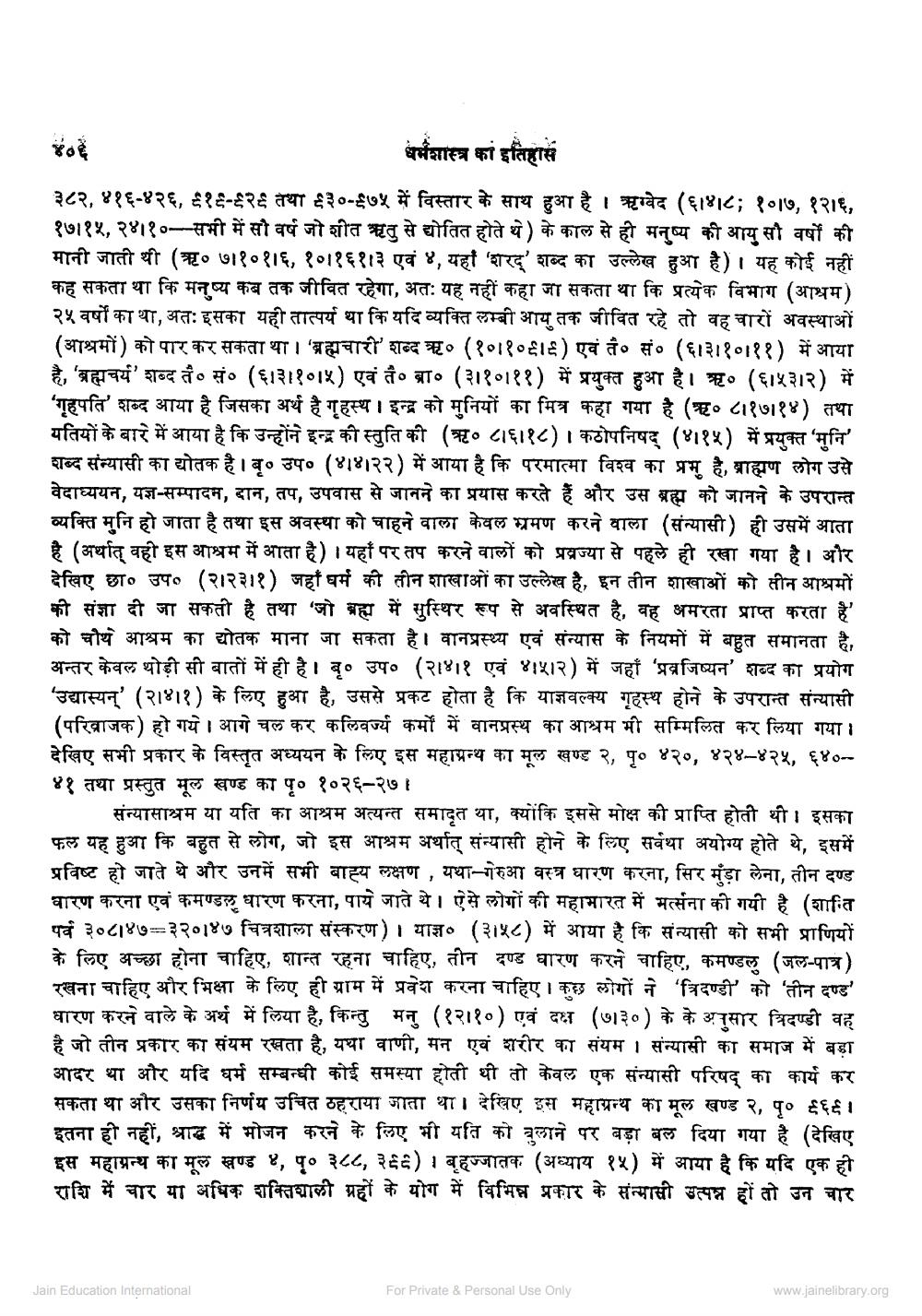________________
४०६
fare का इतिहास
३८२, ४१६-४२६, ६१६-६२६ तथा ६३०-६७५ में विस्तार के साथ हुआ है । ऋग्वेद ( ६ ४८; १०७, १२६, १७।१५, २४।१० – सभी में सौ वर्ष जो शीत ऋतु से द्योतित होते थे) के काल से ही मनुष्य की आयु सौ वर्षों की मानी जाती थी (ऋ० ७ १०१।६, १०।१६११३ एवं ४, यहाँ 'शरद्' शब्द का उल्लेख हुआ है ) । यह कोई नहीं कह सकता था कि मनुष्य कब तक जीवित रहेगा, अतः यह नहीं कहा जा सकता था कि प्रत्येक विभाग (आश्रम ) २५ वर्षों का था, अतः इसका यही तात्पर्य था कि यदि व्यक्ति लम्बी आयु तक जीवित रहे तो वह चारों अवस्थाओं (आश्रमों) को पार कर सकता था। 'ब्रह्मचारी' शब्द ऋ० (१०।१०६१६) एवं तै० सं० (६।३।१०।११ ) में आया है, 'ब्रह्मचर्य' शब्द तै० सं० (६|३|१०|५) एवं तै० ब्रा० ( ३।१०।११ ) में प्रयुक्त हुआ है । ऋ० (६०५३।२ ) में 'गृहपति' शब्द आया है जिसका अर्थ है गृहस्थ । इन्द्र को मुनियों का मित्र कहा गया है (ऋ० ८ १७/१४ ) तथा यतियों के बारे में आया है कि उन्होंने इन्द्र की स्तुति की (ऋ० ८२६ । १८ ) । कठोपनिषद् ( ४।१५) में प्रयुक्त 'मुनि' शब्द संन्यासी का द्योतक है । बृ० उप० ( ४ । ४ । २२ ) में आया है कि परमात्मा विश्व का प्रभु है, ब्राह्मण लोग उसे वेदाध्ययन, यज्ञ-सम्पादन, दान, तप, उपवास से जानने का प्रयास करते हैं और उस ब्रह्म को जानने के उपरान्त व्यक्ति मुनि हो जाता है तथा इस अवस्था को चाहने वाला केवल भ्रमण करने वाला ( संन्यासी) ही उसमें आता है ( अर्थात् वही इस आश्रम में आता है) । यहाँ पर तप करने वालों को प्रव्रज्या से पहले ही रखा गया है। और देखिए छा० उप० (२।२३।१ ) जहाँ धर्म की तीन शाखाओं का उल्लेख है, इन तीन शाखाओं को तीन आश्रमों की संज्ञा दी जा सकती है तथा 'जो ब्रह्म में सुस्थिर रूप से अवस्थित है, वह अमरता प्राप्त करता है' को चौथे आश्रम का द्योतक माना जा सकता है । वानप्रस्थ्य एवं संन्यास के नियमों में बहुत समानता है, अन्तर केवल थोड़ी सी बातों में ही है । बृ० उप० (२।४।१ एवं ४|५|२ ) में जहाँ 'प्रव्रजिष्यन' शब्द का प्रयोग 'उद्यास्यन्' (२।४।१) के लिए हुआ है, उससे प्रकट होता है कि याज्ञवल्क्य गृहस्थ होने के उपरान्त संन्यासी (परिव्राजक ) हो गये । आगे चल कर कलिवर्ज्य कर्मों में वानप्रस्थ का आश्रम मी सम्मिलित कर लिया गया । देखिए सभी प्रकार के विस्तृत अध्ययन के लिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पृ० ४२०, ४२४-४२५, ६४०-४१ तथा प्रस्तुत मूल खण्ड का पृ० १०२६-२७ ।
संन्यासाश्रम या यति का आश्रम अत्यन्त समादृत था, क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती थी । इसका फल यह हुआ कि बहुत से लोग, जो इस आश्रम अर्थात् संन्यासी होने के लिए सर्वथा अयोग्य होते थे, इसमें प्रविष्ट हो जाते थे और उनमें सभी बाह्य लक्षण, यथा- गेरुआ वस्त्र धारण करना, सिर मुंड़ा लेना, तीन दण्ड वारण करना एवं कमण्डलु धारण करना, पाये जाते थे । ऐसे लोगों की महाभारत में भर्त्सना की गयी है (शान्ति पर्व ३०८।४७=३२०।४७ चित्रशाला संस्करण) । याज्ञ० ( ३।५८) में आया है कि संन्यासी को सभी प्राणियों के लिए अच्छा होना चाहिए, शान्त रहना चाहिए, तीन दण्ड धारण करने चाहिए, कमण्डलु ( जल - पात्र ) रखना चाहिए और भिक्षा के लिए ही ग्राम में प्रवेश करना चाहिए । कुछ लोगों ने 'त्रिदण्डी' को 'तीन दण्ड' धारण करने वाले के अर्थ में लिया है, किन्तु मनु ( १२।१० ) एवं दक्ष ७।३० ) के के अनुसार त्रिदण्डी वह है जो तीन प्रकार का संयम रखता है, यथा वाणी, मन एवं शरीर का संयम । संन्यासी का समाज में बड़ा आदर था और यदि धर्म सम्बन्धी कोई समस्या होती थी तो केवल एक संन्यासी परिषद् का कार्य कर सकता था और उसका निर्णय उचित ठहराया जाता था । देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पृ० ६६६ । इतना ही नहीं, श्राद्ध में भोजन करने के लिए भी यति को बुलाने पर बड़ा बल दिया गया है ( देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड ४, पृ० ३८८, ३६६) । बृहज्जातक (अध्याय १५ ) में आया है कि यदि एक ही राशि में चार या अधिक शक्तिशाली ग्रहों के योग में विभिन्न प्रकार के संन्यासी उत्पन्न हों तो उन चार
(
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org