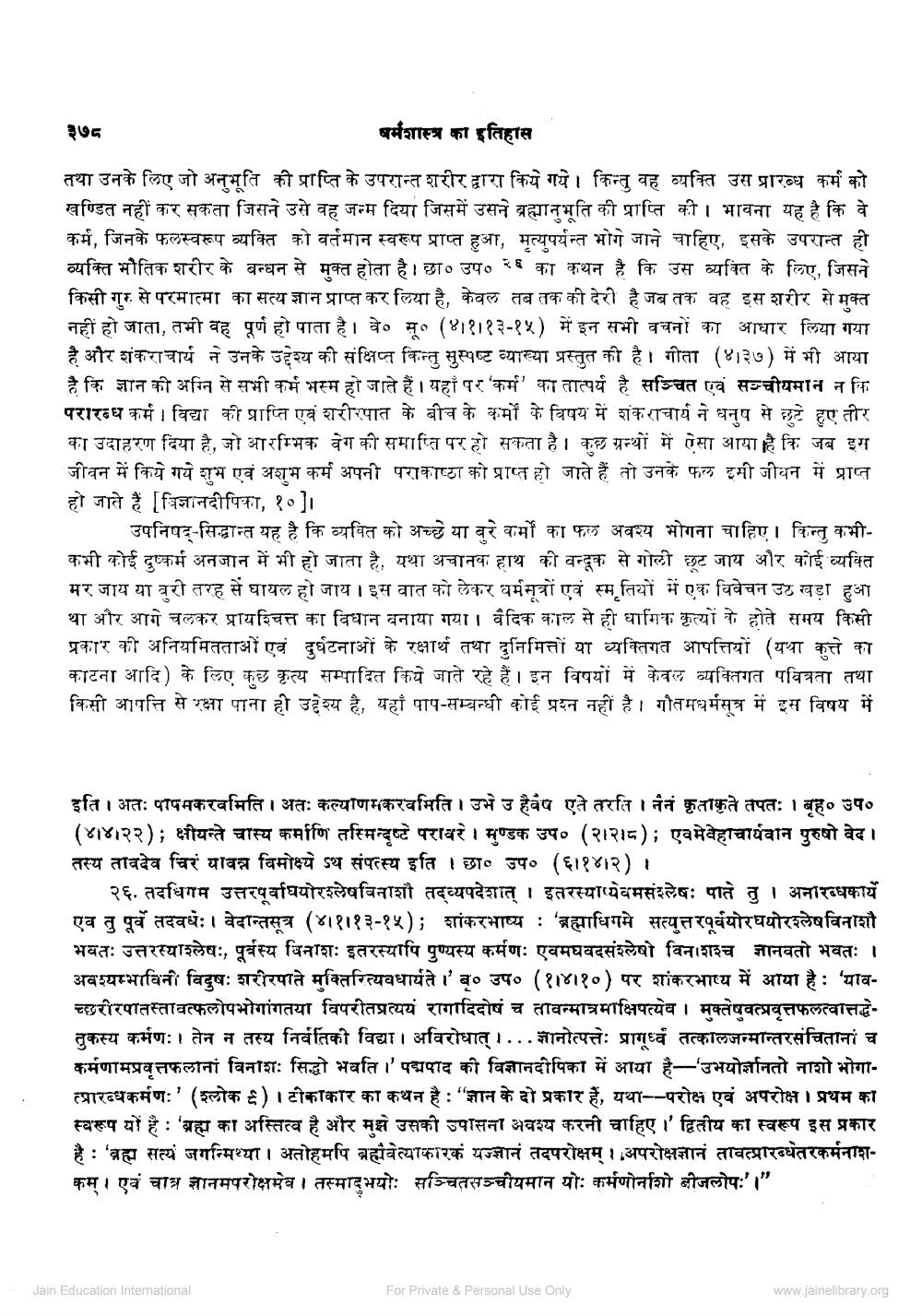________________
धर्मशास्त्र का इतिहास तथा उनके लिए जो अनुभूति की प्राप्ति के उपरान्त शरीर द्वारा किये गये। किन्तु वह व्यक्ति उस प्रारब्ध कर्म को खण्डित नहीं कर सकता जिसने उसे वह जन्म दिया जिसमें उसने ब्रह्मानुभूति की प्राप्ति की। भावना यह है कि वे कर्म, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति को वर्तमान स्वरूप प्राप्त हआ न्त भोगे जाने चाहिए, इसके उपरान्त ही व्यक्ति भौतिक शरीर के बन्धन से मुक्त होता है। छा० उप० २६ का कथन है कि उस व्यक्ति के लिए, जिसने किसी गुरु से परमात्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, केवल तब तक की देरी है जब तक वह इस शरीर से मक्त नहीं हो जाता, तभी वह पूर्ण हो पाता है। वे० स० (४।१।१३-१५) में इन सभी वचनों का आधार लिया गया है और शंकराचार्य ने उनके उद्देश्य की संक्षिप्त किन्तु सुस्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की है। गीता (४।३७) में भी आया है कि ज्ञान की अग्नि से सभी कर्म भस्म हो जाते हैं । यहाँ पर 'कर्म' का तात्पर्य है सञ्चित एवं सञ्चीयमान न कि परारब्ध कर्म । विद्या की प्राप्ति एवं शरीरपात के बीच के कर्मों के विषय में शंकराचार्य ने धनुष से छुटे हए तीर का उदाहरण दिया है, जो आरम्भिक वेग की समाप्ति पर हो सकता है। कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि जब इस जीवन में किये गये शुभ एवं अशुभ कर्म अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके फल इमी जीवन में प्राप्त हो जाते हैं [विज्ञानदीपिका, १०]।
उपनिषद्-सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति को अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना चाहिए। किन्तु कभीकभी कोई दुष्कर्म अनजान में भी हो जाता है, यथा अचानक हाथ की बन्दूक से गोली छूट जाय और कोई व्यक्ति मर जाय या बुरी तरह से घायल हो जाय । इस वात को लेकर धर्मसूत्रों एवं स्म तियों में एक विवेचन उठ खड़ा हुआ था और आगे चलकर प्रायश्चित्त का विधान बनाया गया। वैदिक काल से ही धार्मिक कृत्यों के होते समय किसी प्रकार की अनियमितताओं एवं दुर्घटनाओं के रक्षार्थ तथा दुनिमित्तों या व्यक्तिगत आपत्तियों (यथा कुत्ते का काटना आदि) के लिए कछ कृत्य सम्पादित किये जाते रहे हैं। इन विषयों में केवल व्यक्तिगत पवित्रता तथा किसी आपत्ति से रक्षा पाना ही उद्देश्य है, यहाँ पाप-सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं है। गौतमधर्मसत्र में इस विषय में
इति । अतः पापमकरवमिति । अतः कल्याणमकरवमिति । उभे उ हैवेष एते तरति । ननं कृताकृते तपतः । बृह० उप० (४।४।२२); क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । मुण्डक उप० (२।२१८); एवमेवेहाचार्यवान पुरुषो वेद। तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये ऽथ संपत्स्य इति । छा० उप० (६।१४।२)।
२६. तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् । इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु । अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः । वेदान्तसूत्र (४।१।१३-१५); शांकरभाष्य : 'ब्रह्माधिगमे सत्युत्तरपूर्वयोरघयोरश्लेषविनाशौ भवतः उत्तरस्याश्लेषः, पूर्वस्य विनाशः इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मणः एवमघवदसंश्लेषो विनाशश्च ज्ञानवतो भवतः । अवश्यम्भाविनी विदुषः शरीरपाते मुक्तिरित्यवधार्यते।' ब० उप० (१।४।१०) पर शांकरभाष्य में आया है : 'यावच्छरीरपातस्तावत्फलोपभोगांगतया विपरीतप्रत्ययं रागादिदोषं च तावन्मात्रमाक्षिपत्येव । मुक्तेषुवत्प्रवृत्तफलत्वात्तद्धे. तुकस्य कर्मणः। तेन न तस्य निर्वतिकी विद्या। अविरोधात्।... ज्ञानोत्पत्तेः प्रागवं तत्कालजन्मान्तरसंचितानां च कर्मणामप्रवत्तफलानां विनाशः सिद्धो भवति।' पद्मपाद की विज्ञानदीपिका में आया है-'उभयोनितो नाशो भोगाप्रारब्धकर्मणः' (श्लोक ६)।टीकाकार का कथन है : "ज्ञान के दो प्रकार हैं, यथा--परोक्ष एवं अपरोक्ष। प्रथम का स्वरूप यों है : 'ब्रह्म का अस्तित्व है और मझे उसकी उपासना अवश्य करनी चाहिए।' द्वितीय का स्वरूप इस प्रकार है : 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या। अतोहमपि ब्रह्मवेत्याकारकं यज्ज्ञानं तदपरोक्षम् । अपरोक्षजानं तावत्प्रारब्धतरकर्मनाशकम् । एवं चात्र ज्ञानमपरोक्षमेव । तस्मादुभयोः सञ्चितसञ्चीयमान योः कर्मणो शो नोजलोपः'।"
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org