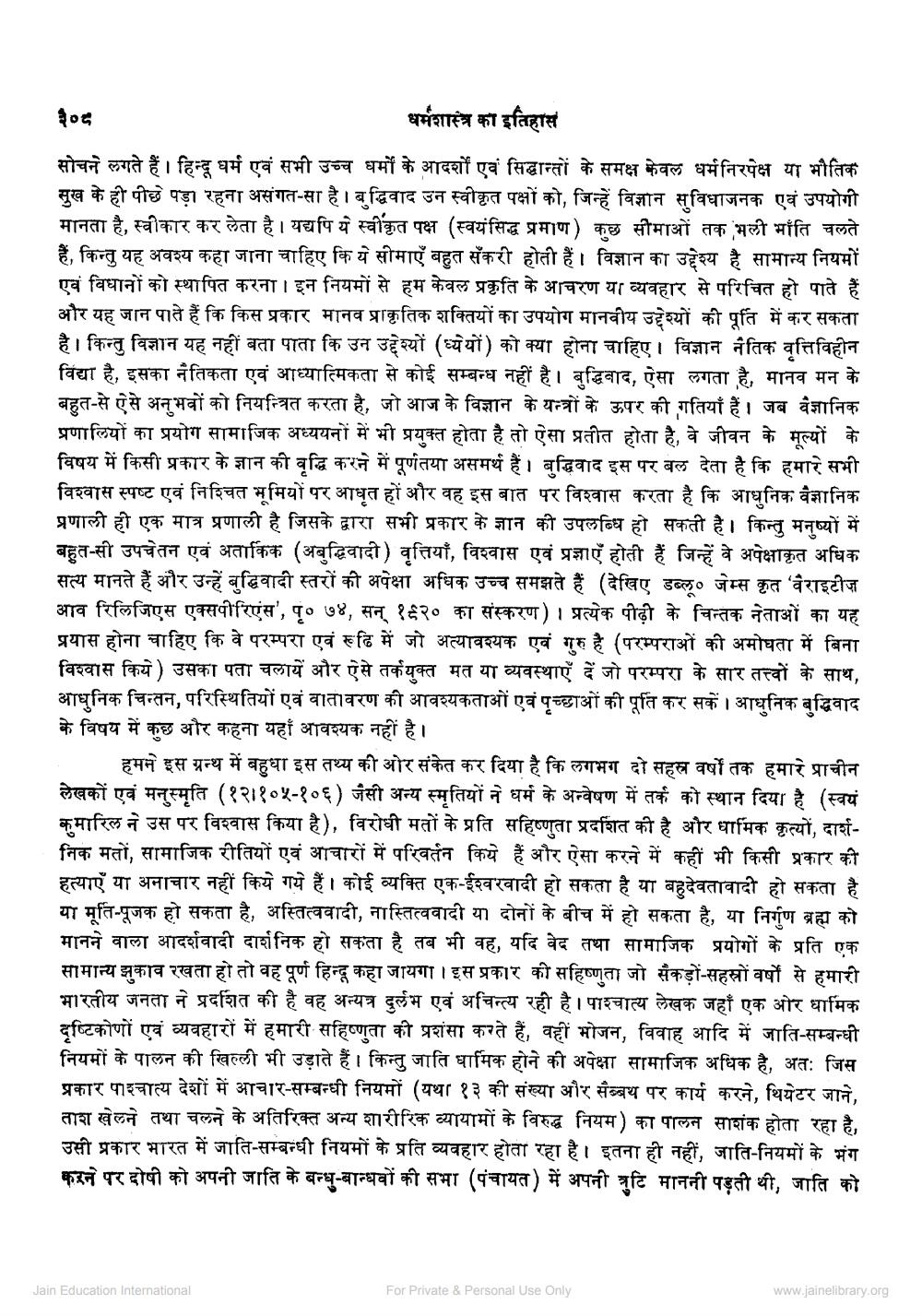________________
धर्मशास्त्र का इतिहास
३०८
सोचने लगते हैं । हिन्दू धर्म एवं सभी उच्च धर्मों के आदर्शों एवं सिद्धान्तों के समक्ष केवल धर्मनिरपेक्ष या भौतिक सुख के ही पीछे पड़ा रहना असंगत-सा है। बुद्धिवाद उन स्वीकृत पक्षों को, जिन्हें विज्ञान सुविधाजनक एवं उपयोगी मानता है, स्वीकार कर लेता है । यद्यपि ये स्वीकृत पक्ष (स्वयंसिद्ध प्रमाण ) कुछ सीमाओं तक भली भाँति चलते हैं, किन्तु यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि ये सीमाएँ बहुत सँकरी होती हैं। विज्ञान का उद्देश्य है सामान्य नियमों एवं विधानों को स्थापित करना । इन नियमों से हम केवल प्रकृति के आचरण या व्यवहार से परिचित हो पाते हैं और यह जान पाते हैं कि किस प्रकार मानव प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति में कर सकता है । किन्तु विज्ञान यह नहीं बता पाता कि उन उद्देश्यों (ध्येयों) को क्या होना चाहिए। विज्ञान नैतिक वृत्तिविहीन विद्या है, इसका नैतिकता एवं आध्यात्मिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है । बुद्धिवाद, ऐसा लगता है, मानव मन के बहुत से ऐसे अनुभवों को नियन्त्रित करता है, जो आज के विज्ञान के यन्त्रों के ऊपर की गतियाँ हैं । जब वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग सामाजिक अध्ययनों में भी प्रयुक्त होता है तो ऐसा प्रतीत होता है, वे जीवन के मूल्यों के विषय में किसी प्रकार के ज्ञान की वृद्धि करने में पूर्णतया असमर्थ हैं । बुद्धिवाद इस पर बल देता है कि हमारे सभी विश्वास स्पष्ट एवं निश्चित भूमियों पर आधृत हों और वह इस बात पर विश्वास करता है कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली ही एक मात्र प्रणाली है जिसके द्वारा सभी प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है । किन्तु मनुष्यों में बहुत-सी उपचेतन एवं अतार्किक (अबुद्धिवादी ) वृत्तियाँ, विश्वास एवं प्रज्ञाएँ होती हैं जिन्हें वे अपेक्षाकृत अधिक सत्य मानते हैं और उन्हें बुद्धिवादी स्तरों की अपेक्षा अधिक उच्च समझते हैं (देखिए डब्लू० जेम्स कृत 'वैराइटीज आव रिलिजिएस एक्सपीरिएंस', पृ० ७४ सन् १६२० का संस्करण) । प्रत्येक पीढ़ी के चिन्तक नेताओं का यह प्रयास होना चाहिए कि वे परम्परा एवं रूढि में जो अत्यावश्यक एवं गुरु है ( परम्पराओं की अमोघता में बिना विश्वास किये ) उसका पता चलायें और ऐसे तर्कयुक्त मत या व्यवस्थाएँ दें जो परम्परा के सार तत्त्वों के साथ, आधुनिक चिन्तन, परिस्थितियों एवं वातावरण की आवश्यकताओं एवं पृच्छाओं की पूर्ति कर सकें । आधुनिक बुद्धिवाद के विषय में कुछ और कहना यहाँ आवश्यक नहीं है ।
हमने इस ग्रन्थ में बहुधा इस तथ्य की ओर संकेत कर दिया है कि लगभग दो सहस्र वर्षों तक हमारे प्राचीन लेखकों एवं मनुस्मृति (१२ १०५-१०६) जैसी अन्य स्मृतियों ने धर्म के अन्वेषण में तर्क को स्थान दिया है (स्वयं कुमारिल ने उस पर विश्वास किया है), विरोधी मतों के प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित की है और धार्मिक कृत्यों, दार्शनिक मतों, सामाजिक रीतियों एवं आचारों में परिवर्तन किये हैं और ऐसा करने में कहीं भी किसी प्रकार की हत्याएँ या अनाचार नहीं किये गये हैं । कोई व्यक्ति एक ईश्वरवादी हो सकता है या बहुदेवतावादी हो सकता है। या मूर्तिपूजक हो सकता है, अस्तित्ववादी, नास्तित्ववादी या दोनों के बीच में हो सकता है, या निर्गुण ब्रह्म को मानने वाला आदर्शवादी दार्शनिक हो सकता है तब भी वह, यदि वेद तथा सामाजिक प्रयोगों के प्रति एक सामान्य झुकाव रखता हो तो वह पूर्ण हिन्दू कहा जायगा । इस प्रकार की सहिष्णुता जो सैकड़ों सहस्रों वर्षों से हमारी भारतीय जनता ने प्रदर्शित की है वह अन्यत्र दुर्लभ एवं अचिन्त्य रही है। पाश्चात्य लेखक जहाँ एक ओर धार्मिक दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों में हमारी सहिष्णुता की प्रशंसा करते हैं, वहीं भोजन, विवाह आदि में जाति-सम्बन्धी नियमों के पालन की खिल्ली भी उड़ाते हैं । किन्तु जाति धार्मिक होने की अपेक्षा सामाजिक अधिक है, अतः जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में आचार-सम्बन्धी नियमों (यथा १३ की संख्या और सैब्बथ पर कार्य करने, थियेटर जाने, ताश खेलने तथा चलने के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्यायामों के विरुद्ध नियम ) का पालन साशंक होता रहा है, उसी प्रकार भारत में जाति-सम्बन्धी नियमों के प्रति व्यवहार होता रहा है। इतना ही नहीं, जाति-नियमों के भंग करने पर दोषी को अपनी जाति के बन्धु बान्धवों की सभा (पंचायत) में अपनी त्रुटि माननी पड़ती थी, जाति को
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org