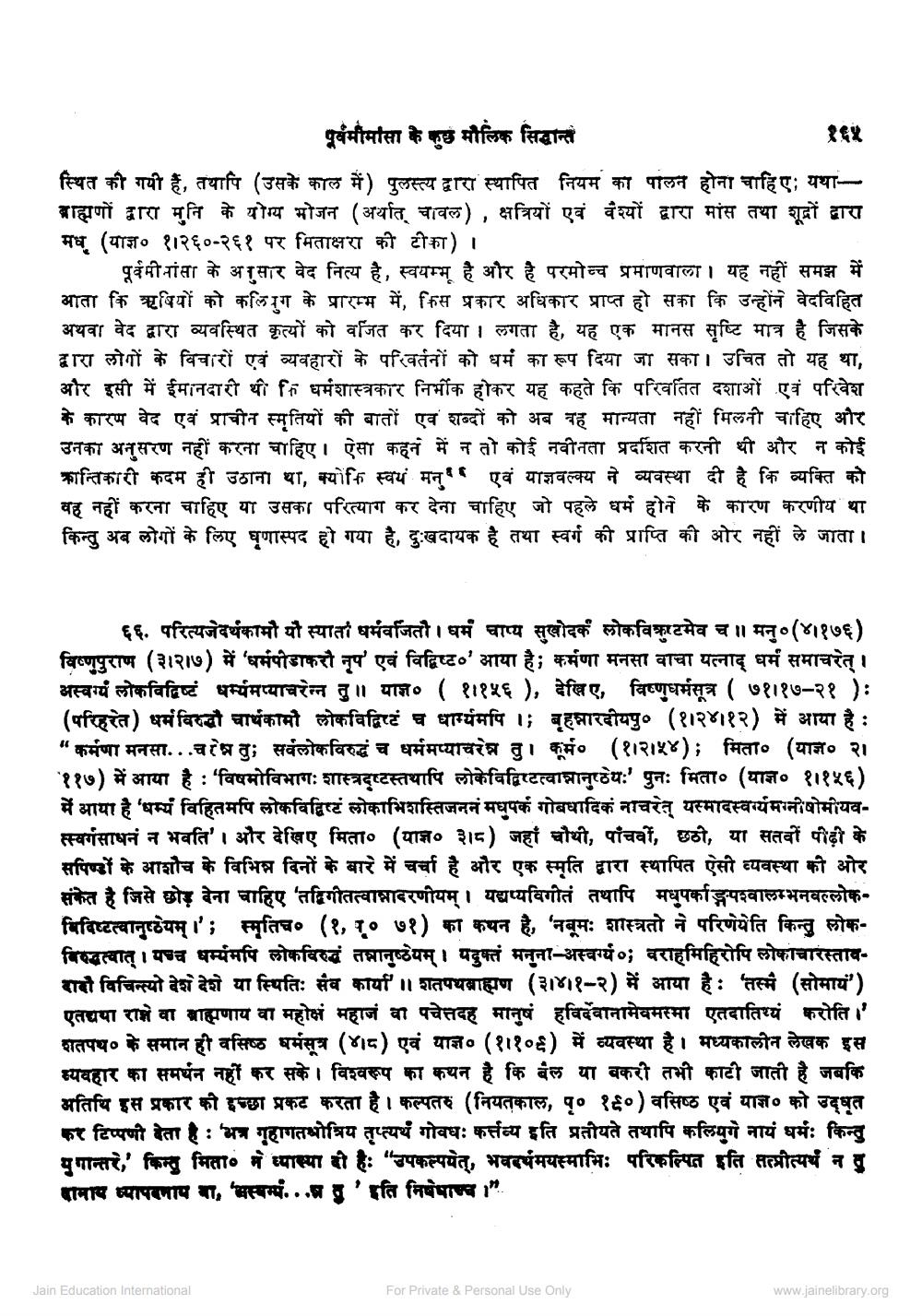________________
पूर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त
१६५ स्थित की गयी हैं, तथापि (उसके काल में) पुलस्त्य द्वारा स्थापित नियम का पालन होना चाहिए; यथाब्राह्मणों द्वारा मुनि के योग्य भोजन (अर्थात् चावल) , क्षत्रियों एवं वैश्यों द्वारा मांस तथा शूद्रों द्वारा मध (याज्ञ० ११२६०-२६१ पर मिताक्षरा की टीका)।
पूर्वमीनांसा के अनुसार वेद नित्य है, स्वयम्भू है और है परमोच्च प्रमाणवाला। यह नहीं समझ में आता कि ऋषियों को कलियुग के प्रारम्भ में, किस प्रकार अधिकार प्राप्त हो सका कि उन्होंने वेदविहित अथवा वेद द्वारा व्यवस्थित कृत्यों को वजित कर दिया। लगता है, यह एक मानस सृष्टि मात्र है जिसके द्वारा लोगों के विचारों एवं व्यवहारों के परिवर्तनों को धर्म का रूप दिया जा सका। उचित तो यह था, और इसी में ईमानदारी थी कि धर्मशास्त्रकार निर्भीक होकर यह कहते कि परिवर्तित दशाओं एवं परिवेश के कारण वेद एवं प्राचीन स्मृतियों की बातों एवं शब्दों को अब वह मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। ऐसा कहनं में न तो कोई नवीनता प्रदर्शित करनी थी और न कोई क्रान्तिकारी कदम ही उठाना था, क्योंकि स्वयं मनु। एवं याज्ञवल्क्य ने व्यवस्था दी है कि व्यक्ति को वह नहीं करना चाहिए या उसका परित्याग कर देना चाहिए जो पहले धर्म होने के कारण करणीय था किन्तु अब लोगों के लिए घृणास्पद हो गया है, दुःखदायक है तथा स्वर्ग की प्राप्ति की ओर नहीं ले जाता।
६६. परित्यजेदर्थकामो यो स्याता धर्मजितौ । धर्म चाप्य सुखोदकं लोकविक्रुटमेव च ॥ मनु० (४।१७६) विष्णुपुराण (३३२१७) में 'धर्मपीडाकरौ नृप' एवं विद्विष्ट०' आया है। कर्मणा मनसा वाचा यत्नाद् धर्म समाचरेत् । अस्वयं लोकविद्विष्टं धर्नामप्याचरेन्न तु॥ याज्ञ० (१११५६ ), देखिए, विष्णुधर्मसूत्र ( ७१।१७-२१ ): (परिहरत) धर्मविरदी चार्थकामो लोकविद्विष्टं च धार्यमपि । बृहन्नारदीयपु० (१।२४।१२) में आया है : "कर्मणा मनसा...चरेन तु; सर्वलोकविरुद्धं च धर्ममप्याचरेन तु। कूर्म० (१।२।५४); मिता० (याज्ञ० २। ११७) में आया है : 'विषमोविभागः शास्त्रदृष्टस्तथापि लोकेविद्विष्टत्वान्नानुष्ठेयः' पुनः मिता० (याज्ञ० ११५६) में आया है 'धम्यं विहितमपि लोकविद्विष्टं लोकाभिशस्तिजननं मधुपर्क गोबधादिकं नाचरेत् यस्मादस्वर्यमग्नीषोमीयवस्वर्गसाधनं न भवति' । और देखिए मिता० (याज्ञ० ३८) जहाँ चौथी, पांचवीं, छठी, या सतवीं पीढ़ी के सपिण्डों के आशौच के विभिन्न दिनों के बारे में चर्चा है और एक स्मृति द्वारा स्थापित ऐसी व्यवस्था की ओर संकेत है जिसे छोड़ देना चाहिए 'तद्विगीतत्वान्नादरणीयम् । यद्यप्यविगीतं तथापि मधुपर्काङ्गपश्वालम्भनवल्लोकविविष्टत्वानुष्ठेयम्।' स्मृतिच० (१, १० ७१) का कथन है, 'नबूमः शास्त्रतो ने परिणेयेति किन्तु लोकविरुद्धत्वात् । यच्च धर्नामपि लोकविरुद्ध तन्नानुष्ठेयम्। यदुक्तं मनुना-अस्वयं; वराहमिहिरोपि लोकाचारस्तावरादौ विचिन्त्यो देश देशे या स्थितिः सैव कार्या' ॥ शतपथब्राह्मण (३।४।१-२) में आया है : 'तस्मै (सोमाय') एतद्यया राक्षे वा ब्राह्मणाय वा महोक्षं महाजं वा पचेत्तदह मानुषं हविर्देवानामेवमस्मा एतदातिथ्यं करोति।' शतपथ के समान ही वसिष्ठ धर्मसूत्र (४८) एवं याज्ञ० (१११०६) में व्यवस्था है। मध्यकालीन लेखक इस व्यवहार का समर्थन नहीं कर सके। विश्वरूप का कथन है कि बल या बकरी तभी काटी जाती है जबकि अतिथि इस प्रकार की इच्छा प्रकट करता है। कल्पतरु (नियतकाल, पृ० १६०) वसिष्ठ एवं याज्ञ० को उद्धृत कर टिप्पणी देता है : 'भत्र गृहागतश्रोत्रिय तृप्त्यर्थ गोवधः कर्तव्य इति प्रतीयते तथापि कलियुगे नायं धर्मः किन्तु युगान्तरे,' किन्तु मिता० में व्याख्या दी है: "उपकल्पयेत्, भवदर्यमयस्माभिः परिकल्पित इति सत्प्रीत्यर्थ न तु बामाप व्यापलाय ना, अस्थम्ब...तु' इति मिषेपाच्च।"
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org