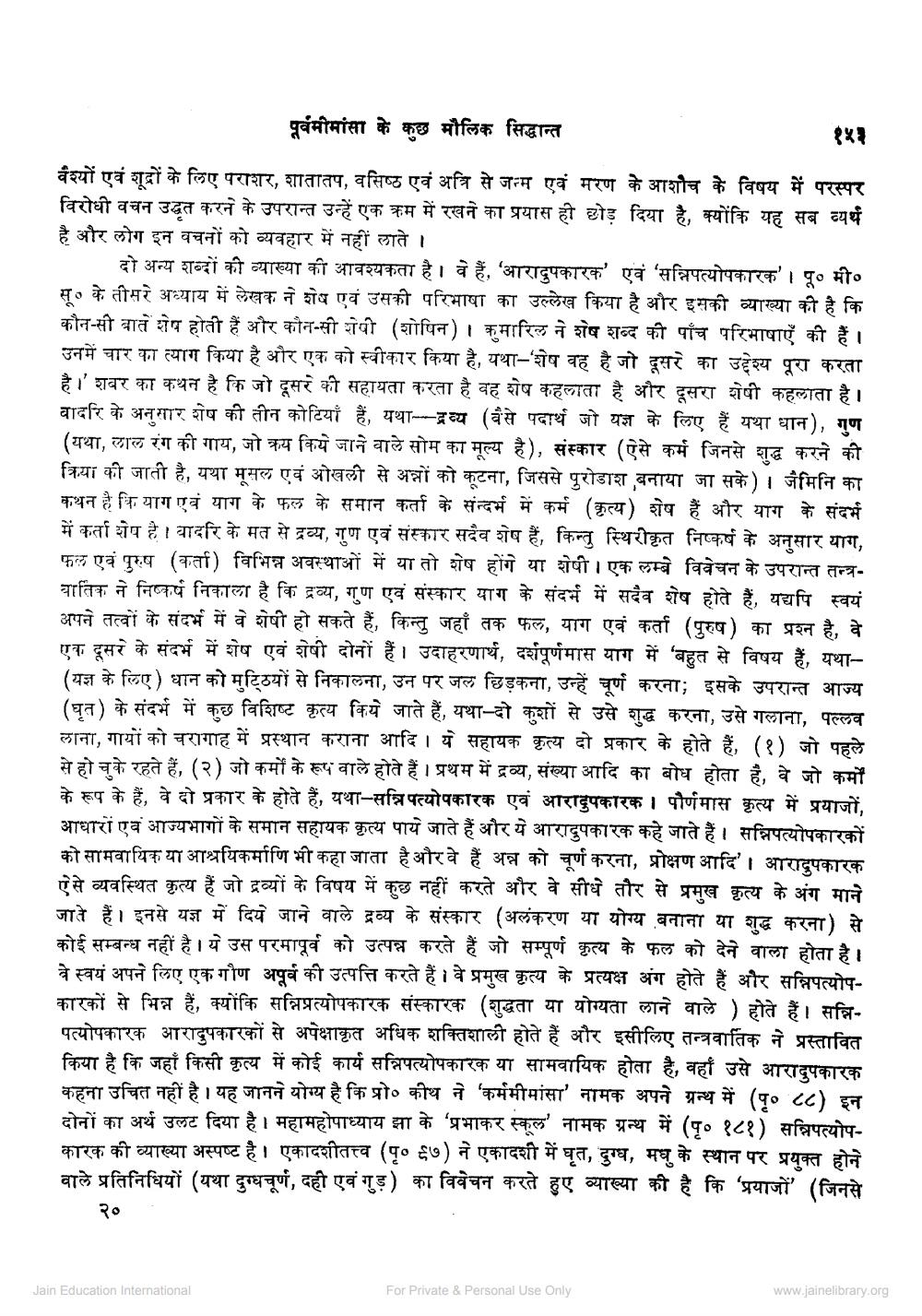________________
पूर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त
वैश्यों एवं शूद्रों के लिए पराशर, शातातप, वसिष्ठ एवं अत्रि से जन्म एवं मरण के आशौच के विषय में परस्पर विरोधी वचन उद्धृत करने के उपरान्त उन्हें एक क्रम में रखने का प्रयास ही छोड़ दिया है, क्योंकि यह सब व्यर्थ है और लोग इन वचनों को व्यवहार में नहीं लाते ।।
___ दो अन्य शब्दों की व्याख्या की आवश्यकता है। वे हैं, 'आरादुपकारक' एवं 'सन्निपत्योपकारक'। पू० मी० सू० के तीसरे अध्याय में लेखक ने शेष एवं उसकी परिभाषा का उल्लेख किया है और इसकी व्याख्या की है कि कौन-सी बाते शेष होती हैं और कौन-सी शेषी (शोषिन)। कुमारिल ने शेष शब्द की पाँच परिभाषाएँ की हैं। उनमें चार का त्याग किया है और एक को स्वीकार किया है, यथा-शेष वह है जो दूसरे का उद्देश्य पूरा करता है।' शबर का कथन है कि जो दूसरे की सहायता करता है वह शेष कहलाता है और दूसरा शेषी कहलाता है। वादरि के अनुसार शेष की तीन कोटियाँ हैं, यथा--द्रव्य (वैसे पदार्थ जो यज्ञ के लिए हैं यथा धान), गुण (यथा, लाल रंग की गाय, जो क्रय किये जाने वाले सोम का मूल्य है), संस्कार (ऐसे कर्म जिनसे शुद्ध करने की क्रिया की जाती है, यथा मूसल एवं ओखली से अन्नों को कूटना, जिससे पुरोडाश बनाया जा सके)। जैमिनि का कथन है कि याग एवं याग के फल के समान कर्ता के संन्दर्भ में कर्म (कृत्य) शेष हैं और याग के संदर्भ में कर्ता शेष है। वादरि के मत से द्रव्य, गण एवं संस्कार सदैव शेष हैं, किन्तु स्थिरीकृत निष्कर्ष के अनुसार याग, फल एवं पुरुष (कर्ता) विभिन्न अवस्थाओं में या तो शेष होंगे या शेषी। एक लम्बे विवेचन के उपरान्त तन्त्रवार्तिक ने निष्कर्ष निकाला है कि द्रव्य, गुण एवं संस्कार याग के संदर्भ में सदैव शेष होते हैं, यद्यपि स्वयं अपने तत्वों के संदर्भ में वे शेषी हो सकते हैं, किन्तु जहाँ तक फल, याग एवं कर्ता (पुरुष) का प्रश्न है, वे एक दूसरे के संदर्भ में शेष एवं शेषी दोनों हैं। उदाहरणार्थ, दर्शपूर्णमास याग में 'बहुत से विषय हैं, यथा(यज्ञ के लिए) धान को मुठ्ठियों से निकालना, उन पर जल छिड़कना, उन्हें चूर्ण करना; इसके उपरान्त आज्य (घृत) के संदर्भ में कुछ विशिष्ट कृत्य किये जाते हैं, यथा-दो कुशों से उसे शुद्ध करना, उसे गलाना, पल्लव लाना, गायों को चरागाह में प्रस्थान कराना आदि। ये सहायक कृत्य दो प्रकार के होते हैं, (१) जो पहले से हो चुके रहते हैं, (२) जो कर्मों के रूप वाले होते हैं । प्रथम में द्रव्य, संख्या आदि का बोध होता है, वे जो कर्मों के रूप के हैं, वे दो प्रकार के होते हैं, यथा-सन्निपत्योपकारक एवं आरादुपकारक । पौर्णमास कृत्य में प्रयाजों. आधारों एवं आज्यभागों के समान सहायक कृत्य पाये जाते हैं और ये आरादुपकारक कहे जाते हैं। सन्निपत्योपकारकों को सामवायिक या आश्रयिकर्माणि भी कहा जाता है और वे हैं अन्न को चूर्ण करना, प्रोक्षण आदि'। आरादुपकारक ऐसे व्यवस्थित कृत्य हैं जो द्रव्यों के विषय में कुछ नहीं करते और वे सीधे तौर से प्रमुख कृत्य के अंग माने जाते हैं। इनसे यज्ञ में दिये जाने वाले द्रव्य के संस्कार (अलंकरण या योग्य बनाना या शुद्ध करना) से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये उस परमापूर्व को उत्पन्न करते हैं जो सम्पूर्ण कृत्य के फल को देने वाला होता है। वे स्वयं अपने लिए एक गौण अपूर्व की उत्पत्ति करते हैं। वे प्रमुख कृत्य के प्रत्यक्ष अंग होते हैं और सन्निपत्योपकारकों से भिन्न हैं, क्योंकि सन्निप्रत्योपकारक संस्कारक (शुद्धता या योग्यता लाने वाले ) होते हैं। सन्निपत्योपकारक आरादुपकारकों से अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होते हैं और इसीलिए तन्त्रवार्तिक ने प्रस्तावित किया है कि जहाँ किसी कृत्य में कोई कार्य सन्निपत्योपकारक या सामवायिक होता है, वहाँ उसे आरादुपकारक कहना उचित नहीं है। यह जानने योग्य है कि प्रो० कीथ ने 'कर्ममीमांसा' नामक अपने ग्रन्थ में (पृ० ८८) इन दोनों का अर्थ उलट दिया है। महामहोपाध्याय झा के 'प्रभाकर स्कूल' नामक ग्रन्थ में (पृ० १८१) सन्निपत्योपकारक की व्याख्या अस्पष्ट है। एकादशीतत्त्व (पृ०६७) ने एकादशी में घृत, दुग्ध, मधु के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले प्रतिनिधियों (यथा दुग्धचूर्ण, दही एवं गुड़) का विवेचन करते हुए व्याख्या की है कि 'प्रयाजों' (जिनसे
२०
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org