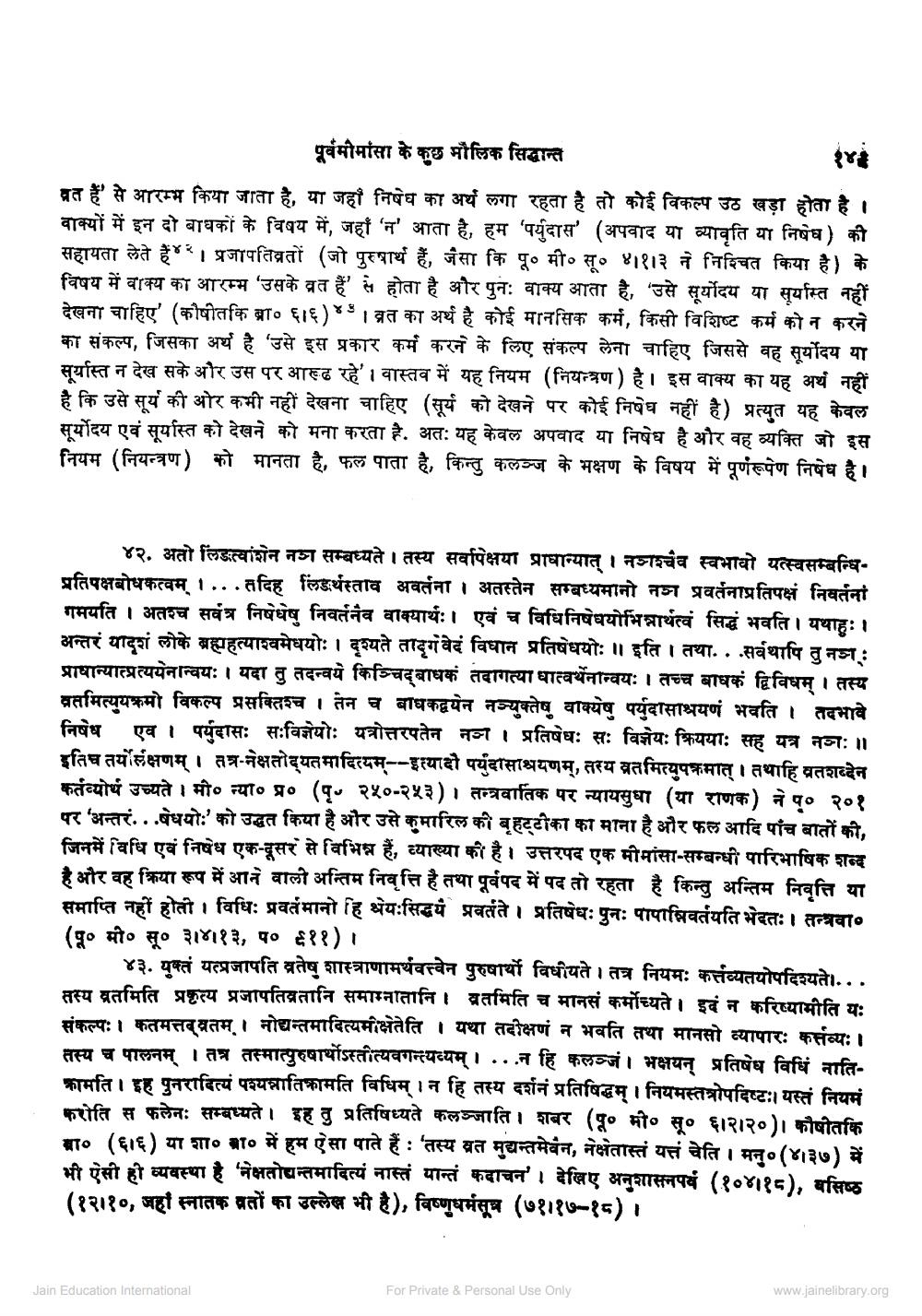________________
पूर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त व्रत हैं से आरम्भ किया जाता है, या जहाँ निषेध का अर्थ लगा रहता है तो कोई विकल्प उठ खड़ा होता है । वाक्यों में इन दो बाधकों के विषय में, जहाँ 'न' आता है, हम 'पर्यदास' (अपवाद या व्यावति या निषेध) की सहायता लेते हैं । प्रजापतिव्रतों (जो पुरषार्थ हैं, जैसा कि पू० मी० स० ४३११३ ने निश्चित किया है। के विषय में वाक्य का आरम्भ 'उसके व्रत हैं' से होता है और पुन: वाक्य आता है, 'उसे सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं देखना चाहिए' (कौषीतकि ब्रा० ६।६)४ । व्रत का अर्थ है कोई मानसिक कर्म, किसी विशिष्ट कर्म को न करने का संकल्प, जिसका अर्थ है 'उसे इस प्रकार कर्म करने के लिए संकल्प लेना चाहिए जिससे वह सूर्योदय या सर्यास्त न देख सके और उस पर आरूढ रहे।वास्तव में यह नियम (नियन्त्रण) है। इस वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि उसे सूर्य की ओर कभी नहीं देखना चाहिए (सूर्य को देखने पर कोई निषेध नहीं है) प्रत्युत यह केवल सूर्योदय एवं सूर्यास्त को देखने को मना करता है. अत: यह केवल अपवाद या निषेध है और वह व्यक्ति जो इस नियम (नियन्त्रण) को मानता है, फल पाता है, किन्तु कलज के भक्षण के विषय में पूर्णरूपेण निषेध है।
४२. अतो लिङत्वांशेन ना सम्बध्यते । तस्य सर्वापेक्षया प्राधान्यात् । नाश्चैव स्वभावो यत्स्वसम्बन्धिप्रतिपक्षबोधकत्वम् । ... तदिह लिंडर्थस्ताव अवर्तना । अतस्तेन सम्बध्यमानो नत्र प्रवर्तनाप्रतिपक्षं निवर्तनां गमयति । अतश्च सर्वत्र निषेधेषु निवर्तनैव वाक्यार्थः। एवं च विधिनिषेधयोभिन्नार्थत्वं सिद्धं भवति । यथाहः । अन्तरं यादृशं लोके ब्रह्महत्याश्वमेधयोः । दृश्यते तादृर्गवेदं विधान प्रतिषेधयोः ॥ इति । तथा.. .सर्वथापि तु न: प्राधान्यात्प्रत्ययेनान्वयः । यदा तु तदन्वये किञ्चिद्बाधकं तदागत्या धात्वर्थेनान्वयः । तच्च बाधकं द्विविधम् । तस्य व्रतमित्ययक्रमो विकल्प प्रसक्तिश्च । तेन च बाधकद्वयेन नञ्युक्तेषु वाक्येषु पर्युदासाश्रयणं भवति । तदभावे निषेध एव । पर्युदासः सःविज्ञेयोः यत्रोत्तरपतेन नन । प्रतिषेधः सः विज्ञेयः क्रिययाः सह यत्र नञः॥ इतिच तोलक्षणम् । तत्र-नेक्षतोद्यतमादित्यम्--इत्यादौ पर्युदासाश्रयणम्, तस्य व्रतमित्युपक्रमात् । तथाहि व्रतशब्देन कर्तव्योर्थ उच्यते । मो० न्या० प्र० (पृ. २५०-२५३)। तन्त्रवार्तिक पर न्यायसुधा (या राणक) ने प० २०१ पर 'अन्तरं...षेधयोः' को उद्धत किया है और उसे कुमारिल को बृहट्टीका का माना है और फल आदि पांच बातों को, जिनमें विधि एवं निषेध एक-दूसरे से विभिन्न हैं, व्याख्या की है। उत्तरपद एक मीमांसा-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द है और वह क्रिया रूप में आने वाली अन्तिम निवृत्ति है तथा पूर्वपद में पद तो रहता है किन्तु अन्तिम निवृत्ति या समाप्ति नहीं होती। विधिः प्रवर्तमानो हि श्रेयःसिद्धय प्रवर्तते। प्रतिषेधः पुनः पापानिवर्तयति भेदतः । तन्त्रवा० (पू० मी० सू० ३।४।१३, प० ६११)।
- ४३. युक्तं यत्प्रजापति व्रतेषु शास्त्राणामर्थवत्त्वेन पुरुषार्थो विधीयते । तत्र नियमः कर्तव्यतयोपदिश्यते।... तस्य व्रतमिति प्रकृत्य प्रजापतिव्रतानि समाम्नातानि। व्रतमिति च मानसं कर्मोच्यते। इदं न करिष्यामीति यः संकल्पः । कतमत्तवतम् । नोद्यन्तमादित्यमीक्षतेति । यथा तदीक्षणं न भवति तथा मानसो व्यापारः कर्तव्यः । तस्य च पालनम् । तत्र तस्मात्पुरुषार्थोऽस्तीत्यवगन्त्यव्यम्। ...न हि कलझं। भक्षयन् प्रतिषेध विधि नातिकामति । इह पुनरादित्यं पश्यन्नातिकामति विधिम् । न हि तस्य दर्शनं प्रतिषिद्धम् । नियमस्तत्रोपदिष्टः। यस्तं नियम करोति स फलेनः सम्बध्यते। इह तु प्रतिषिध्यते कलजाति। शबर (पू० मी० सू० ६।२।२०)। कौषीतकि बा० (६६) या शा० बा० में हम ऐसा पाते हैं : 'तस्य व्रत मुद्यन्तमेवैन, नेक्षेतास्तं यत्तं चेति । मनु० (४३७) में भी ऐसी ही व्यवस्था है 'नेक्षतोयन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन । देखिए अनुशासनपर्व (१०४११८), बसिष्ठ (१२।१०, जहां स्नातक व्रतों का उल्लेख भी है), विष्णुधर्मसूत्र (७१।१७-१८)।
www.jainelibrary.org
Jain Education International
For Private & Personal Use Only