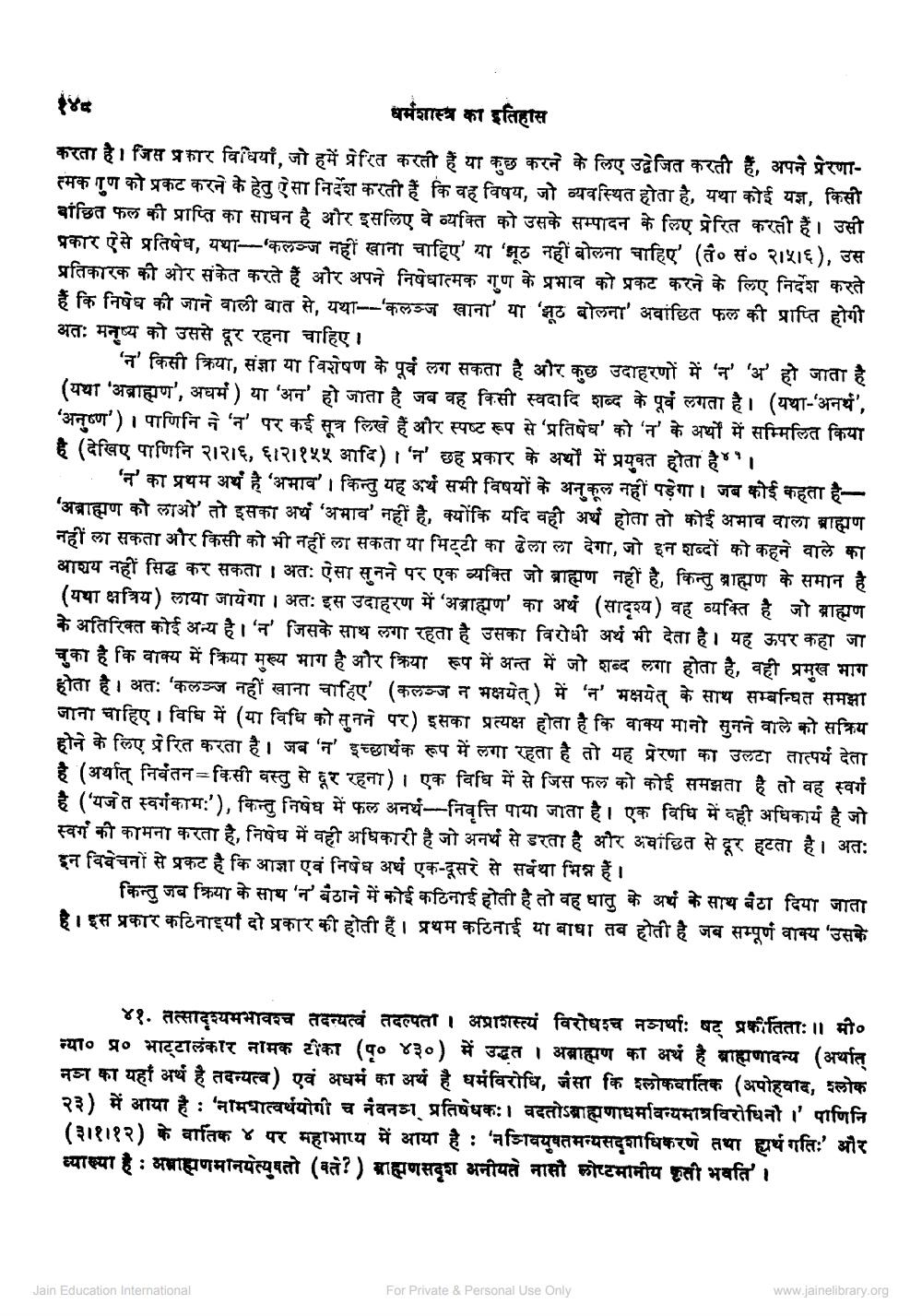________________
धर्मशास्त्र का इतिहास करता है। जिस प्रकार विधियाँ, जो हमें प्रेरित करती हैं या कुछ करने के लिए उद्वेजित करती हैं, अपने प्रेरणास्मक गुण को प्रकट करने के हेतु ऐसा निर्देश करती हैं कि वह विषय, जो व्यवस्थित होता है, यथा कोई यज्ञ, किसी बांछित फल की प्राप्ति का साधन है और इसलिए वे व्यक्ति को उसके सम्पादन के लिए प्रेरित करती हैं। उसी प्रकार ऐसे प्रतिषेध, यथा-'कलञ्ज नहीं खाना चाहिए' या 'झूठ नहीं बोलना चाहिए' (त० सं० २।५।६), उस प्रतिकारक की ओर संकेत करते हैं और अपने निषेधात्मक गुण के प्रभाव को प्रकट करने के लिए निर्देश करते हैं कि निषेध की जाने वाली बात से, यथा--'कलज खाना' या 'झूठ बोलना' अवांछित फल की प्राप्ति होगी अत: मनुष्य को उससे दूर रहना चाहिए।
'न' किसी क्रिया, संज्ञा या विशेषण के पूर्व लग सकता है और कुछ उदाहरणों में 'न' 'अ' हो जाता है (यथा 'अब्राह्मण', अधर्म) या 'अन' हो जाता है जब वह किसी स्वदादि शब्द के पूर्व लगता है। (यथा-'अनर्थ', 'अनुष्ण')। पाणिनि ने 'न' पर कई सूत्र लिखे हैं और स्पष्ट रूप से 'प्रतिषेध' को 'न' के अर्थों में सम्मिलित किया है (देखिए पाणिनि २।२।६, ६।२।१५५ आदि) । 'न' छह प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त होता है ।
'न' का प्रथम अर्थ है 'अभाव' । किन्तु यह अर्थ सभी विषयों के अनुकूल नहीं पड़ेगा। जब कोई कहता है'अब्राह्मण को लाओ तो इसका अर्थ 'अभाव' नहीं है, क्योंकि यदि वही अर्थ होता तो कोई अभाव वाला ब्राह्मण नहीं ला सकता और किसी को भी नहीं ला सकता या मिट्टी का ढेला ला देगा, जो इन शब्दों को कहने वाले का आशय नहीं सिद्ध कर सकता । अत: ऐसा सुनने पर एक व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है, किन्तु ब्राह्मण के समान है (यथा क्षत्रिय) लाया जायेगा । अत: इस उदाहरण में 'अब्राह्मण' का अर्थ (सादृश्य) वह व्यक्ति है जो ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई अन्य है। 'न' जिसके साथ लगा रहता है उसका विरोधी अर्थ भी देता है। यह ऊपर कहा जा चुका है कि वाक्य में क्रिया मुख्य भाग है और क्रिया रूप में अन्त में जो शब्द लगा होता है, वही प्रमुख भाग होता है। अत: 'कलञ्ज नहीं खाना चाहिए' (कलञ्ज न भक्षयेत् ) में 'न' मक्षयेत् के साथ सम्बन्धित समझा जाना चाहिए । विधि में (या विधि को सुनने पर) इसका प्रत्यक्ष होता है कि वाक्य मानो सुनने वाले को सक्रिय होने के लिए प्रेरित करता है। जब 'न' इच्छार्थक रूप में लगा रहता है तो यह प्रेरणा का उलटा तात्पर्य देता है (अर्थात् निर्वतन=किसी वस्तु से दूर रहना)। एक विधि में से जिस फल को कोई समझता है तो वह स्वर्ग है ('यजेत स्वर्गकाम:'), किन्तु निषेध में फल अनर्थ-निवृत्ति पाया जाता है। एक विधि में वही अधिकार्य है जो स्वर्ग की कामना करता है, निषेध में वही अधिकारी है जो अनर्थ से डरता है और अवांछित से दूर हटता है। अत: इन विवेचनों से प्रकट है कि आज्ञा एवं निषेध अर्थ एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं।
किन्तु जब क्रिया के साथ 'न' बैठाने में कोई कठिनाई होती है तो वह धातु के अर्थ के साथ बैठा दिया जाता है। इस प्रकार कठिनाइयाँ दो प्रकार की होती हैं । प्रथम कठिनाई या बाधा तब होती है जब सम्पूर्ण वाक्य 'उसके
४१. तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता। अप्राशस्त्यं विरोधश्च नार्थाः षट् प्रकीर्तिताः॥ मी० न्या० प्र० भाट्टालंकार नामक टीका (पृ० ४३०) में उद्धृत । अब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मणादन्य (अर्थात् नञ का यहां अर्थ है तदन्यत्व) एवं अधर्म का अर्थ है धर्मविरोधि, जैसा कि श्लोकवार्तिक (अपोहवाद, श्लोक २३) में आया है : 'नामधात्वर्थयोगी च नवना प्रतिषेधकः। वदतोऽब्राह्मणाधर्मावन्यमात्रविरोधिनौ ।' पाणिनि (३।१।१२) के वातिक ४ पर महाभाप्य में आया है : 'नशिवयुवतमन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थ गतिः' और व्याख्या है : अब्राह्मणमानयत्युषतो (क्त? ) ब्राह्मणसदृश अनीयते नासौ लोप्टमानीय कृती भवति ।
www.jainelibrary.org
Jain Education International
Jain Education International
For Private & Personal Use Only