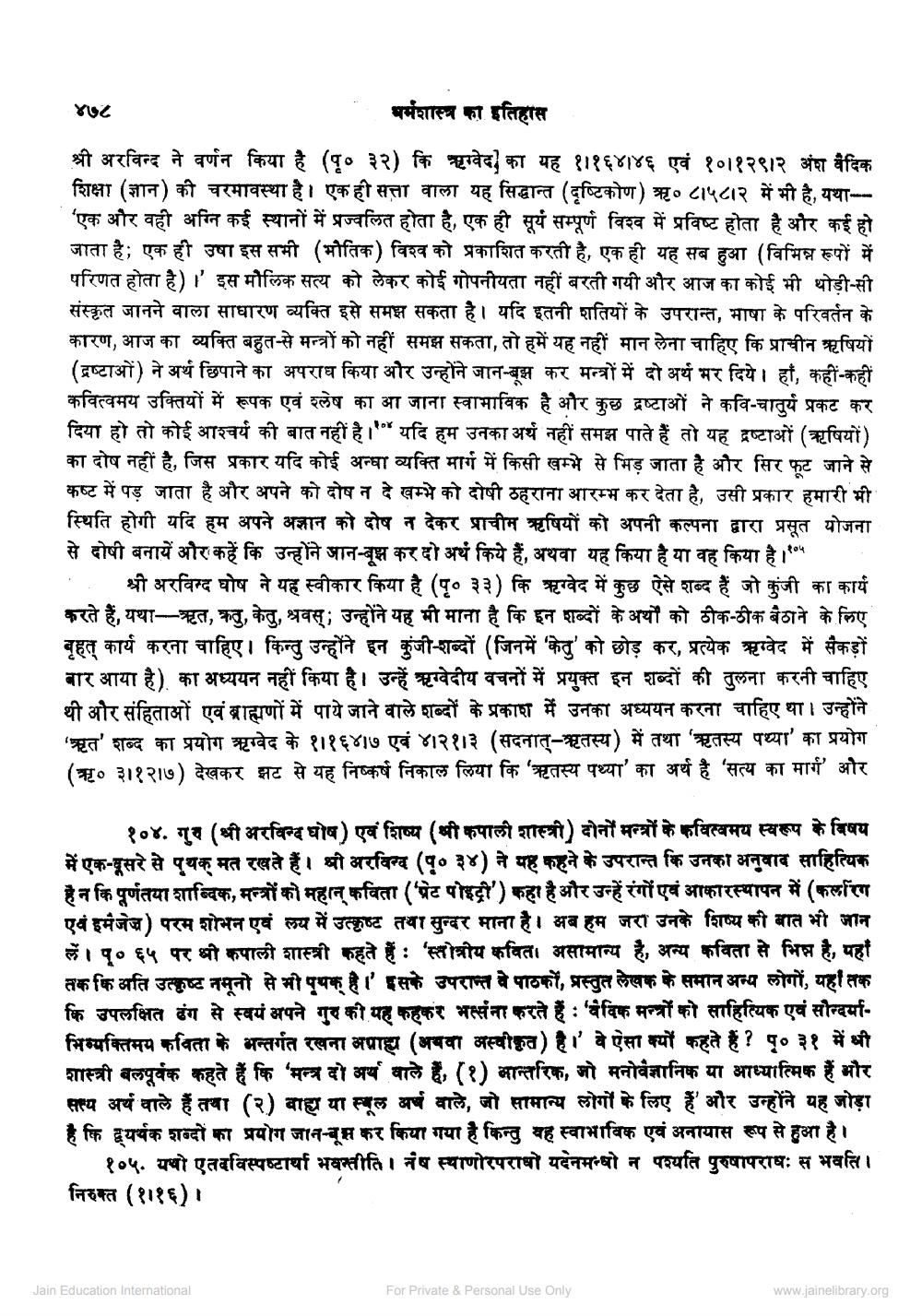________________
४७८
भर्मशास्त्र का इतिहास श्री अरविन्द ने वर्णन किया है (पृ. ३२) कि ऋग्वेद का यह १११६४१४६ एवं १०।१२९।२ अंश वैदिक शिक्षा (ज्ञान) की चरमावस्था है। एक ही सत्ता वाला यह सिद्धान्त (दृष्टिकोण) ऋ० ८५८०२ में भी है, यथा'एक और वही अग्नि कई स्थानों में प्रज्वलित होता है, एक ही सूर्य सम्पूर्ण विश्व में प्रविष्ट होता है और कई हो जाता है; एक ही उषा इस सभी (भौतिक) विश्व को प्रकाशित करती है, एक ही यह सब हुआ (विभिन्न रूपों में परिणत होता है)।' इस मौलिक सत्य को लेकर कोई गोपनीयता नहीं बरती गयी और आज का कोई भी थोड़ी-सी संस्कृत जानने वाला साधारण व्यक्ति इसे समझ सकता है। यदि इतनी शतियों के उपरान्त, भाषा के परिवर्तन के कारण, आज का व्यक्ति बहुत-से मन्त्रों को नहीं समझ सकता, तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि प्राचीन ऋषियों (द्रष्टाओं) ने अर्थ छिपाने का अपराध किया और उन्होंने जान-बूझ कर मन्त्रों में दो अर्थ भर दिये। हाँ, कहीं-कहीं कवित्वमय उक्तियों में रूपक एवं श्लेष का आ जाना स्वाभाविक है और कुछ द्रष्टाओं ने कवि-चातुर्य प्रकट कर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।" यदि हम उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो यह द्रष्टाओं (ऋषियों) का दोष नहीं है, जिस प्रकार यदि कोई अन्धा व्यक्ति मार्ग में किसी खम्भे से भिड़ जाता है और सिर फूट जाने से कष्ट में पड़ जाता है और अपने को दोष न दे खम्भे को दोषी ठहराना आरम्भ कर देता है, उसी प्रकार हमारी भी स्थिति होगी यदि हम अपने अज्ञान को दोष न देकर प्राचीन ऋषियों को अपनी कल्पना द्वारा प्रसूत योजना से दोषी बनायें और कहें कि उन्होंने आन-बूझ कर दो अर्थ किये हैं, अथवा यह किया है या वह किया है।०५ - श्री अरविन्द घोष ने यह स्वीकार किया है (पृ० ३३) कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुंजी का कार्य करते हैं, यथा-ऋत, ऋतु, केतु, श्रवस्; उन्होंने यह भी माना है कि इन शब्दों के अर्थों को ठीक-ठीक बैठाने के लिए बृहत् कार्य करना चाहिए। किन्तु उन्होंने इन कुंजी शब्दों (जिनमें 'केतु' को छोड़ कर, प्रत्येक ऋग्वेद में सैकड़ों बार आया है) का अध्ययन नहीं किया है। उन्हें ऋग्वेदीय वचनों में प्रयुक्त इन शब्दों की तुलना करनी चाहिए थी और संहिताओं एवं ब्राह्मणों में पाये जाने वाले शब्दों के प्रकाश में उनका अध्ययन करना चाहिए था। उन्होंने 'ऋत' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के १२१६४१७ एवं ४१२११३ (सदनात्-ऋतस्य) में तथा 'ऋतस्य पथ्या' का प्रयोग (ऋ० ३।१२।७) देखकर झट से यह निष्कर्ष निकाल लिया कि 'ऋतस्य पथ्या' का अर्थ है 'सत्य का मार्ग' और
१०४. गुव (श्री अरविन्द घोष) एवं शिष्य (श्री कपाली शास्त्री) दोनों मन्त्रों के कवित्वमय स्वरूप के विषय में एक-दूसरे से पृथक् मत रखते हैं। श्री अरविन्द (१० ३४) ने यह कहने के उपरान्त कि उनका अनुवाद साहित्यिक है न कि पूर्णतया शाब्दिक, मन्त्रों को महान कविता ('प्रेट पोइद्री') कहा है और उन्हें रंगों एवं आकारस्थापन में (कलरिंग एवं इमैजेज) परम शोभन एवं लय में उत्कृष्ट तथा सुन्दर माना है। अब हम जरा उनके शिष्य की बात भी जान लें। पृ० ६५ पर श्री कपाली शास्त्री कहते हैं : 'स्तोत्रीय कविता असामान्य है, अन्य कविता से भिन्न है, यहाँ तक कि अति उत्कृष्ट नमूनो से भी पृषक है।' इसके उपरान्त वे पाठकों, प्रस्तुत लेखक के समान अन्य लोगों, यहां तक कि उपलक्षित ढंग से स्वयं अपने गुरु की यह कहकर भत्सना करते हैं : 'वैविक मन्त्रों को साहित्यिक एवं सौन्दर्याभिव्यक्तिमय कविता के अन्तर्गत रखना अग्राह्य (अथवा अस्वीकृत) है।' वे ऐसा क्यों कहते हैं ? पृ० ३१ में श्री शास्त्री बलपूर्वक कहते हैं कि 'मन्त्र दो अर्थ वाले हैं, (१) मान्तरिक, जो मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक हैं और सत्य अर्थ वाले हैं तथा (२) बाह्य या स्थूल अर्थ वाले, जो सामान्य लोगों के लिए हैं और उन्होंने यह जोड़ा है कि यर्थक शब्दों का प्रयोग जान-बूझ कर किया गया है किन्तु वह स्वाभाविक एवं अनायास रूप से हुआ है।
१०५. यथो एतदविस्पष्टार्था भवन्तीति । नंष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति पुरुषापराषः स भवति । निरुक्त (१११६)।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org