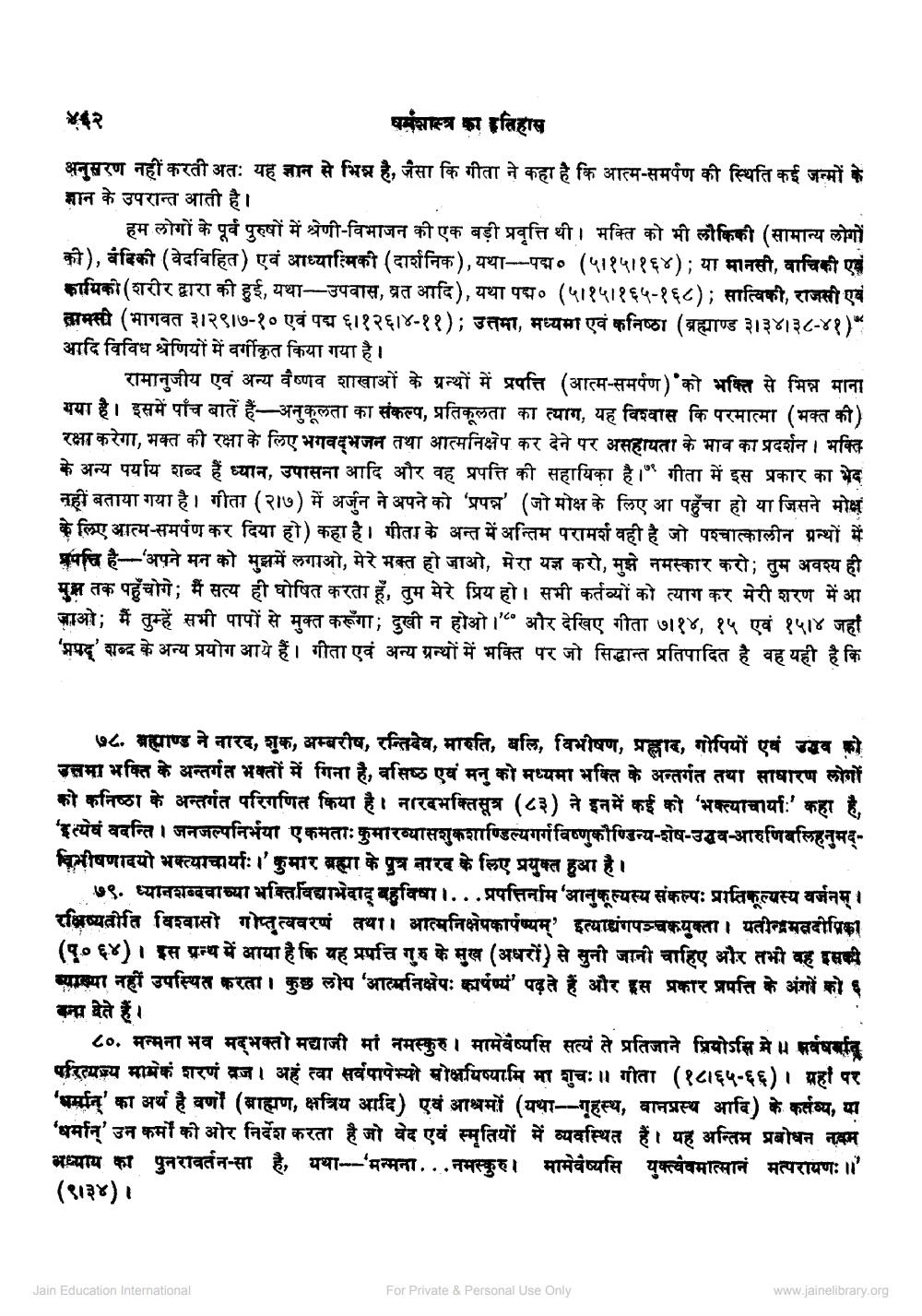________________
४६२
धर्मशास्त्र का इतिहास अनुसरण नहीं करती अतः यह ज्ञान से भिन्न है, जैसा कि गीता ने कहा है कि आत्म-समर्पण की स्थिति कई जन्मों के झान के उपरान्त आती है।
__हम लोगों के पूर्व पुरुषों में श्रेणी-विभाजन की एक बड़ी प्रवृत्ति थी। भक्ति को भी लौकिकी (सामान्य लोगों की), वैदिको (वेदविहित) एवं आध्यात्मिकी (दार्शनिक), यथा---पद्म० (५।१५।१६४); या मानसी, वाचिकी एवं कायिकी (शरीर द्वारा की हुई, यथा-उपवास, प्रत आदि), यथा पद्म० (५।१५।१६५-१६८); सात्विकी, राजसी एवं तामसी (भागवत ३।२९।७-१० एवं पद्म ६।१२६।४-११); उत्तमा, मध्यमा एवं कनिष्ठा (ब्रह्माण्ड ३।३४।३८-४१)* आदि विविध श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
रामानुजीय एवं अन्य वैष्णव शाखाओं के ग्रन्थों में प्रपत्ति (आत्म-समर्पण) को भक्ति से भिन्न माना यया है। इसमें पाँच बातें हैं-अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, यह विश्वास कि परमात्मा (भक्त की) रक्षा करेगा, भक्त की रक्षा के लिए भगवद्भजन तथा आत्मनिक्षेप कर देने पर असहायता के भाव का प्रदर्शन । भक्ति के अन्य पर्याय शब्द हैं ध्यान, उपासना आदि और वह प्रपत्ति की सहायिका है। गीता में इस प्रकार का भेद नहीं बताया गया है। गीता (२१७) में अर्जुन ने अपने को 'प्रपन्न' (जो मोक्ष के लिए आ पहुँचा हो या जिसने मोक्ष के लिए आत्म-समर्पण कर दिया हो) कहा है। गीता के अन्त में अन्तिम परामर्श वही है जो पश्चात्कालीन ग्रन्थों में प्रपत्ति है-'अपने मन को मुझमें लगाओ, मेरे भक्त हो जाओ, मेरा यज्ञ करो, मुझे नमस्कार करो; तुम अवश्य ही मुझ तक पहुँचोगे; मैं सत्य ही घोषित करता हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। सभी कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ; मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँगा; दुखी न होओ। और देखिए गीता ७।१४, १५ एवं १५।४ जहाँ 'प्रपद्' शब्द के अन्य प्रयोग आये हैं। गीता एवं अन्य ग्रन्थों में भक्ति पर जो सिद्धान्त प्रतिपादित है वह यही है कि
७८. ब्रह्माण्ड ने नारद, शुक, अम्बरीष, रन्तिदेव, मारुति, बलि, विभीषण, प्रह्लाद, गोपियों एवं उखव को उत्तमा भक्ति के अन्तर्गत भक्तों में गिना है, वसिष्ठ एवं मनु को मध्यमा भक्ति के अन्तर्गत तथा साधारण लोगों को कनिष्ठा के अन्तर्गत परिगणित किया है। नारदभक्तिसूत्र (८३) ने इनमें कई को 'भक्त्याचार्याः' कहा है, 'इत्येवं वदन्ति । जनजल्पनिर्भया एकमताः कुमारव्यासशुकशाण्डिल्यगर्गविष्णुकौण्डिन्य-शेष-उखव-आरुणिबलिहनुमद्विभीषणादयो भक्त्याचार्याः।' कुमार ब्रह्मा के पुत्र नारद के लिए प्रयुक्त हुआ है।
७९. ध्यानशब्दवाच्या भक्तिविद्याभेदा बहुविषा।...प्रपत्तिर्नाम'आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् । रशिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा। आत्यनिक्षेपकार्पण्यम्' इत्याचंगपञ्चायुक्ता। यतीन्द्रमतदीपिका (पृ.० ६४)। इस ग्रन्थ में आया है कि यह प्रपत्ति गुरु के मुख (अधरों) से सुनी जानी चाहिए और तभी वह इसकी व्याख्या नहीं उपस्थित करता। कुछ लोय 'आत्मनिक्षेपः कार्पण्यं' पढ़ते हैं और इस प्रकार प्रपति के अंगों को ६ बना देते हैं।
८०. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि सत्यं से प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ सर्वषदि परित्यज्य मामेकं शरणं वज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ गीता (१८१६५-६६)। यहाँ पर 'धर्मान्' का अर्थ है वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि) एवं आश्रमों (यथा--गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि) के कर्तव्य, या 'धर्मान्' उन कर्मों को ओर निर्देश करता है जो वेद एवं स्मृतियों में व्यवस्थित हैं। यह अन्तिम प्रबोधन नवम अध्याय का पुनरावर्तन-सा है, यथा--'मन्मना... नमस्कुरु। मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥' (९॥३४)।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org