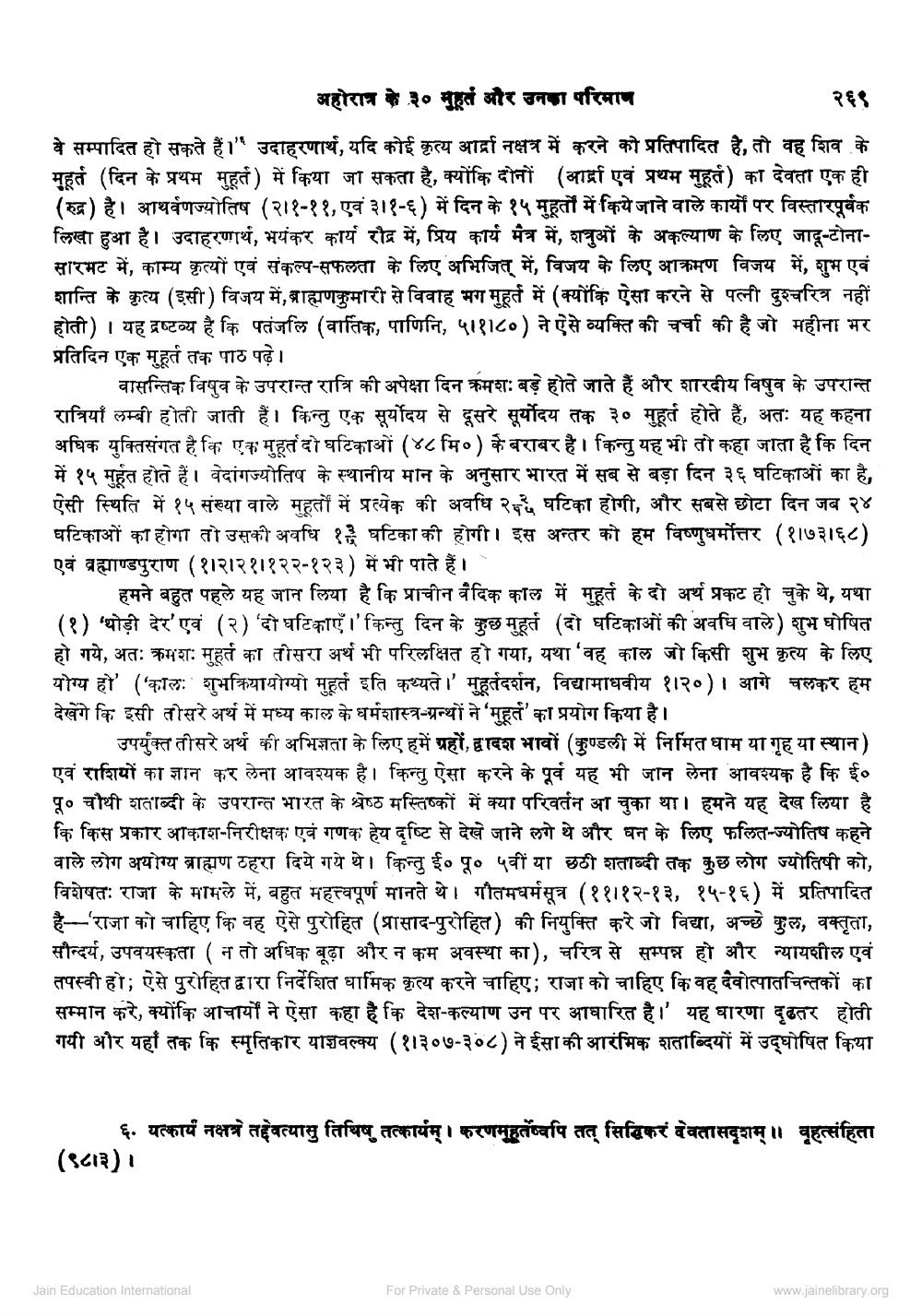________________
अहोरात्र के ३० मुहूर्त और उनका परिमाण
२६९ वे सम्पादित हो सकते हैं ।" उदाहरणार्थ, यदि कोई कृत्य आर्द्रा नक्षत्र में करने को प्रतिपादित है, तो वह शिव के मुहूर्त ( दिन के प्रथम मुहूर्त) में किया जा सकता है, क्योंकि दोनों (आर्द्रा एवं प्रथम मुहूर्त) का देवता एक ही (रुद्र) है । आथर्वणज्योतिष ( २1१-११, एवं ३।१-६) में दिन के १५ मुहूर्तों में किये जाने वाले कार्यों पर विस्तारपूर्वक लिखा हुआ है । उदाहरणार्थ, भयंकर कार्य रौद्र में, प्रिय कार्य मंत्र में, शत्रुओं के अकल्याण के लिए जादू-टोनासारमट में, काम्य कृत्यों एवं संकल्प - सफलता के लिए अभिजित् में, विजय के लिए आक्रमण विजय में, शुभ एवं शान्ति के कृत्य (इसी) विजय में, ब्राह्मणकुमारी से विवाह भग मुहूर्त में (क्योंकि ऐसा करने से पत्नी दुश्चरित्र नहीं होती) । यह द्रष्टव्य है कि पतंजलि (वार्तिक, पाणिनि, ५।१।८० ) ने ऐसे व्यक्ति की चर्चा की है जो महीना भर प्रतिदिन एक मुहूर्त तक पाठ पढ़े।
वासन्तिक विषुव के उपरान्त रात्रि की अपेक्षा दिन क्रमशः बड़े होते जाते हैं और शारदीय विषुव के उपरान्त रात्रियाँ लम्बी होती जाती हैं । किन्तु एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक ३० मुहूर्त होते हैं, अतः यह कहना अधिक युक्तिसंगत है कि एक मुहूर्त दो घटिकाओं ( ४८ मि०) के बराबर है । किन्तु यह भी तो कहा जाता है कि दिन में १५ मुर्हत होते हैं। वेदांगज्योतिष के स्थानीय मान के अनुसार भारत में सब से बड़ा दिन ३६ घटिकाओं का है, ऐसी स्थिति में १५ संख्या वाले मुहूर्तों में प्रत्येक की अवधि २१ घटिका होगी, और सबसे छोटा दिन जब २४ घटिकाओं का होगा तो उसकी अवधि १ घटिका की होगी । इस अन्तर को हम विष्णुधर्मोत्तर (१।७३।६८) एवं ब्रह्माण्डपुराण (१।२।२१।१२२-१२३) में भी पाते हैं ।
हमने बहुत पहले यह जान लिया है कि प्राचीन वैदिक काल में मुहूर्त के दो अर्थ प्रकट हो चुके थे, यथा (१) 'थोड़ी देर ' एवं (२) 'दो घटिकाएँ ।' किन्तु दिन के कुछ मुहूर्त (दो घटिकाओं की अवधि वाले) शुभ घोषित हो गये, अतः क्रमशः मुहूर्त का तीसरा अर्थ भी परिलक्षित हो गया, यथा 'वह काल जो किसी शुभ कृत्य के लिए योग्य हो' ('कालः शुभक्रियायोग्यो मुहूर्त इति कथ्यते ।' मुहूर्तदर्शन, विद्यामाधवीय १।२० ) । आगे चलकर हम देखेंगे कि इसी तीसरे अर्थ में मध्य काल के धर्मशास्त्र-ग्रन्थों ने 'मुहूर्त' का प्रयोग किया है।
उपर्युक्त तीसरे अर्थ की अभिज्ञता के लिए हमें ग्रहों, द्वादश भावों ( कुण्डली में निर्मित धाम या गृह या स्थान ) एवं राशियों का ज्ञान कर लेना आवश्यक है। किन्तु ऐसा करने के पूर्व यह भी जान लेना आवश्यक है कि ई० पू० चौथी शताब्दी के उपरान्त भारत के श्रेष्ठ मस्तिष्कों में क्या परिवर्तन आ चुका था । हमने यह देख लिया है fa fae प्रकार आकाश निरीक्षक एवं गणक हेय दृष्टि से देखे जाने लगे थे और धन के लिए फलित ज्योतिष कहने वाले लोग अयोग्य ब्राह्मण ठहरा दिये गये थे । किन्तु ई० पू० ५वीं या छठी शताब्दी तक कुछ लोग ज्योतिषी को, विशेषतः राजा के मामले में, बहुत महत्त्वपूर्ण मानते थे । गौतमधर्मसूत्र ( ११/१२-१३, १५-१६ ) में प्रतिपादित है— 'राजा को चाहिए कि वह ऐसे पुरोहित ( प्रासाद - पुरोहित) की नियुक्ति करे जो विद्या, अच्छे कुल, वक्तृता, सौन्दर्य, उपवयस्कता न तो अधिक बूढ़ा और न कम अवस्था का ), चरित्र से सम्पन्न हो और न्यायशील एवं तपस्वी हो; ऐसे पुरोहित द्वारा निर्देशित धार्मिक कृत्य करने चाहिए; राजा को चाहिए कि वह दैवोत्पातचिन्तकों का सम्मान करे, क्योंकि आचार्यों ने ऐसा कहा है कि देश - कल्याण उन पर आधारित है।' यह धारणा दृढतर होती गयी और यहाँ तक कि स्मृतिकार याज्ञवल्क्य (१।३०७ - ३०८) ने ईसा की आरंभिक शताब्दियों में उद्घोषित किया
६. यत्कार्य नक्षत्रे तद्देवत्यासु तिथिषु तत्कार्यम् । करणमुहूर्तेष्वपि तत् सिद्धिकरं देवता सदृशम् ॥ वृहत्संहिता (९८१३) ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org